
उच्चतम न्यायालय में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून की सन् 2015 में उसके द्वारा अवैधानिक घोषित धारा 66 ए के तहत प्राथमिकियां दर्ज किए जाने को ‘गंभीर चिंता का विषय’ ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि इन मामलों को तीन सप्ताह में वापस लिया जाए। रद्द की जा चुकी इस धारा 66 ए के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था।
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई धारा 66-ए के तहत पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की कार्यवाही को ‘गंभीर चिंता का विषय’ मानते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को हाल ही में यह निर्देश दिया कि इन मामलों को तीन सप्ताह में वापस लिया जाए। आईटी कानून की रद्द की जा चुकी धारा 66-ए के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2015 को दिए गए अपने निर्णय में इस प्रावधान को असंवैधानिक ठहराते हुए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संविधान का प्रमुख सिद्धांत बताया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर इस प्रावधान को रद्द कर दिया था कि जनता के ‘जानने का अधिकार’ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-ए से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किए गए प्रावधान का कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया और प्रदेशों एवं उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को नोटिस जारी किए।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति रविंद्र भट की पीठ ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस अदालत के एक आधिकारिक निर्णय में प्रावधान की वैधता को निरस्त करने एवं असंवैधानिक ठहराए जाने के बावजूद अब भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को जल्द से जल्द उपचारात्मक कदम उठाने और मामलों को वापस लेने की कार्यवाही तीन सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि इन परिस्थितियों में, हमने केंद्र के वकील से उन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ संवाद करने को भी कहा है, जहां मामले अब भी दर्ज किए जा रहे हैं या दर्ज हैं। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के वकील प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिवों के साथ संवाद करने के लिए स्वतंत्र होंगे और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील उनकी मदद करेंगे। न्यायालय ने कहा कि आज से तीन सप्ताह में यह कार्यवाही पूरी की जाए। मामले को तीन सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने के निर्देश भी न्यायालय ने दिए।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन मामलों में याचिकाएं / गैर पीपुल्स यूनियन फाॅर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा प्रस्तुत की गई थी। पीयूसीएल ने इस रद्द प्रावधान के तहत लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने का आरोप लगाया था। उच्चतम न्यायालय ने उसके द्वारा धारा 66-ए को निरस्त किए जाने के बावजूद लोगों के खिलाफ इसके तहत अब भी मामले दर्ज किए जाने पर पिछले साल पांच जुलाई को आश्चर्य व्यक्त किया। साथ ही इसे चौंकाने वाला भी बताया।
उल्लेखनीय है कि आईटी एक्ट में वर्ष 2009 में संशोधित अधिनियम के तहत धारा 66-ए को जोड़ा गया था। इस प्रावधान में कंप्यूटर रिसोर्स (डेस्क टाॅप, लैपटाॅप, टैब आदि) या संचार उपकरण (मोबाईल, स्मार्टफोन आदि) के माध्यम से संदेश भेजने वाले उन व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। जो मोटे तौर पर आपत्तिजनक है या धमकी भरा संदेश देते हैं। जो कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के जरिए जानबूझकर झूठी सूचना देता है, ताकि किसी को गुस्सा दिलाया जा सके, परेशान किया जा सके। खतरा और बाधा पैदा किया जा सके। अपमान किया जा सके, चोट पहुंचाई जा सके, आपराधिक धमकी दी जाए और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना का वातावरण बनाया जाए अथवा ऐसा व्यक्ति जो किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज भेजकर गुस्सा दिलाने, परेशान करने, धोखा देने और उससे अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करता है। ऐसे अपराध के लिए तीन साल तक की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया था।
इस प्रावधान को हटाने का संबंध शिवसेना चीफ रहे बाल ठाकरे के निधन से जुड़ा है। ठाकरे के निधन के बाद मुंबई का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। इसे लेकर फेसबुक पर टिप्पणियां की गई। इस पर महाराष्ट्र पुलिस ने टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार करने लगी और उनपर आईटी एक्ट की धारा 66-ए के तहत केस दर्ज करने लगी। उस समय कानून की विद्यार्थी श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी याचिका में धारा 66-ए को खत्म करने की मांग की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सन 2015 में ऐतिहासिक फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66-ए संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के उल्लंघन और अनुच्छेद 19(2) के तहत किए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत न आने के कारण आईटी एक्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक घोषित किया जाता है।
इस याचिका के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई सामग्री या संदेश किसी एक के लिए आपत्तिजनक हो सकता है तो दूसरे के लिए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की आजादी का संविधान प्रदत्त अधिकार का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 66-ए से लोगों के ‘जानने के अधिकार’ को भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तत्कालीन जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच ने कहा था कि यह प्रावधान साफ तौर पर संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 66-ए का दायरा काफी व्यापक है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करने से डरेगा। इस तरह यह धारा ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ के खिलाफ है। यह विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को चुनौती देता है। इस कारण धारा 66ए को सर्वोच्च न्यायालय ने गैर संवैधानिक घोषित किया।
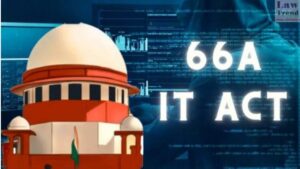
धारा 66-ए के प्रावधानों को जानना भी दिलचस्प है। इस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस को इस संदर्भ में गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया था कि पुलिसकर्मी अपने विवेक से आक्रमक या खतरनाक या बाधा, असुविधा आदि शब्दों को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर या किसी अन्य संचार उपकरण जैसे- मोबाइल फोन या टैबलेट के माध्यम से संदेश भेजने पर सजा को निर्धारित किया है जिसमें दोषी को अधिकतम तीन वर्ष की जेल हो सकती है। न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि धारा 66-ए की कमजोरी इस तथ्य में निहित है कि इसमें अपरिभाषित कार्यों को अपराध का आधार बनाया गया था। जैसे कि असुविधा, खतरा, बाधा और अपमान। ये सभी संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करते है तथा अपवादों की श्रेणी में नहीं आते हैं। न्यायालय के समक्ष चुनौती यह पहचान करने की थी कि लक्ष्मण रेखा कहां खींची जाए।
इसके अलावा न्यायालय ने यह भी पाया था कि धारा 66-ए में कानून के अन्य वर्गों की तरह कार्रवाई करने से पहले केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की आवष्यकता नहीं थी। साथ ही स्थानीय अधिकारी स्वायत रूप से अपने राजनीतिक गुरूओं की मर्जी से आगे बढ़ सकते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दो अन्य प्रावधानों यथा आईटी अधिनियम की धारा 69-ए और 79 को रद्द नहीं किया तथा कहा कि ये कुछ प्रतिबंधों के साथ लागू रह सकते हैं। धारा 69-ए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरूद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है और धारा 79 कुछ मामलों में मध्यस्थ के दायित्व से छूट प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना था कि धारा 66-ए संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण की स्वतंत्रता) 21 (जीवन का अधिकार) दोनों के विपरीत थी। साथ ही सूचना का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा प्रदान किये गए भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है।
नागरिक अधिकारों से जुड़े संगठनों, एनजीओ और विपक्ष की यह शिकायत रही है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए आईटी एक्ट की इस धारा का दुरूपयोग करती है। यह भी देखा गया है कि कई प्रदेशों की पुलिस मशीनरी ने वैसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं। राजनीतिक मुद्दों के अलावा कई बार टिप्पणी के केंद्र में राजनेता भी रहे हैं। इस कृत्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है और तर्क देती है कि ऐसी टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द्र, शांति, समरसता आदि को नुकसान होता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का संविधान के तहत अधिकार प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में अपनी बात रखता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो यह आजादी की जड़ों पर हमला है। अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस कारण इसे ‘रूल बुक’ से तुरन्त हटाया जाना चाहिए। अंतिम फैसले से पहले सरकार की दलील थी कि समाज और जनमानस में इंटरनेट का प्रभाव बहुत व्यापक है। सरकार ने यह भी कहा था कि प्रिंट (अखबार, पत्रिका आदि) और टेलीविजन की तुलना में इंटरनेट पर पाबंदी का नियम और भी कड़ा होना चाहिए। सरकार के मुताबिक टीवी और प्रिंट जहां अपने संस्थागत स्वरूप में चलते हैं। इसके विपरीत इंटरनेट के साथ ऐसा नहीं है। इस कारण इंटरनेट पर ज्यादा चेक एंड बैलेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। सरकार का यह भी तर्क था कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक सामग्री डालने में समाज में कानून का राज प्रभावित हो सकता है और इससे जनमानस में गुस्से का गुबार और हिंसक प्रवृत्ति जागृत हो सकती है।

विनय झैलावत
लेखक : पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं






