संस्मरण
यादों में पिता:
– सूर्यबाला
पान फूल सी बेटियां-
डि’प सा’ब को जानते हैं आप? डि’प‘ सा’ब का मतलब है डिप्टी साहेब। जी हां तो ये ही डिप सा‘ब मेरे बाबूजी हुआ करते थे।
नहीं, ऐसे नहीं बता सकूंगी, इसके लिए आपको दो तिहाई सदी के पहले वाले समय में ‘डाइव’ मारना होगा। सामने, बनारस (वाराणसी नहीं) के चेत गंज मुहल्ले की चउरछटवा की गली होगी और गली का चैथा वाला ही मकान तो है डिप सा‘ब का… आप आसानी से पहचान लेंगे….
क्योंकि यह मकान, अगल बगल के घरों जैसी छोटी खिड़कियां और संकरी सीढ़ियों वाला नहीं। नीचे से ऊपर तक शुभ्र सफेद, लेसदार ब्राइडल-केक की तरह, कंगूरों कटी रेलिंगों और जालीदार मुंड़ेरों से सजा, किसी कलात्मक वास्तुकृति की तरह शान से सिर उठाए खड़ा हुआ करता था गली में। (आज भी खड़ा है…) ‘खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी को चरितार्थ करता….
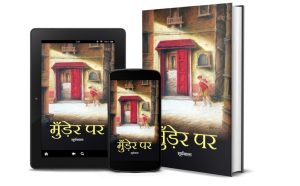
उन दिनों रास्ते से गुजरने वाले लोग अक्सर सिर उठाकर देखते रह जाते…. किसी मध्यवर्गीय गृहस्थ के लिए ऐसे शानदार मकान की कल्पना भी दुष्कर होती उनके लिए। खूब ऊंचे और चौड़े, शीशम के दरवाजे, और ऊंची ही मंजिलें… इतनी कि जहां इस घर की तीसरी मंजिल पूरी होती, उतने पर अगल बगल के घरों की चौथी… मंजिलें भी मुश्किल से पहुंच पातीं।
तो यह डिप‘ साब का मकान था।
और डिप‘ साब?…
बड़े रूआबदार, बड़े शानदार…. जितने गुस्से वाले, उतने ही संजीदे। गुस्सा आया तो जैसे बादल फटे, बिजली कडकी, समूचा घर हिलने पे आजाता, जैसे तूफान बरपा हो…. और पिघले तो जैसे ग्लेशियर…. जैसे पारे की बिखरती बूंदे।… उसके बाद शुरू होता माफीनामों का बेपनाह सिलसिला और पछतावों की किश्तें। बच्चों से लेकर मां तक के सामने अपनी गलती स्वीकारने में उन्हें जरा संकोच नहीं था। मां ऐसे माफीनामों पर थोड़े आदर, थोड़े प्यार से मुस्करा भर देतीं….. और ज्यादातर तो (उनके तेवर अंदाजते हुए) ऐसी स्थितियों की नौबत ही नहीं आने देतीं….
संभाला होगा कभी राजा भगीरथ ने गंगा की प्रचंड वेगधारा को….. यहां तो मेरी माँ ‘भागीरथी’ ही संभाल रही थी, कभी भी पूरे घर को कंपा देने वाले ‘रूद्रावतार’ को।… अचानक छन्नू लाल मिश्र की गाई ठुमरी याद आ रही है… ‘होली खेलें महादेव मसाने में….’ कब इन रूद्रावतार का तांडव शुरू हो जाएगा और कब, ‘सदा बसंतम् हृदयारविंदे, भवम् भवानी….’ सहित मगन मन, गौरा पार्वती और (कार्तिकेय, गणेश न सही) अपनी पान फूल सी बेटियों को पढ़ाते-सिखाते और दुलारते नजर आएंगे, कोई नहीं कह सकता था…
तो इन्हीं डिप सा‘ब की बड़ी-छोटी, हम चार बेटियां थीं। सोने, रूपे सी लाड़ दुलारों में पली। कायदे, कानून और शिष्टाचार के खूबसूरत फ्रेम में मढ़ी…. और अनुशासन ऐसा कि जान पहचान वाले एक दूसरे, से कहते न थकें कि डिप‘साब ने अपनी लड़कियों को बड़ी उम्दा तालीम दी है…. साहब….’
माय नेम इश शूल्य बाला
बेहद जहीन हैं उनकी चारों बेटियां। हिंदी में सवाल पूछो तो अंग्रेजी में जवाब देती हैं। सो तो है ही। बचपन में ही उनकी तोतली जबान के सही हिज्जे फूटने से पहले ही इन बेटियों को रटाया जाता है- कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है बेटी?… तो हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में जवाब देना, समझीं…। जैसे? जैसे-
‘व्हाट इज़ योर नेम?’ तो?
‘माय नेम इश शूल्यबाला उल्फ मोहिनी’
शाब्बाश!….
इसी तरह-
व्हाट इज़ योर फादर्स नेम?…. व्हाट इज़ योर मदर्स नेम?…. व्हेयर डू यू लिव?…. आदि, तमाम सारे सवालों के जवाबों की तोता रटंती।
इस वाक्य ने मेरे अंदर उस बला की छोटी उम्र में एक गुमान भरा स्थायी भाव सा बिठा दिया था कि ऐसा हर रटाया जाता’ वाक्य बहुत विशिष्ट है। इससे लोगों के बीच अपना रूतबा बढ़ता है। लोग हमें आश्चर्यजनित प्रसन्नता, थोड़े रश्क और फख्र से देखते हैं। वाह! इतनी छोटी बच्ची ‘इंग्लिश’ बोलती है! (आज से तीन चौथाई सदी पहले) बेशक, यह गरीबों नहीं अमीरों की भाषा है।… झोपड़ झुग्गी नहीं, पक्के मकानों की भाषा है।… इसके इस्तेमाल से हम जिस बिरादरी, जिस वर्ग के हैं, उससे बहुत ऊपर वाले हो जाते हैं। बल्कि यों कहें कि जो हैं, वो नहीं रह जाते, जो नहीं हैं, वो हो जाते हैं।
लेकिन परेशानी तब होती, जब रट्टा मार कर याद कराई गई इस अंग्रेजी में उलट-पलट हो जाता। यानी ‘सिस्टर’ की जगह ‘मदर’ का और ‘मदर’ की जगह ‘फादर’ का नाम निकल जाता… (अब अगल बगल सुनने वालों की खिलखिलाहट या दबी मुस्कान ही, शर्म से पानी-पानी करनेको काफी होती। तो क्या! अरे भई छोटी बच्ची है गड़बड़ा गई- ‘व्हेयर इज़ योर ‘इयर’? में कानों की जगह ‘हेयर’, बालों को छू दिया और ‘टीथ’ की जगह- ‘नोज’ पर उंगली रख दी- अंदर-अंदर बुरी तरह झेंप जाती… लेकिन उतने छुटपन में भी, लोगों के मन में अपनी अंग्रेजी का सिक्का तो बैठता ही। एक बड़ी तसल्ली। बचपन में पनपी सुपीरियॉरिटी और इनफीरियॉरिटी वाली ऐसी अनेक अदृश्य ग्रांथियां ही शायद आधी सदी बाद मुझसे ‘माय नेम इश ताता…’ जैसी कहानी लिखवा ले गईं। कहानी में नन्हीं तोतली ताता (सुजाता) को शहर के बेस्ट ‘प्रैप’ में एडमीशन दिलाने के लिए उसकी मां नीना लगातार रटाती रहती है- जब मैम पूछेंगी, ‘व्हाट इज़ योर नेम चाइल्ड?…’ तो क्या कहेगी मेरी बेबी?…..
‘ताता!…‘माय नेम इश ताता’…. दो तोतले बोल पकी जामुन से टपक पड़ते….

कभी-कभी लगता है, पिछली आधी सदी से मैं इस वाक्य से छुटकारे की राह खोजती रही थी क्या! यद्यपि यह कहानी सिर्फ भाषा-माध्यम की समस्या नहीं, बल्कि आज की जिंदगी के दमघोंट घमासान में नृशंस स्वार्थ और ‘इस्तेमाल के तराजू पर तौले जाने वाले रिश्तों की विडंबना और उनकी थोड़ी ही सही, भरपाई की दिशा में एक वाजिब संकेत है… लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर पैठी वर्षों की कुंठा, और अपराध-बोध वाली शर्मिंदगी से भी मुझे मुक्त कर गई यह कहानी। मेरे अपने प्रतिरोध का इजहार, मेरे अवचेतन ने, ताता से करवाया।
इंसपेक्टर बनाम डिक्टेटर…
यादों में यह पिता….
हां, तो ‘डिप साब’ बोले तो वही, जिला-विद्यालय-निरीक्षक, अंग्रेजों के जमाने वाले डिप्टी इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स… एक मध्यम वर्ग का सरकारी मुलाज़िम ही… लेकिन रूतबा और शौक, रजवाड़ों को मात करने वाला। शायद यह शहर के ही उच्च वर्गीय तरक्की पसंद रइसजादों की सोहबत और दोस्ती का असर रहा हो… जैसे राय साहब टोडरमल के छोटे भाई बीरबल… जिनकी हवेलीनुमा कोठियों के आयोजनों और शुभकार्यों में नामी गिरामी गायिकाएं, नर्तकियां बाकायदे पर्देदारी में शिरकत करने के लिए ससम्मान बुलाई जाती थीं। (बाद की एकाध राय साहब की संरक्षिता की वंशजाओं में सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका सिद्धेश्वरी देवी, अलकनंदा जैसी उस जमाने की प्रख्यात कत्थक नर्तकियों का शुमार भी था।) अपनी गली के नुक्कड़ वाले हनुमान मंदिर के श्रृंगार (उत्सव) में तख्तों को सटाकर बनाए गए मंच पर कत्थक पर थिरकते अलकनंदा के धुंधुरूओं पर, अपनी तीसरी मंजिल के बारजे पर खड़ी मेरे पैर ताल देते होते…..
बहरहाल, डिप‘ साब ने उन रजवाड़ों से सिर्फ सुरूचि और कलात्मकता का ही सलीका सीखा था। बाकी की अच्छा खाने, अच्छा ही पहनने, अच्छे गीत-संगीत, (हारमोनियम, बांसुरी) सुरूचि पूर्ण साज-सज्जा और तबीयत की शौकीनी उनके अपने स्वभाव की देन थी। जिंदादिल और वाक्पटु इतने कि तिहाई सदी पहले के उनके कई मौलिक जुमले आज तक हमारे कुटुंब के मुहावरे बने हुए हैं। जैसे किसी अतिअशिष्ट, उजड्ड आदमी की बात चलने पर – कौन? फलाना? उसे तो पूंछ लगा दो तो पेड़ पर चढ़ जाये… यानी?…. कि थोड़ी सी ही कसर है बाकी…. सुनने वाला ठठा कर हंसता…
परिहासी कटाक्ष की ऐसी बानगी, उनकी विदग्धता की प्रतीक तो होती ही, उनकी हद की अनुशासन प्रियता और नो-नॉनसेंस की तरफ भी बकायदे इशारा कर देती।
बारीकी से ही सही, पर प्रतिरोधी पर ताने तिश्नों के वाक् प्रहारों से भी कभी चूकते नहीं थे…. लेकिन हां उतनी ही शाइस्तगी से सामने वाले का वार भी हंसते-हंसते झेल ले जाने की कूवत रखते थे। (बशर्ते वह सही हो…) अपनी चूकों पर खुलकर क्षमा मांगना भी उन्हें आता था, चाहे प्रतिवादी उनसे बारह वर्ष छोटी उनकी पत्नी और बड़ी, छोटी बेटियां ही क्यों न हों।
आज आधी सदी बाद भी, जहां एक तरफ, गुस्से से गरजते-तरजते, पिता की हुंकार मेरे कानों को सहमाती है तो दूसरी तरफ सिर्फ घंटे दो घंटे बाद ही पछतावे से विगलित मां से माफी मांगते पिता का आर्द्र स्वर भी।…
लेकिन उसे छोटी उम्र में मुझे यह सब बेहद नागवार गुजरता था…. उनका गरजना तरजना ही नहीं, माफी मांगना भी… मुझे गुस्सैल पिता ही नहीं, माफी मांगने वाले पिता से भी अरूचि और चिढ़ हो जाती थी।…. लेकिन आज समझ पाई हूं कि बड़ी से बड़ी गलती पर किया जाने वाला पश्चाताप आदमी को मनुष्य बनाता है। फिर यह पिता, अपने मिजाज की ‘नो-नॉनसेंस’ वाली आदत से भी तो लाचार था।
ये फलानी कान पकड़कर खड़ी क्यों हैं भाई?….
उस जमाने में हम छुटकनियां बहनों के आचरण और व्यवहार की पहरेदारी इतनी सर्तकता से की जाती कि कभी भी अपनी किसी अशिष्टता या बेजा हरकत पर (गल्तियों की गंभीरता के हिसाब से) हममे से कोई भी घर के किसी कौने में कान पकड़ कर खड़ी देखी जा सकती थी। सजा थोड़ी ज्यादा लंबी होने पर, मेरे लिये ही बनी एक छोटी कुर्सी पर मुझे कान पकडा़कर बिठा दिया जाता। यह सजा, दीवाल की तरफ मुंह कर खड़े होने की मिलती तो फिर भी गनीमत होती लेकिन यदि इसकी उल्टी होती, अर्थात सारे आते जाते लोगों के सामने (होठों में मुस्कराते नौकरों चाकरों तक) हम कान पकड कर खड़े या कुर्सी पर बैठे होते तो उस शर्मिंदगी की कल्पना किसी के लिए मुश्किल होगी। कभी-कभी तो कोई मेहमान या दूध, भाजी वाला पूछ भी बैठता- ‘ये फलानी’ कान पकड़ कर खड़ी क्यों है भाई- तब हम पर घड़ों पानी पड़ जाता। लेकिन यह भी याद है कि कुछ देर बीतते न बीतते, पिता से गुफ्तगू भी करती मां की आवाज आती- ‘सुन रहे हैं आप!…’ कहिये तो इन्हें अब माफी दे दी जाये।… इन्होंने अपनी गलती मान ली है। कह रही हैं कि आगे से कभी फ्रॉक पर स्याही नहीं गिरायेगी। नाक में उंगली नहीं डालेगी और मुंह से ‘हट्ट’ या ‘केदार’ को ‘केदरवा’ नहीं बुलायेंगी।….
तो चलो, भई सजा माफ। ग्लानि और शर्मिंदगी से छुटकारा, बहुत बड़ी राहत होती हमारे लिए। ‘रिहाई’ की घोषणा के साथ ही हम सचमुच दिल से अपने थानेदार पिता के शुक्रगुजार महसूस करते… और दुबारा वैसी गलती न करने की कसम के साथ खुश-खुश भाग निकलते…. वह तो बड़ी होने के बाद पता चला कि ‘माफीनामे’ वाली मां की पेशकश भी, पिता के इशारों पर ही चलायी गई होती।
तो वह बचपन बहुत अबोध, भोला और अनुशसित था। बड़ों के आदेश, निर्देश या सलाहों पर उखड़ कर बगावत पर नहीं उतरा करता था, और न अपने आपको ‘बड़ों’ से भी ज्यादा बड़ा और समझदार प्रमाणित करने की जिद् पर अड़ा होता था। उल्टे उनका किंचित संकोच और लिहाज, अक्सर गलत उठते कदमों को रोक भी दिया करता था। (अब तो, ‘सॉरी’, बच्चें नहीं, ‘बड़े’ ‘सॉरी’ ही बोलते देखते जाते हैं।)
बावजूद इस सबके पिता के प्रति विद्रोह या बगावत वाली बात मन में कभी नहीं आई….
सिवा उस एक खौफज़दा अंधेरी शाम के-
जब सूरज डूबते ‘किदवई’ चाचा अपनी गाड़ी में आये और घर के बाहर खेलती हम तीनों बहनों से डिप‘ साब के बारे में पूछने लगे… हमारे कहने पर कि ‘बाबू जी तो दौरे पर गए हैं चाचा जी…’
उन्होंने झटपट निर्णय लिया- ‘अच्छा-अच्छा… तो आओ तुम तीनों को नुक्कड तक की सैर करा लाता हूं…. आ जाओ बच्चियों अंदर….

मैं तो खैर कुल चार की थी लेकिन आठ और दस की बड़ी बहनें भी जब तक कुछ कह पातीं, उनके ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल कर हमें अंदर बिठा दिया था। इधर ‘चाचा जी’ का लिहाज, उधर मां को न बता पाने का डर।
इन सबसे अनजान, किदवई चाचा अपने बेफ्रिक अंदाज में हमें शहर की सड़कों पर घुमाते और बताते जा रहे थे। बीच-बीच में पिछली सीट पर बैठी हम बहनों को नीबू, संतरे वाली खट्टी मीठी गोलियां भी थमाते जा रहे थे।

भय, अदब और शिष्टचार की मारी दोनों बड़ी बहनें, बीच-बीच में सहमे शब्दों में, ‘चाचा जी! देर हो रही है…’ अम्मा, बाबूजी परेशान हो रहे होंगे।’ जैसे वाक्य दुहराती जा रहीं थीं लेकिन किदवई चाचा पूरे इत्मीनान हमें आश्वस्त कर रहे थे- अरे तो कौन तुम लोग अकेली हो बच्चियों?मैं हूं न!… कह देना, किदवई चाचा के साथ गए थे….
अंततः हम लौटे। लेकिन तब तक सड़क पर पूरा अंधेरा घिर आया था- घर से थोड़ी दूर पर ही रामधारी लालटेन लिये आता दिखाई दिया…. (प्रतापगढ़ में तब बिजली नहीं थी…) और कार रोक कर पूछने पर बोला….
– ‘बहिनी-लोगों को देखने निकले हैं…. ‘साहेब’ दौरे से आ गए…
ओह! हमारे प्राण सूख गए।…
पत्तों से कांपते, डर से अधमरे, हम तीनों कार से उतरे।
हमारे अंदर लहर मारती दहशत बेकार नहीं थी। अहाता पार करते-करते पिता की तेज़ गरज सुनाई पड़ने लगी। जैसे पूरे घर में तूफान बरपा हो। मां से लेकर नौकर, महाराज सब पर गाज गिरी थी। (बहुत बाद में मां ने हमें बताया था कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद के उन दिनों में हिंदू-मुस्लिम दंगो के भड़कने की गुंजाइश और भय बराबर बना रहता था।)
थर-थर कांपती हम तीनों बहनों को हमारे इक्के वाले सईस की किनारे वाली कोठरी से अंदर ले जाया गया। वहीं से मां की आवाज सुनाई दे रही थी हमें- कहा न, तीनों बहुत रो रही हैं। कह रही हैं, अब कभी एसी गलती नहीं होंगी। गुस्सा थूकिये, बच्चियां रो रही हैं आपकी….
उस समय अपनी दोनों रोती बहनों पर मुझे बेतरह तरस आ रहा था। रो मैं भी रही थी लेकिन ज़ाहिर था कि मुख्य अपराधी दोनों बड़ी, ‘समझदार’ बहनें ही मानी जा रही थीं।

उस दिन का अपने अंदर का उबलता गुस्सा मुझे अभी तक याद है, ज्यादा अपनी बहनों की बेबसी और लाचारी पर कि उन्हें सफाई देने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? आप लोगों ने ही तो सिखाई है हमें, बड़ों से मुंह न लगने और जवाब न देने जैसी बातें। किदवई साहब हमें जबरदस्ती ले गए और नुक्कड़ तक के बदले टाउनहाल तक घुमा लाये तो हमारी गलती?… हम क्या कार से कूद पड़ते?
हमें तो तमाम सारी नसीहतें दी जाती हैं कि जोर से मत बोलो लेकिन इस तरह बेकसूर बच्चियों पर घर के मालिक का गरजना, तरजना और सहमी हुई मां से लेकर सारे घर पर कहर बरपा देना ‘पिता टाइप’ बड़ों को शोभा देता है क्या? तब हमें सिखाया गया शिष्टाचार कहां चला जाता है? ऐ? (मेरे अंदर के अदृश्य पृष्ठों पर जरूर यह सब दर्ज होता चला जा रहा था…. जो अब अनायास खुलता जा रहा है….)
गुस्सा मां के गिड़गिड़ाने पर भी आ रहा था। समूचा माहौल बेलज्जत और शर्मनाक महसूस हुआ था। साढ़े तीन-चार वर्ष की बच्ची को उससे कहीं ज्यादा समझ होती है, जितनी बड़े समझते हैं। (फिर से अपनी ‘माय नेम इश ताता’… कहानी याद आ रही है। कहानी में ‘ताता’ की लगभग यही उम्र है।)
ऐसे किसी प्रसंग पर, और प्रसंग तो घटते ही रहते थे, पिता का गुस्सा और हद से गुजरती अनुशासन-प्रियता दोनों मुझे बेहद नागवार गुजरती, बल्कि अत्याचार लगती। कभी घर के सबसे छोटे बच्चे की देख रेख के लिये रखे छोटे मुंडु को बीड़ी पीते देख कर, कभी बच्चे को गोद में लिये किसी और मुंडू के साथ धागे में कंकड़ बांध ‘लंगर’ लड़ाते देख कर, तो कभी पानी से भरे ग्लास में उंगली डाल कर लाते देखकर ही….. या फिर भूल से उसके मुंह से निकली कोई सड़क छाप गाली सुन कर…
कब कौन सा नौकर, किस गलती के लिए कितनी निर्दयता से पीट दिया जाएगा, कोई ठिकाना नहीं था।
नौकर तो नौकर, तय किये पैसे से ज्यादा पैसे मांगे या उदंडता से बोला तो रिक्शे वाला तुरंत पिट गया और बात का जवाब दिया तो चपरासी की छुट्टी…. और तो और, स्कूल में उनकी लाडली बिटिया को, घंटी बजने के बाद भी, कक्षा के बाहर, खंभे से खेलती देखकर, अध्यापिका ने अगर हल्की सी ठुनकी दे दी तो बेचारी अध्यापिका सस्पेंड।….
विरासत में मिली ऐसी उदंड क्रूरताओं की न जाने कितनी मिसालें, हमारी पीढ़ी की स्मृतियों में, दीवालों पर टंगी चीते, भालू की खालों सी दर्ज हैं।
ये बड़े लोग गुस्सा आने पर नौकरों को इस तरह पीटते कि नौकर कम हॉफता, वे खुद ज्यादा।….
लेकिन दुनिया का सबसे ममतालु पिता –
तो क्या इतना क्रूर था मेरा पिता भी!… लेकिन तब वह अपनी पत्नी, बच्चियों पर ही नहीं, बरामदे में टंगे पिंजरों में चहकती बज्जी और ललमुनियों तक पर इतनी ममता कैसे उडे़लता था!…
यह पिता हर हफ्ते पिंजरों के ऊपर पानी की धार डालकर, पंखों से पानी छिटकती ललमुनियों को प्यार से निहारता, उनकी कटोरियां साफ कर दाना चुग्गा डालता और टिहकारते मिठ्ठू को सहलाते देख जा सकता था!
इतना ही क्यों, आंगन के हौज की नारंगी, चित्तीदार, सुनहरी मछलियों को बगल में रखी पानी से भरी बाल्टी में डाल कर, गोल पत्थर की पूरी हौजी को खुरच-खुरच कर साफ किया जाता। नया, साफ पानी डलवा कर मछलियां वापस हौजी में छोड़ी जातीं। फिर बीचों-बीच का चुनार मिट्टी का ‘मरमेडों’ (जलपरियों) जैसी आकृति वाला फौव्वारा चालू किया जाता।
फैव्वारे से बरसती धारों में भींगने के लिए हमें बच्चियों को लालायित देखकर यही पिता, मुस्कुरा कर अनुमति भी दे देता।
यह पिता हर हफ्ते, पखवारे, स्वयं तौलिया बांधे, रामधारी के साथ पीली, हरी पत्तियों वाले क्रोटन से लेकर पाम, गुड़हल तक की गुड़ाई निराई करता। बैठक में सजे, बड़े-बड़े पीतल के स्टैंड वाले गमलों को पॉलिश से चमकाने के निर्देश दिये जाते। अलमारियों में फिट आइने पोंछे जाते। राजा रवि वर्मा के ‘गंगावतरण’ और हंस से संदेश भेजती जरी बार्डर की गुलाबी साड़ी वाली दमयंती के चित्रों के फ्रेम पुंछवाये जाते। दरी, कालीने झड़वाई जातीं। मां इन सबसे पूरी तरह असंपृक्त, आराम से घर छोटे मुंड, महराजिन को गृहस्थी के दूसरे कामों के निर्देश देने में लगी होतीं। यह उनका डिपार्टमेंट नहीं था।
हम बेटियों में किसी को तेज बुखार होता, यह पिता रात-रात भर ‘माथे पर ‘यूडी क्लोन’ की ठंडी पट्टी, और आइस-कैप रखे सिरहाने बैठा रहता। दसियों बार थर्मामीटर से बुखार नापता। नोट करता।
सन्नाटी रातों में गली से किसी अर्थी के गुजरने की आवाज आते ही वह अगल-बगल चारपाइयों पर सोई अपनी बच्चियों को थपथपाना नहीं भूलता- मैं यही हूं बेटे, डरने की कोई बात नहीं।
जी-बाबूजी… हम सहमी आवाज में कहते।
बसंत पंचमी की आधी रात जब इसपिता की अर्थी उठी थी तो सबसे पहले यही याद आया था।…
बांसुरी पर अल्हैया बिलावल और ‘जागो मीनोल…’
यह पिता दुर्द्धश ऊर्जा का धनी था। यह बांसुरी पर अल्हैया विलावल और हारमोनियम पर राग पीलू की बंदिशें निकालता था। ‘अछूत कन्या’, ‘चंडीदास’ जैसी फिल्मों और जद्दन बाई की गाई बंदिशें भी पुरानी फिल्मों और शास्त्रीय गीतों के बीसों रिकॉर्ड, हमारे भोंपू वाले ग्रामोफोन पर बजाता था। हम बच्चियां बड़े चाव से चारों तरफ बैठ कर सुनती थीं।
मेरे लिए खास तौर पर मेरा प्रिय मान लिया गया गीत-
‘नन्हीं नन्हीं बुंदिया रे, सावन का मेरा झूलना-
एक झूला डाला मैंने अमंवां की डाल पर-
जी अमवां की डाल पर…
ऊंची-ऊंची पेंगे रे…. सावन का मेरा झूलना…
लेकिन सबसे ज्यादा उतावली से इंतजार होता,
कजली की अंतिम कड़ी का…
एक झूला डाला मैंने अम्मा की गोद में-
जी अम्मां की गोद में….
छोटी-छोटी पेंगे रे…. सावन का मेरा झूलना….
अक्सर मां भी हम सबके बीच कारपेट पर बैठी होतीं। इस लाइन पर सब एक साथ मुझे देखकर और मैं शरमा कर मुस्कुरा रही होती।….
फिर मेरे लिये लाया गया एक छोटे से मंजुदार प्रहसन का रिकार्ड-गुलाबो सिताबो के तमाशे…. यह पिता हमारे साथ कैरम, बैगाडेल, और सांप-सीढ़ी खेलता और खेलते हुए, मां को भी आकर शमिल होने की आवाज लगाना कभी नहीं भूलता था।
यह पिता दीवाली के हफ्ते भर पहले से गली में ‘लेऽऽ… दिया दियलीऽऽ’ की आवाज लगाकर मिट्टी के दिये बेचने वालियों के टोकरे उझलवा कर सारे दियों को पहले नादों में धुलवाता, फिर सूखने के लिए रखवाता था जिससे दीवाली की रात हमारे कटावदार मेहराबों वाले तिमंजिले मकान के चारों तरफ की मुंडेरों पर सैकड़ों दियों की कतारें जगमगा उठें।
अगली सुबह हम बच्चियां उन जल चुके दियों को बटोर कर टिकुरी से तीन-तीन छेद करके मोटे धागे डाल कर तराजू के पलड़े बनातीं, मोटी सीक की डंडी… और दीवाली पर आये खील, बताशों की दुकानें लगा, तौल-तौल कर बेचतीं। महीनों चलता यह खेल।
यही पिता दीवाली से तीन चार दिन पहले की रातों में, अपनी पलंग पर तांबे के पैसों की ढेरी लगाकर बैठ जाता। फिर हम बच्चियों में बराबर-बराबर बांट कर हमें तीन-पत्ती, ‘फ्लश’ सिखाता कि ‘पेयर’ से बड़ा ‘फ्लश’ और फ्लश से बड़ा ‘रन’… और सबसे बड़ा? तीन इक्कों वाला ‘ट्रायो….‘
ऐसा नरम, ऐसा सख्त और ऐसा ममतालु… कि हर रोज सुबह अपनी बेटियों को जगाने का एक नया तरीका ढूंढता। बेतुकी ही सही, तुकबंदिया जोड़ता और गा-गा कर अपनी बुलंद आवाज में मुझे जगाता….
जागो मीनोल (मिन्नी… यानी मैं),
(अब तो) आंखे दे खोल…
कुंए में ढोल,…. ढमाढम बोल
और मैं आंखे मुलमुलाती, मुस्कुराती उठ जाती।
बहुत सीधी, संतिनी सी बड़ी वाली लाडली बेटी को जगाने के लिए, कोमल छुईमुई सी सी पंक्तियां बनाते तो मंझली, तेज तर्रार जंबाज मंझली बहन के लिये ‘हंटर वाली’ नुमा एक पूरी मसखरी स्क्रिप्ट… कि-
– ‘जानती हो तुम लोग?जब हमारी झांसी की रानी जैसी सुलक्षणा, सविता, ससुराल जायेगी और अपनी आदरणीया सासू जी की किसी गलती पर धाड़ से बेलन चला देगी न!…. तो कराहते-कराहते बेचारी औरत जो ख़त मुझे लिखेगी, उसका मजमून कुछ इस तरह का होगा कि-
‘श्रीमान बाबू डिप्टी साहेब बहादुर जी, के चरणों में सादर दंडवत… प्रणाम…. आगे समाचार यह है कि मेरे बेटे ‘झगडू की दुलहिन ने’ मुझ बेकसूर को दो बेलन मारा है- हल्दी चूना लगाकर पड़ी दर्द से कराह रही हूं।
अब आप से करबद्ध बिनती है कि मुझ पर रहम करिए। खत को ‘तार’ समझिए, जल्दी से जल्दी आइये और अपनी सुलक्षणा ‘सुपुत्री’ को ले जाइये… मैं वादा करती हूं, जरा ठीक हो जाऊंगी तो बल्कि आप फिर वापस पहुंचा जाइएगा….
हा-हा ही-ही की किलकारियों से सारा घर नहा उठता और दंबग मंझली, ताबड़तोड़ बाबूजी की पीठ पर छोटे-छोटे मुक्के मारने लगती…. हां, मुक्त-विनोद के उन प्रहसनी क्षणों में यह सब कुछ माफ, सबकुछ की मंजूरी हुआ करती थी।
पुरूषवर्चस्वी ज्यादतियों स्त्री-वादी ललकार और कन्याभ्रूण हत्या के आतंकित कर देने वाले इस समय में ऐसी सलोनी सच्चाइयां कुछ काल्पनिक, अतीन्द्रिय किस्म की सी ही लगती हैं न!… जबकि है यह एक अति सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के पिता का सच-
वह समय…. या यह समय….. दोनों हमारे ही तो बनाए हुए हैं… पता नहीं क्या, कैसे…. और क्यों हम ही समय के हाथों अवश, अशक्त होते चले गए।…..
आंखों में आंसू और ज़बान पर परोडियां-
यह पिता मेरी मां से जी भर कर नोंक-झोंक किया करता। मखौल उड़ाता नहीं, मखौल करता। कभी उनकी मिर्जापुरी कजलियों की पंक्तियां सुना कर खिझाता तो कभी मां की किसी पुरानी सखी को लेकर चिढ़ाता…. जिसके बादामी पोस्टकार्ड में, मां के लिये ‘सखी जी’ तो पिता के लिए ‘सखा जी’ लिख कर आया होता। सारी ठिठोलिया कुछ इस तरह कि चैंतीस की मां से लेकर हम चार, छ, आठ बरस की बच्चियां तक उसमें शमिल हो लेते।
गंभीर शेरो शायरी से लेकर राम चरित मानस की चैपाइयों तक की जाने कितनी द्विअर्थी पैरोडियां उनकी जबान पर होतीं। एकाध तो मुझे अभी तक याद हैं…. जैसे –
‘जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवश नरक अधिकारी’
को – जा, ‘सुराज’! प्रिय प्रजा दुखारी….
‘हेसुराज!’ वापस जाओ…)
कह कर इस तरह बुलंद आवाज में तरन्नुम से सुनाते कि सुनने वाले लहालोट….
यह पिता जितनी वाक्पटुता से छतफोड़ ठहाके लगवाता उतनी ही मृदुता से नरोत्तम दास का सुदामा-चरित पढ़ कर अपनी आंखें डभाडभ कर लेता…. जहां कृष्ण, परात के पानी से नहीं, अपने आंसुओं से सुदामा के कांटो बिंधे पैर धो रहे होते हैं-
देखि सुदामा की दीन दसा,
करूना करि कै करूणा निधि रोये।
पानी परात को हाथ छुयो नहिं,
नैनन के जलसो पग धोये….।
उर्दू के किसी कवि का एक ऐसा ‘सुदामा-चरित’ हमारे घर में था जिसमें द्वारपाल द्वारा सुदामा के आने की सूचना पाकर कृष्ण का बेसुध विह्वल दौड़ पड़ते हैं यह भी पिता का बहुत प्रिय प्रसंग था- जब तब गा उठते-
श्री कृष्ण से प्रथम सुदामा,
या श्री कृष्ण सुदामा से पहले-
लेखनी नहीं बतला सकती,
दोनों में कौन मिले पहले….
संजीदी आवाज में, सस्वर गाई इन पंक्तियों पर पति-पत्नी दोनों की आँखें से बावड़ी, पोखर सी हो- हो जाती।…..

– सूर्यबाला
मोबाइलः9930968670
(लेखिका द्वारा लिखे जार हेआत्मसंस्मरण ’डिपसाहब की तीसरी बेटी’ से एकअंश।)





