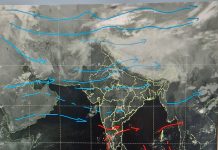मेरे मन/मेरी स्मृतियों में मेरे पिता
पिता को लेकर mediawala.in में शुरू की हैं शृंखला-मेरे मन/मेरी स्मृतियों में मेरे पिता। इस श्रृंखला की 45th किस्त में आज हम प्रस्तुत कर रहे है वरिष्ठ कथाकार, विलियम पैट्रसन यूनिवर्सिटी, न्यूजर्सी में हिन्दी भाषा और साहित्य की प्राध्यापक रहीं अनिल प्रभा कुमार को. ‘आवेश’, “संचेतना’, हंस, “ज्ञानोदय’ और ‘धर्मयुग’ में उनकी अनेक कहानियाँ प्रकाशित होती रही हैं .वे 1972 से अमरीका में निवासरत हैं और दस वर्षों तक न्यूयार्क में “वायस ऑफ़ अमरीका” की संवाददाता रही, सात वर्षों तक ‘विज़न्यूज़’ में तकनीकी संपादक के रूप में काम करते हुए उन्होंने कई कवितायें और कहानियाँ लिखी . उन्होंने बहुत ही बेबाकी से पितृसत्तात्मक समाज की अंदरूनी परतें खोलते हुए यह बताया है कि पढ़े लिखे परिवारों में भी सोच और व्यवहार में स्त्रियों का हमेशा दोयम दर्जा ही रहा। उसी का विरोध और खलबलाहट उनके व्यक्तित्व और लेखन में उतरे. उन्होंने उस काल खंड को रेखांकित करते हुए अपने आसपास के परिवेश के ताने बाने भी इस संस्मरण में बुनते हुए अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की यादों के साथ अपने पिता स्व. श्री सुदर्शन देव शर्मा के व्यक्तित्व की झलक प्रस्तुत करते हुए अपना संस्मरण लिखा है जो उनकी अपने पिता को भावांजलि है …….
पितृसत्ता का आदर्श पुरुष बहुत कठोर होता है। ठीक रसोई में रखे उन पत्थरों की तरह जिस पर अम्मा मसाला पिसती है। ये बहुत कठोर सोचता, बोलता है। वो अपने सोचने बोलने में पीस देता है, बच्चियों के बच्चा बनने की संभावना को, औरतों को इंसान समझे जाने के दृष्टिकोण को, इन सबको पीस कर वो स्त्रीत्व की अपनी नयी परिभाषा गढ़ देता है। पितृसत्ता का आदर्श पुरुष बहुत निर्मम भी होता है, इसके आंसू सुख चुके होते हैं ठीक उस शीशम की तरह जो अकाल पड़ने पर पत्ती विहीन हो चुका है.- अंजली यादव सम्पादन स्वाति तिवारी
46.In Memory of My Father-shri Sudarshan Dev Sharma: मेरे पिता पितृसत्तात्मक समाज के प्रतिनिधि थे- अनिल प्रभा कुमार
![]()
अनिल प्रभा कुमार
सलाखों को झकझोरते हाथ और हवा में लटकते पांव
मैं अपनी विस्मृति के उस तल तक पहुंच रही हूं कि उससे पहले जैसे कोई स्मृति थी ही नहीं |इतनी छोटी थी तब मैं | सच यह है कि यह घटना विस्मृति के गर्भ में ही थी | मुझे लगा कि मैं इसे भूल चुकी हूं पर जैसे-जैसे मैं बड़ी हो रही थी तो यह मेरे चेतन मन में कौंधने लगी | इसका आकार और रूप स्पष्ट और तीव्र होता गया | आज जब मैं जीवन परिस्थतियों के विषय में अधिक सजग और सचेत हूं तो यह घटना मुझे बार–बार आकर ललकारती है | गुहार लगाती है – “कुछ कर | अभी तक कुछ भी तो नहीं बदला|”
एक छोटा सा बुलबुला उठा था | सोचा , विलुप्त हो गया | हुआ नहीं | वह मेरे समय के साथ बढ़ता गया और इतना दैत्याकार हो चुका है कि उसकी छाया के नीचे समस्त दुनिया की औरतें आ गईं | एक बहनापा बन गया हम सभी में | तब मालूम नहीं था | मेरी संवेदना को भड़का देने वाली चिंगारी , मेरे लेखन का बीज शायद तभी उस घड़ी ही पड़ गया था | वह बहुत लंबे समय तक सुषुप्त अवस्था में रहा पर मृत कभी नहीं था | उसकी नब्ज हमेशा चलती रही |
इतना याद है कि तब हम दिल्ली में उस बुलंद इमारत में रहते थे जहां के रहने वाले उसी तरह इसे छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे जिस तरह मेरे ननिहाल के लोग अपना सब कुछ लाहौर में छोड़कर जान बचाते हुए दिल्ली पहुँचे थे | तब हर बातचीत की शुरुआत यूं होती थी – “जब पाकिस्तान बना ——|” हालांकि तब तक पाकिस्तान बने भी काफी समय हो चुका था पर उसके ज़ख्म , उसके किस्से बताने वाली पीढ़ी इस विभाजन को न भूलती थी और न ही भूलने देती थी | हम जैसे बच्चों के लिए ये हॉरर स्टोरीज़ थी | हमारी कल्पनाओं में भी डर और आतंक ही छाए रहते |
पहली मंजिल पर हम और दूसरी मंजिल पर मेरी नानी और रिश्ते के मामा-मामी | तब तक मेरा कोई भाई पैदा ही नहीं हुआ था | किसके साथ खेलती ? चुपके से खिसक कर ऊपर चली जाती | नई ब्याही मामी बहुत प्यार करतीं और मामा खेलते तो नानी कुछ अच्छा- सा खिलाकर लाड़ करतीं | उस घर में रौनक थी और मेरे लिए वही आकर्षण |
वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी ज़रूरी थीं | पक्की लाल पत्थर की आठ सीढ़ियां| फिर एक चौड़ी सीढ़ी, दायीं ओर मोड़ पर एक और चौड़ी सीढ़ी|इस घुमाव के बाद फिर आठ सीढ़ियां | मुश्किल यह थी कि दोनों चौड़ी सीढ़ियों के मध्य में , ऊपर की तरफ एक छोटा सा रोशनदान था – लोहे की मजबूत सलाखों वाला | मेरे लिए वह बहुत चुंबकीय था | दिन में उस रोशनदान से रोशनी और हवा आती | पीछे जमीन पर खड़े पीपल के पेड़ की शाखाएं हिलतीं | धुंधलका होते ही वह शाखाएं भूत -प्रेतों की बाहें बन जातीं |

उस तरफ एक और दुनिया थी जिसके पात्र अदृश्य थे पर उनकी आवाज़ें मेरे बाल -मन को खींचतीं | मेरा मन वहां झांकने को आतुर | मैं अध-बीच की पहली और दूसरी सीढ़ी के मध्य वाली जगह पर संतुलन बनाकर , किसी तरह से उचककर रोशनदान के बढ़े हुए हिस्से को एक हाथ से पकड़ लेती|फिर नीचे की दीवार पर पैर घसीटते हुए, दूसरे हाथ से किसी तरह रोशनदान की किनारे वाली छड़ पकड़ती| पांव हवा में झूलते और मैं दोनों हाथों से सलाखों को कस कर पकड़े रखती | ठुड्डी सिल पर और सचमुच का बायस्कोप शुरू |
समझ में आ गया कि हमारा घर मुख्य सड़क पर था और उसके समानांतर पिछली ओर एक गली चलती थी | ऐन हमारे घर के पीछे , उस गली में ही यह एक बड़ा सा अहाता था जिसके तीनों ओर थे छोटे छोटे एक कमरे वाले घर और घरों में परिवार | रोशनदान के सामने जो सबसे स्पष्ट रूप से दिखता था वह दृश्य था एक भट्ठी का | एक बड़ी उम्र की महिला बड़ी मुस्तैदी से मक्की और चने के दाने भूनती रहती | उस जगह की चर्चा मैंने भट्ठी वाले घर के नाम से सुनी थी | वहां जीवन था | बहुत से लोग और बहुत सी हलचल | मैं तब तक उस रोशनदान से लटकी रहती जब तक मेरे छोटे -छोटे हाथों में उन सलाखों को पकड़े रहने का दम होता | पांव जमीन पर हैं या हवा में झूल रहे हैं, इन सबसे बेखबर |
एक दिन उसी जगह से अलग ही तरह का शोर सुनाई दिया | एक स्त्री की दिल दहला देने वाली चीखें | चीखों को दबाता हुआ एक सामूहिक कर्कश कोलाहल | मैं झट से उन सलाखों को पकड़कर लटक गई | उस छोटे से झरोखे से जो दृश्य देखा वह मेरी चेतना में तेजाब से लिखा गया | बचपन में ही मेरे मन की कोमलता दागी गई हो जैसे |
आठ – दस औरतों का झुंड | बीच में घिरी , पिटती , चीखती एक कम उम्र की युवती| एक आदमी लगातार उसे चप्पल, थप्पड़ों और घूंसों से बेरहमी से मार रहा था | युवती के सिर से खिसका हुआ दुपट्टा , कपड़े अस्त -व्यस्त और उस घेरे से बाहर भागने की कोशिश करती हुई वह | आदमी उसकी लंबी चोटी बड़ी बेदर्दी से खींचकर उसे फिर से वापिस घेरे में घसीट लेता | फिर से अंधाधुंध उसे पीटने लगता | बीच बीच में उसके पेट पर लात से भी प्रहार करता | उस औरत की पीड़ा और कलेजा चीरती चीखें | मेरी सांस रुकने लगी | मैं बहुत दूर थी , बेहद असमर्थ | लगा जैसे उसकी चीखें मेरे अलावा और किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थीं |
लोग जान-बूझ कर अंधे और बहरे कैसे हो जाते हैं, बहुत देर से समझ में आया | यह भी कि पितृसत्ता के कई रूप होते हैं | यह एक स्त्री को जानवर की तरह घेराबंदी करके सामूहिक हांका लगाने वाली भी स्त्रियां ही थीं | वे सब औरतें ही छिब्बीयां दे देकर , उस आदमी को जो शायद उस युवती का पति था , उसे और , थोड़ा और पीटने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं | उनके हाथ नचा -नचा कर ललकारने से वह आदमी जैसे और ऊर्जा से भर जाता |जितनी उस पिटती औरत की चीखें माहौल में कंपन भरतीं उतना ही वह अपनी मर्दानगी के जोश में और हिंसक होता जा रहा था |
मुझे लगा कि कुछ भयंकर घटित हो रहा है | मैंने पहली और आखिरी बार किसी अकेली , निस्सहाय औरत को यूं पिटते हुए देखा था | मेरी सांसें रुकने लगीं | शायद सलाखों पर मेरी पकड़ शिथिल हो गई या पांव लटकते हुए सुन्न | दिमाग सकते में था | उस उम्र के लिए यह समझ में न आने वाला एक भयंकर अनुभव था | चुपचाप ऊपर नानी के घर चली गई | किसी को कुछ नहीं बताया | शायद कभी भी किसी को भी नहीं बताया |
वर्षों बीत गए | मैं भूल गई होऊंगी शायद | सलाखें वहीं बरकरार रहीं | हल्की सी रोशनी और थोड़ी सी हवा आने के लिए | बस इतनी भर ही जगह थी |
मैं उसी घर में बड़ी हो रही थी अपने माहौल की सलाखों के साथ |ज्यों ज्यों मुझे होश आता गया मैंने अपने इर्द -गिर्द भी इन सलाखों की सख्ती महसूस करनी शुरू की | जब बच्ची थी तो हल्की कोमल बाड़ थी फिर मेरी उम्र के साथ -साथ उनकी कठोरता भी बढ़ती गई | यह पितृसत्ता की सलाखें थीं | पहरे थे , ढेरों -ढेर वर्जनाएं और निषेध |
वैसे मैं एक अच्छे -खासे शिक्षित परिवार से थी |माँ लाहौर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट की पढ़ी हुईं | इंटर पूरा किया पर बीए के प्रथम वर्ष में विवाह हो जाने से उसका अंतिम वर्ष पूरा नहीं कर पाईं | जिसका उन्हें हमेशा ताना सुनना पड़ा और उन्हें अफसोस भी बहुत रहा | मेरे नाना लाहौर के प्रतिष्ठित सिविल -सर्जन थे | एक रुतबेदार बाप की बेटी और तीन भाइयों की इकलौती बहन होने के बावजूद भी मेरी मां को लिंग-भेद का शिकार होना पड़ा | वह लड़की हैं , यह बात उन्हें बात बात पर महसूस करवाई गई | उनकी हर छोटी -बड़ी इच्छा को यह कहकर वहीं दबा दिया जाता कि शादी के बाद जो मर्ज़ी करना | वही सलाखें तब भी थीं और अब भी | मां सब कुछ समझतीं और मौन –प्रतिबद्ध थीं कि अपनी बेटी को वह कभी भी इस जीवन अनुभव से नहीं गुज़रने देंगी | आज सोचती हूं तो वह शिक्षित ,प्रगतिशील विचारों वाली,अपनी सुंदरता से अनभिज्ञ , एक पारंपरिक स्त्री का समर्पित जीवन जीने को आजीवन बाध्य रहीं |
मेरे पिता श्री सुदर्शन देव शर्मा ,का व्यक्तित्व कुछ इस तरह समझा जा सकता है –
उनका जन्म २ अप्रैल 1916 में बेदियाँ , ज़िला कसूर में हुआ। वह भाग अब पाकिस्तान में पड़ता है। उनका पैतृक घर दसुआ , पठानकोट में था। कहा जाता है कि दसुआ ही महाभारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था जहां पाण्डवों ने अपना अज्ञात वास बिताया।
मेरे पिता बहुत मेधावी छात्र थे। अपनी योग्यता के बूते अधिकतर छात्रवृतियाँ प्राप्त करते रहे। उन्होंने लाहौर के डी ए वी कॉलेज से ग्रेजुएट किया था। एम ए अंग्रेज़ी भाषा में और वह पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं।
मेरे दादा जी की नौकरी नहरों वाले क्षेत्र में होने के कारण वह अद्भुत तैराक थे। अपनी हॉकी टीम के साथ उन्होंने कई सुदूर स्थानों की भी यात्रा की। लिखने पढ़ने का रोग मुझे शायद उन्हीं से विरासत में मिला। वह शौक़िया अंग्रेज़ी में कविताएँ लिखते थे। जब मेरी लाहौर वासिनी माँ से विवाह हुआ तो तब तक मेरे पिता जी दिल्ली में बस चुके थे।

हम लोग हमेशा दिल्ली में ही रहे। उनके परिवार के सभी सदस्य दिल्ली में ही थे सिवाए मेरे दादा – दादी के। व्यापार में हाथ आजमा कर और सब कुछ घाटे में खो देने के बाद आख़िर उन्होंने टाइम्स ऑफ़ इंडिया में उप संपादक की नौकरी कर ली और बाद में उन्होंने वहीं से अवकाश ग्रहण किया। सारी उपलब्धियों और तमग़ों के बावजूद मेरे पिता पितृसत्तात्मक समाज के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। स्त्रियों को बराबरी और उनकी योग्यता का सम्मान , उनके चरित्र के शब्दकोश में नहीं थे। उनकी सोच और व्यवहार में स्त्रियों का हमेशा दोयम दर्जा ही रहा। उसी का विरोध और खलबलाहट मेरे व्यक्तित्व और लेखन में उतर आए।
मेरे पिता शिक्षा के स्तर पर उस ज़माने के इंग्लिश में एम ए और पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर रह चुके थे | अपनी हॉकी टीम के साथ काबुल तक का दौरा कर चुके थे | टाइम्स ऑफ इंडिया के सह-संपादक थे पर विचारों में वह कस्बाई, सामंती मूल्यों के घोर समर्थक ! मेरी दादी के रूढ़िवादी विचारों और संस्कारों के ध्वज वाहक |
अपने बच्चों से प्यार वह बेहद करते थे पर उन्हें अपने ढंग से जीने की स्वतंत्रता देने में विश्वास नहीं करते थे , खासकर स्त्रियों को|मेरे उपन्यास “सितारों में सूराख” का नायक जय जब तर्जनी उठा कर कहता है कि “बस , एक बार कह दिया न |”वह अकाट्य संवाद मेरे पिता का था | जिसके आगे कोई तर्क, कोई समझौता या संवाद की गुंजायश ही नहीं होती थी |
मेरे पिता शिक्षा के पक्षधर थे | पढ़ो ! वह हरदम यही आदेश देते | पढ़ाई करना एक सुरक्षित ज़मीन थी | मैं पढ़ने में अच्छी थी | उन्हें मेरी उपलब्धियों पर गर्व भी होता | उपलब्धियां वही जो उनकी खींची हुई लक्ष्मण रेखा के भीतर हों | घर में वह स्वयं मेरे लिए हिन्दी की पत्रिकाएं लाते | घर में बैठकर पढ़ो | मैं स्कूल में लेख पढ़ती | वाद -विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेती | अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों के सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करती | पापा जी खुश होते , सभी सिर्फ लड़कियों के स्कूल थे |
उनकी तनी हुई भृकुटी के संकेत स्पष्ट थे
किसी भी लड़के से मिलना, बातें करना मना था | चाहे वे मेरे ममेरे , चचेरे भाई ही क्यों न हों | हंसना तो वर्जित ही था | बिना कहे भी मुझे उनके बहुत से कानून मालूम थे पर समझ नहीं आते थे | मन पहले परेशान होता था | फिर एक विवश विद्रोह जिसमें उत्ताप नहीं था | वह बस इच्छाओं की रेत में दबा सुलगता रहा | समय आने पर मेरे लेखन में भी यह बहुत मंझ कर, रिस -रिस कर बह आया | कभी भी लावा बनकर विस्फोटक नहीं हुआ | मैंने इन बंदिशों को साधने का हुनर सीख लिया |
दिल्ली जैसे शहर में रहते-पलते हुए भी मैंने जान-बूझ कर वुमन कॉलेज चुना | जानती थी कि को-एड कॉलेज में रहते हुए पिता के अदृश्य आतंक का भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगी | कम से कम लड़कियों के बीच तो मैं सहजता से हँस बोल सकूंगी | इधर मैं युवा हो रही थी और उधर अदृश्य दीवारें मेरे पास और पास घिरती गईं | मुझे अकेले कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी | अक्सर मेरी मां साथ होतीं | मुझे इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी पर हर जगह तो माँ के साथ नहीं जाया जा सकता था | चाहे कोई गर्ल्स गाइड का कैम्प हो, कोई शादी ब्याह , किसी भी रिश्तेदार का घर मतलब जहां भी कभी कहीं किसी युवा लड़के के होने की संभावना होती – एक पत्थर पर लकीर खिंच जाती – नहीं | ऐसी लकीर जिसके आगे कोई तर्क , आंसू , उदासी के कोई मायने ही नहीं होते थे | बस , एक बार कह दिया न !
मेरी बेबस फड़फड़ाहट | दुनिया को रोशनदान के भीतर से देखती , किताबों की खुशबू से महसूस करती | छोटी छोटी ख्वाहिशें और बड़ी बड़ी सलाखें |मैं शादी के सपने देखती जिसका पर्याय था बस , पति के साथ घूमना और फिल्में देखना | प्रेमी का तो सवाल ही नहीं था | साथ की सहेलियां सब जगह जातीं , मस्ती करतीं | मासूम सी आज़ादी – फिल्म देखने की| याद नहीं उन्होंने कभी खुशी से स्वीकृति दी हो | पिक्चरें देखीं | मां को बताकर और पापा जी से छिपाकर | डरते -कांपते हुए ,धड़कते दिल और अपराध भावना के साथ | दिल्ली जैसे शहर में पली तो सीमित आजादी तो मिली पर उड़ान पर प्रतिबंध थे |
अपनी सहपाठियों के घर , उनकी सगाई या शादियों में जाने तक के लिए मुझे बहुत रोना -धोना और अनशन करना पड़ता | मेरी वह लोहे की छड़ें कभी अपनी जगह से हिली तक नहीं | मेरी सहेलियां कभी अपनी बंदिनी सहेली को मुक्त कराने के लिए समूह बनाकर आतीं | कभी अपने अभिभावकों को साथ लाकर मेरी पैरवी करतीं तो कभी कभी मुझे पैरोल मिल जाती | तब तक रो -रो कर बेहाल ,सूजी आंखों और मुरझाए चेहरे और बुझे हुए मन से मैं फिर से खिल नहीं पाती थी | चली तो जाती पर आनंद कहीं गुम हो चुका होता |
मुझे ये निषेध तब समझ नहीं आते थे | अब जब यौन- शोषण की बातें सुनती – समझती हूं तो लगता है कि शायद मेरे पिता मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे | काश वह मुझसे बात करते, समझा देते या मां के द्वारा ही कहलवा देते | उनकी क्रोध भरी चुप्पी या कभी हिटलरी दहाड़ के सामने मां की भी कुछ नहीं चलती थी | मेरा रोना -धोना , अनशन सब बे-असर | पापा जी कुछ भी सुनने की मानसिक स्थिति में नहीं होते थे और न ही हमारी हिम्मत होती कि उनके सामने कोई तर्क रख सकें |
ऐसे वातावरण में मैंने उसी झरोखे की तरफ़ मुंह करके सांस लेनी शुरू कर दी जहां से मुझे आक्सीजन मिल सकती थी | मेरे पास विचार थे , कलम थी और थी साहित्य के प्रति सहज अभिरुचि | मैं बहुत पढ़ती पर कोर्स के बाहर की पुस्तकें |अच्छी पुस्तकें पढ़कर एक अलग तरह के नशे में रहती | कुछ छोटा -मोटा लिखती भी | कॉलेज की साहित्यिक पत्रिका की संपादक थी | लिखने का रोग लग चुका था | कोई भी कागज़ का टुकड़ा हाथ लग जाए, पढ़ना शुरु | मेरे अंग्रेजी और उर्दू के विद्वान पिता को इतनी हिन्दी तो आती ही थी कि वह मेरी किताब पर नजर मार सकें | एक बार यूं ही नाम सुनकर मंटो की कहानियों की कोई किताब घर ले आई | तब ज्यादा समझ क्या ही आया होगा | शायद “खोल दो “ कहानी थी | विभाजन की कहानी है , यह तो समझें आ गया | साथ ही पता नहीं क्यों लगा कि शायद नहीं पढ़नी चाहिए थी | जैसे इसे पढ़कर कोई वर्जित गुनाह हो गया | मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी | शायद कहीं कुछ सतर्कता थी कि मैंने चाह कर भी कभी डायरी नहीं लिखी |
बहुत छोटी सी दुनिया थी मेरी | पुस्तकें , पत्रिकाएं , कॉलेज , सहेलियां और मां |मां से मिलने आने वाली स्त्रियों की बातें भी मैं खूब डूब कर सुनती | वही मेरा अनुभव क्षेत्र था | मेरी कल्पना के पंखों को उड़ान भरने के लिए अनुकूल हवाएं|
गर्मियों की छुट्टियां और आलसी, निकम्मे दिन |किसी निकट संबंध में एक लड़की थी , मुझसे थोड़ी बड़ी | उसकी मां हमारे घर आती और मेरी मां से बातें करती , मैं सुना करती | इस महिला का बात करने का ढंग सबसे अलग था | कुछ कुछ दुनिया मेरी ठोकर पर जैसे लहजे में बात करती | मैं उसकी बातों के पार , उसकी असली तकलीफ को देखने की कोशिश कर रही थी तभी कुछ घुमड़ा मेरे भीतर | मैं उस लड़की की काया में प्रवेश कर उस दुखती रग तक पहुंच गई | मैंने एक ही बैठक में कहानी लिखी – खाली दायरे | लगा मैं किसी समाधि में हूं | लिखकर अजीब सी अनुभूति हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी | एक भीतरी सामर्थ्य का भी अहसास हुआ | मैं अपने दिल की बात निस्संकोच कागजों पर उतार सकती हूं |
संयोग यह हुआ कि इस कहानी को ज्ञानोदय के नई कलम अंक की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिल गया | कठिनाई यह हुई कि अब मुझे उन्हें अपनी तस्वीर भेजनी थी | मेरा दिमाग चीखा – खतरा ! कहीं अगर मैंने अपनी तस्वीर भेज दी और वह सुन्दर आ गई तो ? किसी पाठक ने पत्र लिख दिया तो मेरा मरण निश्चित था | मां के साथ चांदनी चौक के किसी स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाई | जानबूझ कर गाल फुला लिए , आंखें भेंगी कर लीं और चेहरे पर लड़ाकू भाव ले आई | मां के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था और मुझे अपनी जान बचा कर रखनी थी |

संयोग मेरे लिए नए- नए रास्ते खोल रहे थे | मैंने चोरी -चोरी किसी तरह यूथ फेस्टिवल के लिए एक रेडियो प्ले की तैयारी भी कर ली पर रिकॉर्डिंग के दिन तो बताना ही पड़ा | किस्मत से कोई रिश्तेदार हमारे यहां रह रही थीं | उन्होंने अपने ऊपर मेरी ज़िम्मेदारी लेकर मुझे आकाशवाणी के स्टूडियो तक पहुंचाया |
उसी तरह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने मुझे दूरदर्शन की किसी परिचर्चा के लिए चुना | मैं अपने सहज स्वाभाविक रूप में बोल रही थी और कंट्रोल रूम के भीतर बैठे प्रोड्यूसर किसी नई उद्घोषिका की खोज में थे | मैं बिना किसी टेस्ट के चुन ली गई | यह प्रतिष्ठा की बात थी पर पापा जी ? उन्होंने रोका तो नहीं लेकिन ज्यों ही तैयार होकर मैं पहले दिन घर से निकलने लगी तो पास आकर उन्होंने एक ही वाक्य बोला – “वहां जाकर आदमियों से ज्यादा बकड़ – बकड़ मत करना |”
इस वाक्य की सारी हदें मुझे समझ में आ गईं | जब तक मैं दूरदर्शन पर काम करती रही कभी सहज होकर सहकर्मियों से बात नहीं कर पाई | वही हाल यूनिवर्सिटी का था | कभी अपने किसी भी सहपाठी से बात तक नहीं की |जब जब मुझे रंगमंच पर अभिनय करने के प्रस्ताव आए मैंने स्पष्ट बता दिया कि मेरे पिताजी कभी इसकी स्वीकृति नहीं देंगे | मैंने स्वयं ही अपने को सलाखों की ओट में कर लिया था |
अच्छी बात यह थी कि मेरे पांवों में बेड़ियां थीं , मैं उड़ान नहीं भर सकती थी पर मेरे हाथों में हथकड़ियां भी नहीं थीं | मेरा मन, और मेरी कलम आज़ाद थी | कल्पना के पंखों पर सवार होकर , संवेदना का तार पकड़ कर मैं मनचाहा डूब -उतरा सकती थी | वह मेरा साम्राज्य था |
जैसे मेरे ही भीतर एक गर्भगृह था जिसमें एक लड़की नृत्य करती है| सपने देखती है और अपने ही मन में लिखे गए संवादों पर अभिनय करती है और फिर उसके द्वार पर अनुशासन , निषेधों का पत्थर रखकर बाहर निकल आती है | एक भली सी पढ़ाकू लड़की , घरघुसरी |

———–
कहते हैं न कि आप जब किसी के साथ हँसते हैं तो वह भले ही आपको याद न रहे लेकिन जब आप रोते हैं तो वह हमेशा याद रहता है | जीवन में दो महत्वपूर्ण अवसरों पर इन बंदिशों ने बहुत रुलाया | एम ए की अंतिम परीक्षाएं चल रही थीं | अचानक एक दिन मेरी मामी जी अपनी आठ महीने की गर्भवती बेटी और तीन साल की नातिन के साथ हमारे घर पहुंच गईं | उनके दामाद का भयंकर कार- एक्सीडेंट हुआ था और वह हमारे घर के समीपवर्ती अस्पताल में भर्ती था | हम दिल्ली मे थे तो वे लोग हमारे पास ही आकर रुके | मम्मी ने जल्दी से उन्हें ऊपर वाला कमरा खोल दिया | पापा जी का तनाव बढ़ रहा था | वह मेरी परीक्षाओं के कारण उनके आने से बेहद नाराज़ थे पर बात की गंभीरता को देखकर चुप कर गए | घर में बहुत तनाव पूर्ण वातावरण बन गया | वह बच्ची खिसक कर नीचे आ जाती और मैं उससे खेलने लगती | सब घबरा जाते | मम्मी मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बन्द कर देतीं ताकि मेरी पढ़ाई में कोई खलल न पड़े |
एक दिन मुझे पर्चा देने जाने से पहले थोड़ी घबराहट हो रही थी | लगा कुछ महत्वपूर्ण दोबारा पढ़ने की जरूरत है | मैं हड़बड़ी में पढ़ रही थी और उधर यूनिवर्सिटी जाने का वक्त भी क़रीब आ रहा था | एक आंख घड़ी पर और दूसरी अपने नोट्स पर | घर से बाहर आई तो समझ गई कि बस का इंतज़ार किया तो समय पर पहुंचना असंभव है | दूरदर्शन पर काम करने से थोड़ी पॉकेट-मनी मेरे पास हुआ करती थी | घर से निकलते ही एक खाली आटो दिख गया और मैं लपक कर चढ़ गई |
खैर ,परीक्षा देकर जब घर लौटी तो पापा जी का भयानक रौद्र रूप मेरी प्रतीक्षा कर रहा था | मेरे पिताजी लंबे कद के थे और उनकी नजरें बहुत तेज थीं | वह उस छज्जे पर ज़रा सा सिर आगे करके बहुत दूर तक देख सकते थे | उन्होंने मुझे बॉलकनी से ऑटो पर चढ़ते देख लिया था (यही बॉलकनी मेरी कहानी “बहता पानी” में प्रगट हुई है )| मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है|
मैं परीक्षाओं के कारण बहुत कम सो पा रही थी | ऊपर से घर में भी तनाव का धुआं | पापा जी के इस रौद्र रूप के आघात से बिखर गई| मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपराध क्या किया है | मेरा दिल दहला हुआ था | घर के शेष सदस्य शायद अस्पताल गए हुए थे | मैं एकदम निर्जीव सी अपने कमरे में दाखिल हुई और उसे अंदर से बन्द कर लिया | बिस्तर पर गिरकर मैं बिलख -बिलख कर रोई | शायद होश में रहते पहली बार इतना | मेरे दुख का कोई पारावार नहीं था |
मेरे विवाह की भी अलग कहानी है , वह फिर कभी | जब -जब मैं भारत अपने पति के बिना जाती तब -तब फिर से दोनों परिवारों की सलाखें यंत्रवत मेरे आस पास आकार सावधान की मुद्रा में तैनात हो जातीं | मां की मृत्यु के कुछ महीनों बाद मैं बदहवास सी अकेली ही भारत आई | अपने परिवार के साथ अपना दुख बांटने | तब तक मैं दो बच्चों की मां बन चुकी थी | अमेरिका में वॉयस ऑफ अमेरिका के लिए काम करती थी | उम्र की कई सीढ़ियां ऊपर चढ़ चुकने के बावजूद मां के अकस्मात चले जाने के दुख से छोटी बच्ची की तरह विह्वल थी | मैं परदेश में थी | मेरे लिए इस दुख की कोई पूर्णाहुति नहीं हुई थी | मैं सामान्य नहीं हो पाई कभी भी |
उन्हीं दिनों एक दिन मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान के दफ़्तर जाकर मृणाल पांडे से मिलने का कार्यक्रम बनाया | पापा जी को बता दिया | इनका आदेश भी आ गया कि भाई को साथ लेकर जाना |
भाई -भाभी ने मेरा मुंह ताका और मैंने उनका |
हम तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए जहां कनॉट प्लेस जाने वाली ऑटो मिलती थी |
भाई ने आटो रोका और कहा अब तू जा | हम अब अपने काम के लिए दूसरे आटो से चले जाएंगे |
दुर्भाग्य कि मेरे पिताजी ने बालकनी से थोड़ा सिर बाहर निकालकर , अपनी दूर दृष्टि के वरदान से सारा दृश्य देख लिया |
कुछ समय बाद मैं लौटी और उनके गुस्से का कहर मुझ पर ताबड़तोड़ बरसा |
मैं तिलमिला गई | अब मैं विवाहिता थी , खुद दो बच्चों की मां | कुछ दिन पहले ही अपनी मां को खो देने के दुख से जर्जर, मातृविहीना | उस वक्त मेरा अस्तित्व जैसे एक भरा हुआ ज़ख्म | यह आक्रमण इतना अकस्मात था कि मुझमें न तर्क करने की शक्ति थी और न बचाव में कुछ कहने की | इस बार शब्दों से मेरी ताबड़तोड़ पिटाई हुई थी |
“जब कहा था कि भाई को साथ लेकर जाना है तो फिर अकेली क्यों गईं?”
अरे , मैं एक लेखिका से , स्त्री से मिलने गई थी | किसी पुरुष के साथ मस्ती करने के लिए नहीं | कौन समझाता और कौन समझता ?
मेरे भाइयों और भाभियों पर उनका कोई अधिकार नहीं था | मां पर था और फिर मुझ पर | उन्हें कभी कोई तर्क समझ में नहीं आता था | बस उनकी सोच और उनका फरमान |
उनकी आवाज़ की दहाड़ से मैं शिथिल हो गई | इतना गलत अतार्किक व्यवहार !
मैं वहीं सोफ़े पर बैठ गई | अनियंत्रित होकर बिलखने लगी जैसे मुझे कोई दौरा पड़ा हो | कहां कहां से आकर सभी दुख एकाकार हो गए | वेग इतना प्रबल कि मेरे संयम का बाँध टूट गया |
पापा जी हमेशा की तरह अनदेखा करके दूसरे कमरे में चले गए | शायद पहले की तरह सोचा होगा कि आखिर कब तक रोएगी | अपने आप चुप हो जाएगी |
मेरा दुःख असीम था | यह एक बेटी की ही कारा तोड़ने की छटपटाहट नही थी | यह एक पत्नी , मां और दिल -दिमाग रखने वाली औरत का क्रंदन था | कब से स्थिर सलाखों पर सिर पटकने जैसा उन्माद | मुक्ति की गुहार लगाती आत्मा का रुदन |
मेरी सांसें शिथिल हो रही थीं और विचार धराशायी | था तो बस दर्द | अपनी अदृश्य मां के गले लगकर , बिलख -बिलख कर रोती हुई मैं |
शायद कमरे में अँधेरा घिर गया था , मुझे कुछ होश नहीं | आंखों ने देखा कि पापाजी ने धीरे -धीरे दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला और मेरे सामने आकार खड़े हो गए |
”मुझे माफ़ कर दे |” मैंने सिर उठाया और उन्हें सूनी आंखों से बस देखती रही |
“तेरी मां भी अब यहां नहीं है | मैंने तेरा दिल दुखाया |” वह कहीं और देखकर बुदबुदाए |
मेरे पिता जिनके मुंह से मैंने कभी अपनी गलती मानने वाला कोई शब्द सुना ही नहीं था इस समय मेरे सामने खड़े थे |
“मुझसे गलती हो गई | मुझे तुझे कुछ नहीं कहना चाहिए था |”
उनकी आंखें झुकी हुई थीं और उनमें दयनीयता थी |
मैंने यह कभी नहीं चाहा था | सिर्फ अपने लिए थोड़ा आकाश , थोड़ी उड़ान भरने भर की जगह चाही थी | उनका यूं अपने अपराध भाव से झुक जाना मुझे और ज्यादा उदास कर गया | मैं अभी भी सुबक रही थी पर धीमे -धीमे | कुछ नहीं कहा मैंने | मुझमें कुछ कहने लायक बचा ही नहीं था |मैं भीतर से बिलकुल खोखली हो चुकी थी |
यह तो मेरे अनुभव और मेरी लड़ाई थी | बाद में जाना कि उस समय अधिकांश लड़कियां कमोबेश इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही थीं | पितृ सत्ता का अंकुश सभी पर हमेशा रहा, किसी न किसी रूप में | कइयों पर तो मातृ सत्ता का भी |हो सकता है कुछ अपवाद हों | निरंकुश तो अभी भी कोई नहीं |
मैंने बहुत शिद्दत से इस पराधीनता को अनुभव किया , अस्वीकार भी | मेरा विद्रोह न आक्रामक था और न ही विस्फोटक | वह भीतरी लावा एक शांत आकार लेता रहा | मेरा आक्रोश परिपक्व हो गया | न सिर्फ अपने लिए बल्कि सभी के लिए | मेरे अनुभवों ने मुझे स्त्री -पुरुष मात्र होने से ऊपर उठकर एक अलग ही विमर्श दिया और वह है इंसानियत का ,बराबरी का | मेरी टक्कर हर उन इस्पात की सलाखों से है जो मनुष्य को मनुष्य होने से रोककर , शेष हर वर्ग में उसे बांट देती है |
मेरे हाथ अभी भी रूढ़ियों और परंपराओं से निर्मित समाज की इन सलाखों को झकझोर रहे हैं | इनकी नींवों को हिला रहे हैं | इस बार पाँव हवा में नहीं जमीन पर टिके हैं | इस आशा से कि कुछ तो अंतर पड़ेगा | इसे पड़ना ही होगा |
अनिल प्रभा कुमार
मोबाइल : 973 978 3719
ईमेल : [email protected]