
कहानी
कोई शाम उदास ना हों
स्वाति तिवारी
पिछले दो माह से घर आ गया हूँ। लॉकडाउन के बाद दो महीने उसी शहर में रहकर ऑनलाइन काम करता रहा। बाद में पता चला मैनेजमेंट ने उन दिनों 70% सैलरी काट ली थी, यह कहकर कि कंपनी का सारा बिज़नेस मार्केट ठप्प है। पैसों की आवक बंद है तो सैलरी देना बहुत मुश्किल और अगर स्थितियाँ ऐसी ही रही तो अगले कुछ माह तक वेतन की स्थिति यही रहेगी या इससे भी कम। दरअसल ज़्यादातर नौकरियों की स्थिति इससे भी बुरी थी। एक तरह से मैनेजमेंट हमें निकाल कर अपनी बदनामी नहीं चाहता था इसीलिए यह कंडीशन रखी गई थी। शायद हम ख़ुद ही छोड़कर चले जाएँ क्योंकि बैंगलोर जो अब बेंगलुरु हो गया है, कर्नाटक की राजधानी, जिसकी जनसंख्या 84 लाख पार हो चुकी है, नगरीय जनसंख्या 89 लाख से ऊपर है.
भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर और पांचवा महानगरीय क्षेत्र, आईटी हब के नाम से मशहूर इस महानगर में आने वाले मेरे जैसे मध्यमवर्गीय परिवारों से इंजीनियर बनने वाले लाखों छात्र जाने कितने सपने लिए नौकरी के लिए चले आते हैं यहाँ। 30% सैलरी तो फ़्लैट के किराए को शेयर करने और रोज़-रोज़ बस के किराए में ही ख़र्च हो जाती है। अभी सारा मार्केट खस्ता हाल है ऐसे में लगी लगाई नौकरी छोड़ी भी नहीं जा सकती थी क्योंकि भविष्य का क्या भरोसा! कल को यह भी ना रही तो जेब-ख़र्च के लिए भी मुश्किल हो सकती है।

इसी महानगर में हम एक ही स्टेट के चार लड़के 2 बैडरूम-हॉल-किचन के फ़्लैट में रहकर कार्यरत हैं। एक साल से सब ठीक ही चल रहा था, व्यवस्थाएँ सब हो ही गई थीं। सुबह मेड आती थी जो फ़्लैट की सफाई के साथ-साथ सुबह का चाय-नाश्ता बना देती थी। घर सुव्यवस्थित रहता। लंच हम सभी अपनी-अपनी कंपनी के कैंटीन में लेते थे। शाम को टिफ़िन आ जाता। टिफ़िन-सेंटर भी बिलकुल घर जैसा भोजन दे रहा था।
हर संडे मल्टी में लगी कमर्शियल वाशिंग मशीन में, जो लॉन्ड्री रूम के नाम से जानी जाती थी, हम में से कोई भी जाकर लॉन्ड्री कर लेते। प्रेस के लिए सामने ही एक लड़का था जो प्रेस कर देता था। छुट्टी वाले दिन मूवी देख लेते या मॉल में चले जाते और मनपसंद का कुछ खा-पी लेते। कभी आसपास कोई पिकनिक स्पॉट पर चले जाते। दिन आराम से कट रहे थे। ना कोई तनाव, ना कोई बहस, ना हिसाब-किताब को लेकर कोई झगड़ा। बहुत आसान-सी व्यवस्थाएँ थी सबके साथ। फ़्रिज पर रखी डायरी हमारा सार्वजनिक बही-खाता थी। कोई भी जो कुछ भी लाता उस डायरी में नोट कर लेता जैसे ग्रॉसरी, सब्जियाँ, फल, ब्रेड, अंडे, सफ़ाई का सामान इत्यादि। ना कोई बताता, ना कोई पूछता।

माह के अंत में हिसाब-किताब हो जाता। जिसे जो ज़रूरत हो वही ले आता फ़्लैट में फ़र्निचर, फ़्रिज, माइक्रोवेव और गैस का चूल्हा लगे हुए थे। एक टीवी हम सब ने मिलकर ख़रीद लिया था। जब कभी भी सहकर्मियों के बीच रूममेट का ज़िक्र होता तो मैं बड़े फ़ख्र के साथ सबको बताता कि मैं लकी हूँ इस मामले में।
10 मई 2021 अचानक लॉकडाउन लगते ही जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई कि चलो थोड़ा रेस्ट मिलेगा। केवल सुबह-शाम एक साथ रूम शेयर करने वाले हम चारों लड़के अचानक फ़्लैट के अंदर बंद हो गए। शुरुआत बहुत अच्छी हुई सब जैसे भागते-भागते थके से चुके थे। छप्पर फाड़ कर मिली वर्क-फ्रॉम-होम की सौगात से प्रसन्न थे। चलो आराम से रहेंगे कुछ दिन। सब ने मिल कर खूब गप्पे लगाए। नेटफ्लिक्स पर फ़िल्में चलती रहती और हम चारों अपने-अपने लैपटॉप पर काम करते रहते।
खाने और बनाने का शौकीन अनिरुद्ध उन दिनों बड़े प्रेम से इंदौरी पोहा, उपमा, आलू के पराँठे, छोले-पूरी जैसा बढ़िया नाश्ता और लंच बनाता और तारीफ़ सुन-सुनकर फूल कर कुप्पा हो जाता। इतना अच्छा नाश्ता तो मेड भी नहीं खिलाती थी। लॉकडाउन के दिनों में हाउसकीपर के ना आने से सारे काम हम सभी मिलकर कर रहे थे। सुबह की चाय मैं बना देता और सामने वाले मिल्क पार्लर से जाकर दूध, ब्रेड अंडा,मैगी भरपूर मात्रा में उठा लाता। शाम का खाना अरविंद कभी खिचड़ी तो कभी दाल-चावल या पुलाव बनाकर तैयार कर देता शुरुआती समय अच्छा कट रहा था।

एक परिवार हो गए थे सब। ताश के पत्ते भी निकल आए, कभी तीन-पत्ती खेलते तो कभी रमी। लॉकडाउन वाले महीने की पहली सैलरी के पहले मिले एक ईमेल ने जैसे हम सबकी हवा निकाल दी। अब हाथ थोड़े-थोड़े टाइट होने लगे उकताहट की शुरुआत होने लगी थी। बंद घरों में बोरियत और बंद बाजारों ने एक उदासी पैदा कर दी। जो जोश शुरू-शुरू में था वह धीरे-धीरे कम होने लगा। शुरुआत अनिरुद्ध से हुई। एक रोज़ वह पड़ा रहा बिस्तर में। ना ब्रेकफास्ट बनाया ना ही लंच। वह उठा और ब्रेड-ऑमलेट खा कर फिर सो गया। उस दिन सब ने ही ऐसा ही किया ब्रेड-ऑमलेट खा कर सब पड़े रहे।
लॉन्ड्री रूम बंद होने से कई दिनों से बिना धुले कपड़े, गीले तौलिए यहाँ-वहाँ पड़े थे जो फ़्लैट में एक अजीब-सी गंध फैला रहे थे। कपड़ों की सीलन भरी गंध वातावरण में नकारात्मकता फैलाने लगी।सब अपने अपने-अपने लैपटॉप पर काम करते रहते थे पर अब घर के काम में किसी का मन नहीं लगता। घर के काम के लिए आने वाली बाई के ना आने से अब असुविधा हो रही थी। रोज़-रोज़ ब्रेकफास्ट में वहीं ऑमलेट-ब्रेड ख़ुद ही बनाना अब अच्छा नहीं लगता था। शुरुआत में बनाई सारी व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न होकर खल रही थी।
घर के वही काम रोज़-रोज़ करना, खाना बनाना, चौका-बर्तन, कमरों की सफ़ाई, टॉयलेट की सफ़ाई जैसे काम अब भारी लगने लगे। पहली बार लगा समय पर स्नान, ध्यान और प्रेस के कपड़े पहन कर तैयार होने में भी कितनी सकारात्मकता है। स्फ़ूर्ति का बड़ा कारण चुस्त-दुरुस्त रहना भी होता है। समय की पाबंदी भी। पर अब घर और मन दोनों जैसे बासी रोटी का डिब्बा हो गए थे जिसमें स्वाद और ताज़े भोजन की गंध नहीं होती तो भूख भी कहाँ जागती।
हल्की-हल्की शुरुआत होने लगी थी तनाव, फ़्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट और एक-दूसरे पर अव्यवस्थाओं के दोषारोपण के रूप में। इगो हर्ट होने के साथ अब मनमुटाव होने लगे और धीरे-धीरे बोलचाल बंद हो गई। बस काम हो तो बोलो। हॉल में यदि एक टीवी देख रहा होता तो दूसरे को डिस्टर्ब होने लगता। मोबाइल पर अगर कोई बात करता तो लगता दूसरे पर हमला कर रहा है। महेश का गिटार बजाना अरविंद के लिए सिरदर्द का कारण होने लगा लगता। अब स्थिति यह हो गई थी कि जैसे हम दुश्मनों के साथ रह रहे हों। सारा याराना ख़त्म होने लगा।
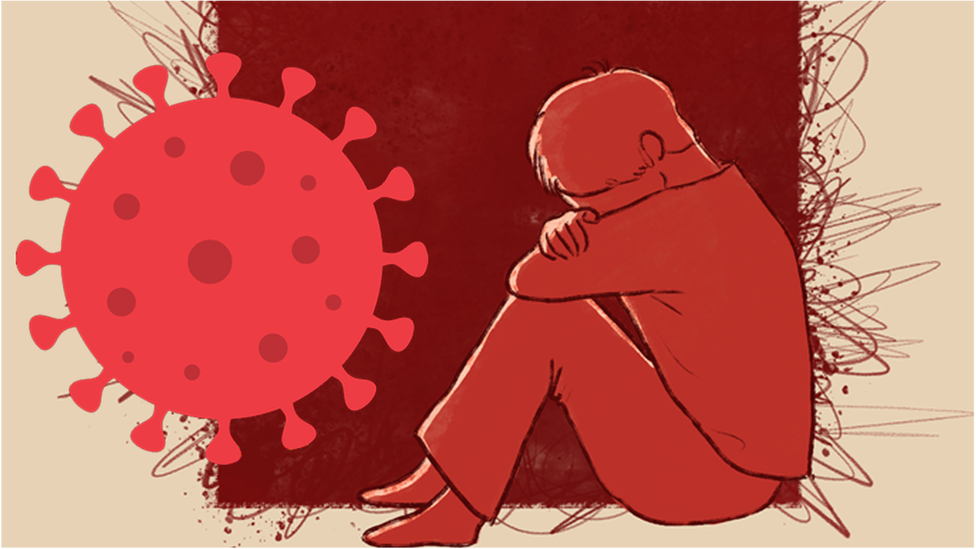
एक रूम में बैठता तो दूसरा उठ कर चल देता। अब बातें करने का भी मन नहीं होता चुप रहना ही बेहतर विकल्प लगता। परिणाम- उदासी और अकेलापन घेरने लगा जिसने कोरोना के संक्रमण के भय को जन्म दे दिया। सबसे पहले अनिरुद्ध को गले में हल्की-सी ख़राश हुई। अब घर के अंदर भी सब ने मास्क लगा लिए। असुरक्षा, हताशा, अकेलापन और असहाय करती स्थिति ने निराशा के बीज बो दिए जिसके अंकुर अवसाद के रूप में उगने लगे। धीरे-धीरे इस कोरोना की दूसरी लहर ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया।
सायरन बजाती भागती एम्बुलेंस, टीवी पर अस्पतालों की चीख-पुकार, व्यवस्थाओं का चरमरा जाना अब डराने लगा था। अकेलेपन का सबसे बड़ा सहारा सोशल-मीडिया ही तो था पर अब उस पर भी क्या देखें! किससे बात करें! दहशत और लाचारी व्हाट्सएप और फ़ेसबुक भी सबसे ज़्यादा थी। वहाँ हार चढ़े फोटो के साथ ‘ॐ शान्ति’ लिखते-लिखते भी थक गए थे; वे जैसे श्रद्धांजलि के मंच हो गए थे।
घर पर बात करते हुए भी मन डरता था। घर से फ़ोन आता तब हाथ और मन दोनों ही, काँपने लगते, मन बैठ जाता कि क्या पता कैसा फ़ोन होगा? क्या पता कौन कोरोना के संक्रमण में आ गया हो। कोई सूचना ना मिलाने पर हाथ स्वतः जुड़ जाते भगवान् के सामने कि चलो सब ठीक है। फिर एक दिन सबसे पहले संक्रमण की ख़बर अरविंद को मिली। उसकी दीदी संक्रमित हुई थी। उनके आइसोलेशन से लेकर आईसीयू तक अरविंद बेजान होने लगा था। उसके प्राण अपनी दीदी में बसते हैं उसके पिता के जाने के बाद एक दीदी ही तो है जिसने उसे इस मुक़ाम तक पहुँचाया। दीदी के लिए वह यहीं से सब मैनेज करता रहा। उनके अस्पताल जाने और आईसीयू के ख़र्चे ने अरविंद के सारे डिपाज़िट ख़ाली कर दिए। आर्थिक तंगी में अरविंद हम लोगों से बड़ी उम्मीद रख रहा था पर आर्थिक तंगी से गुज़रते हुए हम मदद करने की स्थिति में नहीं थे। यह वह भी समझ रहा था कि जेब में मुद्रा हो तो कोई मदद भी करें… नंगा क्या निचोड़ेगा!

फिर भी जो मदद बन सकती थी, कर रहे थे पर वह नाकाफ़ी थी; ऊँट के मुँह में जीरे जैसी। सुना तो था कि बूँद-बूँद से सागर बनता है पर इन दिनों तो अस्पतालों में थैले भर-भर कर डालने पर भी काम नहीं हो रहा था। परिवार-रिश्तेदार सब आर्थिक मदद दें तब भी कम ही पड़ रहा था रूपया। अस्पतालों के मुँह महिषासुर से हो गए थे कि भरते ही नहीं। अरविंद की दीदी 22 दिन में घर पहुँची तब तक अरविंद के पास 22 रुपए भी नहीं बचे थे। कैसा विकट समय था कभी कल्पना भी नहीं की थी किसी ने कि आपदा का ऐसा महा संकट यूँ दुनिया भर में आएगा? ना रुपये की वैल्यू थी, ना आदमी की। दीदी और माँ अकेली है। आफ़्टर-कोविड दीदी को देखभाल चाहिए पर अरविंद अपने घर दीदी के पास जाय भी तो कैसे? कोई साधन नहीं था और टैक्सी के लिए पैसे भी नहीं थे।
अवसाद ने सबसे पहले अरविंद को जकड़ा। उसने ठीक से खाना-पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। एक किताब पकड़े पड़ा रहता था। छत को ताकता हुआ… शून्य में कुछ खोजता–सा…। ये दिन और समय सबसे ज़्यादा उदासी भरे थे। चारों तरफ अवसाद का समय रहा। जैसे सब इच्छाएँ मर गई थीं। लगा था अब जीवन यहीं समाप्त हो सकता है। कौन जाने हममें से कौन घर लौट पाएगा। क्या पता घर लौटने पर घर में कोई मिले ना मिले.
ऑफ़िस से काम का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। मैनेजमेंट को लगने लगा था जितनी सैलरी दे रहे हैं उसका डबल वसूल कर ले। यह दबाव अब शरीर को तोड़ने लगा। बग़ैर टेबल-कुर्सी के लगातार काम थका देता। पलंग और गद्दे पर लैपटॉप पर लगातार काम करने से सबकी पीठ में दर्द की शिकायत हो गई। कुछ दिन पेन किलर खा-खा कर काम करते रहे फिर एक मित्र ने एक डॉक्टर का नंबर दिया था। नंबर कई बार मिलाने पर नहीं मिला। इंटरनेट से एक और डॉक्टर का नंबर मिला लेकिन वह टेस्ट-रिपोर्ट के बिना देखने को राज़ी नहीं था। टेस्ट मतलब गरीबी में गीला आटा यानी 3 हज़ार रुपए का बेवजह ख़र्च। घर से पैसे मँगाना भी जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी ज़रूरतों के लिए उनके पास कुछ तो रहे। रिचार्ज के अभाव में टीवी ने चलना बंद कर दिया था। अब फ़ोन ही सहारा था लेकिन फ़ोन आने पर फ़ोन उठाने का मन नहीं होता।
मेडिकल इमरजेंसी की इस भयावहता ने आहत मनों को बेबस और लाचार कर दिया। संक्रमण की भयावहता से अब पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में धीरे-धीरे ग्रॉसरी भी आसपास में मिलना बंद हो गई। ब्रेड और अंडे ही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सहारा बचे थे। खाने-पीने का सामान लगभग समाप्त हो रहा था। उकताहट-सी होने लगी थी ब्रेड खाते-खाते। और इसी दौरान अरविंद की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई। आइसोलेशन में एक कमरा चला गया। हॉल और एक कमरा हम तीनों के पास रहा। अब साथ रहना मजबूरी थी, पर सच बताऊँ कम-से-कम अनकही हिम्मत भी थी। अब फिर हम एक हो गए थे क्यूँकि अरविंद को बचाना हमारी प्राथमिकता में आ गया था। समस्याएँ थीं कि कम नहीं हो रही थी, पैसा था कि बच नहीं रहा था। इतने दिनों का साथ यूँ ही तो छोड़ा नहीं जाता।
अरविंद की दवाइयाँ लेने गया जो लगभग 14 हज़ार रुपयों की थी और जेब में केवल 7000 थे। मेडिकल स्टोर वाला पूर्व परिचित था मैं अक्सर वहीं से दवाइयाँ लेता रहा था। उसने उदारता दिखाते हुए दवाइयाँ उधार दे दी लेकिन अच्छा भोजन और अन्य ख़र्चे दिख रहे थे। अगर अरविंद को पर्याप्त प्रोटीन, पोषक तत्व, अच्छा भोजन भी ज़रुरी था। भोजन के साथ पौष्टिक तत्व और मिनरल्स ना दिए तो रिकवर होना मुश्किल होगा। अब दूध-ब्रेड वाले से ही पनीर भी ख़रीदने लगा। पैसों की कमी, रोज़-रोज़ उधार लेना मन को कचोटता। मैंने अपने सबसे प्रिय घड़ी दवाई वाले भैया के पास 10,000 रुपये लेकर गिरवी रख दी। यह सोच कर कि कुछ खाने-पीने का सामान आराम से आ जाएगा।
अरविंद 10 दिनों में लगभग ठीक हो गया था पर जैसे उसके जीवन की ऊर्जा को कोरोना खा चुका था। वह नर्वस था… बेहद नर्वस। उसने अपने दीदी को फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। मुझे फ़ोन करती दीदी रोने लगतीं, कहतीं, “बेटा उसका ध्यान रखना प्लीज़।” मुझे याद दिलातीं कि अरविंद बहुत भावुक है जानते हो ना निराशा में कोई ग़लत कदम ना उठा ले। प्लीज़ उसके साथ रहना।
एक बार फिर खाने का सामान ख़त्म होने लगा था। एक दिन दरवाज़े पर पार्सल मिला। अमेजॉन से आया था महेश ने अपने परिवार में बात की थी बॉक्स खोला तो देखा कि खाने-पीने का सामान था कई तरह के नमकीन, बिस्किट्स, अचार, बेकरी और दालें, मैगी के कुछ पैकेट्स, रेडीमेड के पैकेट्स, खाकरे जैसा बहुत-कुछ। उसी बॉक्स में कुछ ज़रूरत की दवाइयाँ भी रखी हुई थीं। यह पार्सल जीवन में फिर उम्मीद की तरह आया था।
अनिरुद्ध ने फिर खाना बनाना शुरू कर दिया था अब हम दिन में दाल-चावल बनाने लगे। एक समय अचार-नमकीन के साथ ब्रेड से काम चलाते। टूटता परिवार जैसे भी हो, जुड़ने लगा था। अब हम सब एक साथ खाना खाने लगे थे। महेश ने टीवी रिचार्ज करवा लिया था। अरविंद ने सभी को धन्यवाद दिया तो सब ख़ूब रोए। सबको लगा जैसे बिछड़ा परिवार फिर मिल गया हो। अचानक अरविंद ने पूछा था, “तेरी घड़ी कहाँ गई?”
“रखी होगी यहीं-कहीं मैंने बात को टालना चाहा।”
“पर तू तो कभी घड़ी निकालता नहीं था हाथ से!”
“घड़ी का क्या करना है… कौन रोज़ ऑफ़िस जाना है।”
“मतलब?”
“छोड़ यार! बुरी घड़ी निकल गई।”
“सच बता मुझे, मतलब तूने घड़ी बेच दी ना?”
“हाँ! मुझे बदलनी भी थी इसलिए।”
“साफ़-साफ़ क्यों नहीं बोलता कि मेरी दवाइयों के लिए… ”
“नहीं यार बेची नहीं, दवाई वाले के पास रखी है। पैसे देकर उठा लूँगा.”
“क्यों? क्यों किया तूने ऐसा?”
“तू चला जाता तो? बुरी घड़ी आ गयी थी ना, तब अच्छी घड़ी काम आ गयी।”
“ओह! और मैं तुम्हारे लिए क्या-क्या सोचता रहा? जो तुम लोगों ने किया वो तो मेरा सगा भाई भी होता तो क्या पता करता या नहीं।” वह फूट-फूट कर रोने लगा।
“मैंने उसका हाथ पकड़ा, “पगले, घड़ी दुबारा आ सकती है, लेकिन हम नहीं… तू वापस आ गया, दीदी घर आ गई इससे ज़्यादा अच्छी घड़ी और क्या हो सकती है!”
अरविंद और मैं रो रहे थे।
महेश ने बात को पलटा, “दिन बदल रहे हैं दोस्तों। अच्छे दिन भी आएँगे। देखो, आँकड़े कम होने लगे हैं। चला जाएगा यह संघर्ष का समय भी, थोड़ी सी हिम्मत की और ज़रूरत है। हम सब थोड़े घबरा गए थे तभी तो संक्रमण हुआ, पर अब हम सब एक साथ हैं अब कोई बीमार नहीं होगा।”
कुछ दिनों के बाद ने महेश ने बताया, “चलो अच्छी ख़बर आई है। तैयारी करो। चाचा भोपाल से टैक्सी भेज रहे हैं। हम सब भोपाल तक साथ चल सकते हैं।”
महेश का कहना था, “भोपाल तक सब लोग चलो। वहाँ से सबका जाना आसान हो जाएगा। भोपाल से जबलपुर, इंदौर, रतलाम के लिए कोई-ना-कोई साधन मिल ही जाएगा।”
हम सामान पैक करने लगे। सामान क्या पैक करना था बैग में भरना था। बिना धुले कपड़े, कुछ किताबें और अन्य आवश्यक सामान मिलाकर था ही कितना? एक राहत-सी मिली कि शायद अब इस संघर्ष से मुक्ति मिले। अब महसूस हुआ कि अपने देश में घर को मंदिर क्यूँ कहा गया है। हम कितने भी ग़रीब क्यों ना हों अभी-भी इतनी सामर्थ रखते हैं कि अपने बच्चों का, अपने सदस्यों का पेट भर सकें। दादी माँ कहती थीं, “घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। भारतीय परिवारों में स्त्री अन्नपूर्णा होती है, वह भूखा उठाती है पर सुलाती नहीं है।”
घर जाने का साधन मिल रहा है, यह बहुत बड़ी सहायता थी महेश के चाचा की। कम-से-कम भूख, अकेलापन और परिवार की कमी का संकट तो हटेगा। घर जाते हुए हम तीनों रूम भी छोड़ना चाहते थे वरना बेवजह 2 या 3 महीने का किराया भरना पड़ेगा और हो सकता है आगे लंबे समय तक वापस ना आ पाएँ तो फ़िज़ूल इतना सारा रुपया चला जाएगा। जब आना होगा तो ऑनलाइन किसी ब्रोकर से बात करके फिर कोई व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन अरविंद ज़िद पर अड़ा था कि वह घर नहीं जाएगा जब तक कि वह यहाँ रहकर सब के पैसे नहीं चुका देता। अरविंद का कहना था कि जब तक दवाईवाले से घड़ी ना ले आएगा तब तक वह बेंगलुरु नहीं छोड़ेगा।
“छोड़ यार,” मैंने समझाने की कोशिश की, “घड़ी नई आ जाएगी।”
“एक तारीख़ को सैलरी मिलेगी तो वह पैसे चुका कर घड़ी ले कर ही लौटेगा।” अरविंद की ज़िद के आगे हमारा कोई तर्क नहीं चला। हमने तय किया कि तब तक का मकान का भाड़ा हम सब शेयर करेंगे।
मन उदास था, छुट्टी मिलने पर ख़ुशी-ख़ुशी घर जाते वक़्त अलग बात होती है, लेकिन ख़ुशियाँ इन दिनों दूर चली गई थीं सबसे। महेश के चाचा की गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। हम सब अपना सामान गाड़ी में रखने लगे, मैं देख रहा था अरविंद के चेहरे पर एक अजीब बेचैनी। जैसे वह किसी मानसिक द्वंद्व में उलझा है। मुझे लगा उसके अंदर कोई युद्ध ख़ुद से ही ख़ुद के ख़िलाफ़ चल रहा है। शायद वह अपने आप से लड़ रहा था। कुछ है जो उसे परेशान कर रहा है वह अवसाद की स्थिति में तो था ही ऊपर से हम सब के जाने से एकदम अकेला हो जाएगा। मुझे पता है कि उसे अकेले में डर लगता है। पर क्या करता समझाने से वह समझ कहाँ रहा है? ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती थी।
निकलने से एक घंटा पहले भी उसे फिर समझाया था, “चले चल यार! क्यों ज़िद करता है। सब साथ ही वापस भी आ जाएँगे ना। थोड़े दिन की तो बात है। मन बदल जाएगा और घर-परिवार से भी मिल लेंगे। तुझे तो दीदी से भी मिलना है ना! दोनों भाई-बहनों ने इस संकट को झेला है। नया जीवन मिला है दोनों को। उन्हें ख़ुशी होगी तुझे देख कर। चल जल्दी तेरा सामान पैक करते हैं.”

वो नहीं माना, “जल्दी आ जाऊँगा बस एक तारीख़ को सैलरी मिल जाए। दवाई वाले के पैसे देकर तेरी घड़ी ले लूँ बस।” घड़ी को उसने जैसे अपने रुकने का बहाना बना लिया था।
निकलने से पहले हम सब से गले मिले। वॉशरूम से निकलते हुए मैंने अरविंद के किताबों के कलेक्शन में से एक किताब उठा ली रास्ते में पढ़ने के लिए। हम उसे छोड़ कर निकल गए। मन सभी का उसके साथ ही छूट गया था जैसे। थोड़ी देर तक रास्ते में अरविंद की ही बातें होती रहीं।
महेश का कहना था, “पहले तो वो ऐसा ज़िद्दी नहीं था। बीमारी के बाद से देख रहा हूँ अरविंद ज़िद्दी हो गया है।”
“हाँ, मुझे भी वह बदला-बदला-सा लगने लगा है। डर है कहीं गहरे डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए…”
भाग-दौड़ करते थक गए थे हम सभी। थोड़ी देर बाद सब चुप हो गए। चुपचाप बंद गाड़ी के शीशे से बाहर देख रहे थे। शहर जैसे सो गया था। बल्कि कहूँ निर्जीव-सा हो रहा था। बेंगलुरु जैसा शहर कैसा नीरस और बेजान-सा लग रहा है। ना शहर की रौनक बची थी ना चमक। सब फीका-फीका-सा दिख रहा था। मनुष्य अपनी गति भूल गया है जैसे, केवल ज़िन्दा रहने की जद्दोज़हद के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कैसा प्रकोप है यह, जिसने एक सुंदर शहर को उदास बना दिया। शहर को ही क्यों पूरी दुनिया ही इस जद्दोज़हद के रसातल में चली गई है। जीवन के लिए ऑक्सीजन, दवाइयाँ, डॉक्टर, वेंटिलेटर इसके अलावा कोई और शब्द बचे ही नहीं थे हमारे शब्दकोष में।
मन यह सब सोचकर फिर बेचैन होने लगा तो मैंने किताब उठा ली जो मैं अरविंद के कलेक्शन से उठा लाया था। सोच ही रहा था कि बीमारी ने आदमी को उसकी औक़ात बता दी थी। कड़वे सच को सबने स्वीकार कर लिया था। इतना ही रुपया-पैसा हो या पावर हो। आप प्रिंस चाल्स हों या अमिताभ बच्चन, धरती पर ईश्वर की मर्ज़ी के बिना जीवन संभव नहीं है। इन ख़यालों के चलते हमारी गाड़ी बेंगलुरु के कई क्षेत्रों को पार कर चुकी थी। जाने क्यों भय की एक लहर मन में उठी, मैंने पुस्तक पलटी। अन्दर दबा एक छोटा-सा कागज का पुर्ज़ा मिला काग़ज़ पर अरविंद की लिखावट थी लिखा था ——-
हर रोज़ हम उदास होते हैं
और शाम गुज़र जाती है
किसी रोज़ शाम उदास होगी
और हम गुज़र जाएँगे…
फिर कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह बने थे मेरा सिक्स्थ सेंस जाग उठा, ओह तो अरविंद की मनःस्थिति में बहुत कुछ चल रहा है। मैं चिल्लाया, “वापस चलो! भगवान की लिए वापस चलो!!! महेश फ़्लैट पर वापस चलो ———-”
“पागल हो गया है क्या?” महेश ने कहा, “जानता है न कई किलोमीटर दूर आ चुके हैं हम”
“हाँ जानता हूँ, अभी सिर्फ़ एक घंटा हुआ होगा…”
“हाँ! एक घंटा वापस लगेगा…”
“तो! और क्या कर लेगा वापस जाकर तू? क्या कुछ छूट गया है?”
“वापस चलो, वापस चलो, प्लीज़…”
“वापस जाना मतलब 1000-2000 का पेट्रोल और 2 घंटे! समझ रहा है ना? दोनों की ही बर्बादी।”
“बाक़ी सब बातें बाद में करेंगे। मुझसे ले लेना हज़ार-दो हज़ार। इस वक़्त वापस जाना बहुत ज़रूरी है वरना हम बहुत कुछ खो देंगे।”
ड्राइवर हमें लड़ते हुए देख रहा था। शायद उसने मेरे हाथ की पर्ची देख ली थी। उस ने गाड़ी मोड़ दी। जब फ़्लैट पर पहुँचे तो फ़्लैट अंदर से बंद था। मेरी जेब में एकस्ट्रा चाबी पड़ी थी जो रोज़ हम लेकर ऑफ़िस जाते थे। ताला खोल हम अंदर पहुँचे। अरविंद ने हमें भावशून्य निगाहों से देखा। वो पड़ा हुआ था पलंग पर। मैंने उससे लिपटते हुए पूछा, “तू ठीक है ना? तूने कुछ किया तो नहीं…???”
उसकी आँखों से खारा पानी भरने लगा।
उसकी बंद मुट्ठी को महेश ने खोला, “क्या हो गया है तुझे? यह क्या कर रहा था तू?”
“अलविदा दोस्तों…”
“महेश! उठाओ इसे गाड़ी में डालो।” ड्राइवर ऊपर फ़्लैट में आ गया था। हम तुरंत उसे लेकर सीटी हॉस्पिटल पहुँचे। दो घंटे की मशक्कत के बाद उसके पेट से नींद की गोलियाँ बाहर निकाल ली गई थीं। अब वह ख़तरे से बाहर था। देर रात उसे लेकर रूम पर आए। वह सो रहा था। महेश को टी-टेबल पर दो पंक्तियों का एक नोट लिखा मिला। लिखा था ——
मुझसे कटेगी नहीं ये उदास रातें
सूरज से कहूँगा मुझे आज साथ लेकर डूबे…
महेश ने मुझसे किताब में मिली स्लिप माँगी और पूछा, “ऐसा क्या लिखा था उसमें जो तूने इतनी जल्दी समझ लिया?”
“देख क्या बना है इसमें! महेश ने मुझसे किताब में मिली स्लिप माँगी और उसे पढ़ने, laga उसमें लिखा था-
‘हर रोज़ हम उदास होते हैं
और शाम गुज़र जाती है
किसी रोज़ शाम उदास होगी
और हम गुज़र जाएँगे…’
एक तरफ़ पेंसिल से कुछ उकेरा गया था – रेल की पटरी, नींद की गोलियों की शीशी, एक फ़न्दा, पंखा ,और… और एक चेहरा…।
डॉ .स्वाति तिवारी
Book Reviews : जीवन की सार्थक फिलसफी से रूबरू कराता उपन्यास







