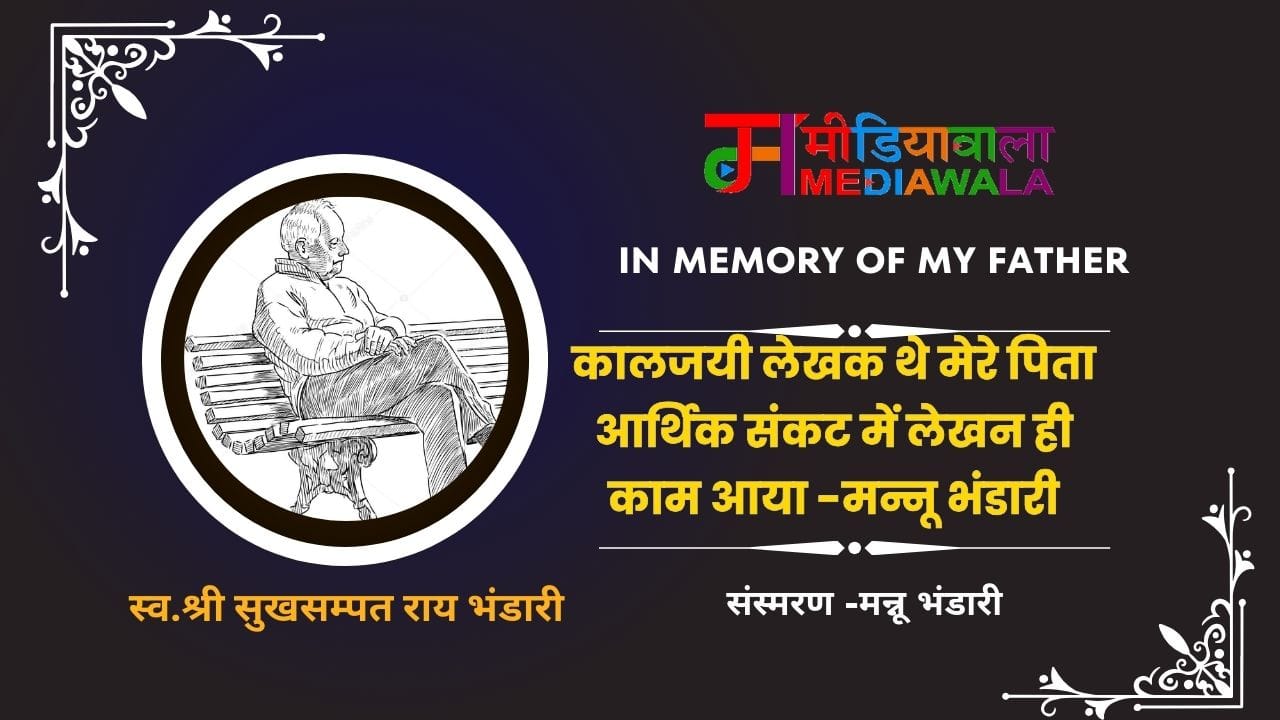
पिता पर संस्मरण/ मेरे मन/मेरी स्मृतियों में मेरे पिता
पिता को लेकर mediawala.in में शुरू की हैं शृंखला-मेरे मन/मेरी स्मृतियों में मेरे पिता। इस श्रृंखला की 39th किस्त में आज हम प्रस्तुत कर रहे है मेरी प्रिय कथाकार परम आदरणीय स्व.मन्नू भंडारी का अनूठा संस्मरण : स्मृति विशेष-हिंदी साहित्य की शीर्षस्थ कथाकार मन्नू जी की आज पुण्यतिथि पर उनका पिता पर यह संस्मरण मीडियावाला पर हमारी प्रिय सुप्रसिद्ध कथाकार आदरणीय सुधा अरोड़ा जी ने भेजा हैं . सुधा जी और मन्नू जी की मित्रता जग जाहिर है .यह संस्मरण इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अपने समय के कालजयी साहित्यकार पिता पर एक कालजयी साहित्यकार बेटी ने लिखते हुए इस संस्मरण के माध्यम से भारतीय समाज की पितृ सत्ता को लेकर भी अपनी बात कही है .सुधा अरोड़ा जी का आभार उन्होंने यह बड़े स्नेह और मनोयोग से हमें भेजा . मन्नू जी और बाबूजी को सादर नमन करते हुए यह मीडियावाला की विनम्र भावांजलि …………स्वाति


39.In Memory of My Father-Mr. Sukhsampatrai Bhandari :कालजयी लेखक थे मेरे पिता ,आर्थिक संकट में लेखन ही काम आया -मन्नू भंडारी
उम्र में माँ पिताजी से दस महीने बड़ी थीं। उस उम्र में लड़कियों को पति का अर्थ चाहे न समझ में आता हो पर ससुराल का अर्थ ठोंक-ठोंक कर समझा दिया जाता था। वे जब भानपुरा आईं तो पीपाड़ के अपने उस कच्चे, बेढंगे मकान की तुलना में यहाँ की इस भव्य दुमंज़िला कोठी को भरी आंखों से निहारकर उन्होंने ज़रूर अपने को ख़ुशकिस्मत समझा
होगा। उस हवेली का भारी दरवाज़ा जिसमें बाहर की ओर पीतल के बड़े-बड़े ख़ूबसूरत, नुकीले कुन्दे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आज तो वे दरवाज़े एक एंटीक-पीस की हैसियत रखते हैं। भारी तो इतने कि आज भी मैं शायद ही उन्हें खोल बंद कर सकूं ।
अन्दर घुसते ही एक चौड़ा-सा लम्बा बरामदा, जिसके दाहिने सिरे पर कोई पाँच फ़ीट ऊँचा एक लम्बा-चौड़ा मंच, जिस पर सफ़ेद चादर में ढँका बड़ा-सा गद्दा और तीन तरफ़ गाव-तकिए लगे रहते हैं। यह थी उस घर की मर्दाना बैठक, जो आज भी वैसी ही है। बरामदे के बायीं तरफ़ बीच में गोल आकार के बड़े दरवाज़े जितनी खुली जगह, जिसमें घर के अन्दर प्रवेश किया जाता है। अन्दर बीच में एक चौक जिसके बीचोबीच एक गोल चबूतरे में नीम का पेड़ लगा है। कहते हैं पिताजी के जन्म के समय जब उनकी नाल यहाँ गाड़ी गई थी तो मिट्टी और खाद के साथ कुछ निम्बौलियाँ भी वहीं गाड़ दी गई थीं। उस समय वहाँ जो नीम उगा वह आज तीसरी मंज़िल की छत तक गया पिताजी की उम्र का एक भरा-पूरा लहलहाता नीम का पेड़ है।


चौक के चारों तरफ़ कोई डेढ़ फ़ीट की ऊँचाई पर बने चौड़े-चौड़े बरामदे। बरामदों का कच्चाफ़र्श जिसे राती (लाल) मिट्टी से मिले गोबर से लीपा जाता और कभी-कभी, विशेषकर तीज-त्यौहारों पर उन पर बड़े-बड़े सफ़ेद माँडने माँडे जाते (जिसे आज हम अल्पना कहते हैं)। आज से कोई साठ साल पहले मैंने एक दीवाली भानपुरा में मनाई थी और तब माँडने के इस दृष्य की कला को देखा था। माँडने वाली औरत बिना पहले से कोई डिज़ाइन बनाए, हाथों में बालों का छोटा-सा गुच्छा लेकर उसे सफ़ेद घोल में डुबोती और शुरू हो जाती और देखते ही देखते उनका वह डिज़ाइन फैलते-फैलते एक बड़े से गोलाकार या चौकोर माँडने का रूप ले लेता।

तीन बरामदों में तीन अलग-अलग डिज़ाइन। मैं चकित रह गई थी उनकी उंगलियों की इस महारत पर। पता नहीं आज भी वैसी कलाकार स्त्रियाँ भानपुरा में हैं या नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों ने अपने कच्चे फ़र्श तो अब पक्के करवा लिये हैं।
शादी के एक साल बाद दादा साहब से छिपकर पिताजी दो लोगों की मदद से आगे पढ़ने केलिए जोधपुर भाग गए थे। भानपुरा में तो चार क्लास तक का स्कूल था, बस ! सो दादा साहब तो चाहते थे कि उसके बाद वे भी उनके धन्धे में लगें पर तेरे पिताजी तो पढ़ने के पीछे पागल, सो भाग लिए। पहले तो दादा साहब, दादी साहब ख़ूब ग़ुस्सा हुए पर फिर सन्तोष
कर लिया। रुपया पैसा भेजने लगे। सन्तोष था कि चलो, पढ़ ही तो रहा है। कोई ग़लत काम तो नहीं कर रहा है।““भाग कर गए आपको भी नहीं बताया? ”माँ हँस कर बोलीं- “ये आजकल की लड़कियाँ ऊ ज़माना री बाताँ न जानो… न समझो। उस ज़माने में शादी के बाद पति-पत्नी का बोलना तो दूर… चेहरा भी नहीं देखते थे। ब्याह कर आई तब से मेरी कोई बातचीत ही नहीं थी उनसे उस उमर में धणी-लुगाई (पति-पत्नी) कोई बात करते थे क्या, उन्होंने तो तब तक मेरा मुँह भी नहीं देखा था।‘ तब पिताजी की जीवनी में पढ़ी बात याद आई कि वे तो उस उम्र में न शादी करना चाहते थे, न दादा साहब का धन्धा। उन पर तो बस, पढ़ने की…कुछ बनने की धुन सवार थी। पर शादी तो उन्हें करनी पड़ी। हाँ, धन्धे में जुड़ने से पहले वे ज़रूर घर से ही भाग लिए।


यानी दादी ने शादी बेटे के लिए नहीं, अपने लिए की थी जिसमें उन्हें एक बहू मिले और जिसे डाँट-फटकार कर…घरवालों की सेवा में लगाकर वे अपना सा सपना संतुष्ट कर सकें। माँ अपवाद नहीं थीं… उस ज़माने में यही तो होता था। लड़की की शादी नौ-दस साल की उमर में कर दी जाती थी। हाँ, उस हालत में गौना ज़रूर दो-तीन साल बाद होता था, जिससे कम से कम वह सुसराल वालों की सेवा के लायक़ हो जाए। उन शादियों में लड़की के लिए शायद पति की तो कोई अहमियत ही नहीं होती थी। अहमियत होती थी तो केवल सुसराल की। पिता की ज़्यादतियों के खि़लाफ़ भी वह कभी एक शब्द तक न बोल सकीं। शायद इसीलिए मैंने कभी लिखा था कि मेरी सारी सहानुभूति हमेशा चाहे माँ की ही तरफ़ रही हो, पर वे मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकीं।

जोधपुर से पिताजी इन्दौर चले गए और वहीं उन्होंने अपनी दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की।(केवल दसवीं तक ही पढ़े थे पिताजी ! ) धीरे-धीरे उन्होंने वहाँ के सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र में केवल अपनी जगह ही नहीं बनाई बल्कि इन क्षेत्रों में उनका महत्व भी बढ़ता गया। अब पिताजी बराबर भानपुरा आते-जाते रहते थे और इस दौरान ही माँ से उनका सम्बन्ध भी
जुड़ा। दादी ने भानपुरा में ही अपने तीसरे-चौथे बेटे को जन्म दिया। चौथे बेटे के जन्म के कोई साल भर बाद माँ ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया पर शायद साल भर बाद ही शायद वह गुज़र भी गया। दूसरी बेटी भी जन्म के कुछ समय बाद ही गुज़र गई। दोनों बच्चे किन हालात में रहे… कैसे गुज़र गए मुझे कुछ नहीं मालूम। माँ तो अपने अतीत के बारे में कुछ बताती ही नहीं थी। वे किस भावनात्मक कष्ट से गुज़री होंगी, इसकी कल्पना मैं ज़रूर कर सकती हूँ। उस ज़माने में माँ-बाप के सामने अपने बच्चों को गोद में लेना भी पहले सिरे की बेशर्मी मानी जाती थी। पता नहीं, बीमारी के दौरान भी माँ उन्हें गोद में ले पाई होंगी या नहीं? कौन जाने दादी के सामने वे अपने बच्चों की मौत पर खुलकर रो भी पाई होंगी या नहीं
? पिताजी बच्चों के जन्म के समय भी भानपुरा आए थे और मृत्यु के समय तो आना ही था। उन्हें अपने बच्चों से बहुत लगाव था और उनकी मृत्यु पर वे बहुत दुखी भी हुए।
मैं कल्पना कर सकती हूँ कि माँ ने भी पिताजी के सामने ही मन में जमा हुआ सारा दुख उँडेला होगा। उसके बाद पिताजी माँ को इन्दौर ले गए और वहीं कुछ समय बाद मेरी सबसे बड़ी बहन का जन्म हुआ। उस समय तक पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी सो उन्हें हथेलियों पर ही पाला-पोसा गया। पिताजी के साथ माँ इन्दौर चली गईं । पिताजी अपने दोनों छोटे भाइयों को भी पढ़ाने के लिए इन्दौर ले आए थे… आठ-नौ विद्यार्थियों को भी घर में रखकर पढ़ा रहे थे। उनमें से कुछ तो भानपुरा के ही थे। आने-जाने वाले और मिलने वालों का ताँता तो लगा ही रहता था और जिनमें से कइयों के लिए पिताजी का आग्रह कि खाना यहीं खाकर जाएँगे, सो माँ तो सारा दिन रसोई में ही झुकी रहती। नौकर थे पर ऊपर के काम के लिए। खाना भी क्या, वही चार सब्ज़ियाँ, ढेर सारे आटे के पतले-पतले फुलके, हाथ की बनी मिठाई… सभी कुछ तो चाहिए था।

‘बहन जी भी बड़े प्रशंसात्मक भाव से जब-तब पिताजी के उस समय के यश की बात करती रही हैं और मैंने उनकी जीवनी में भी पढ़ा कि उन दिनों पिताजी का यश, उनकी प्रशंसा दिक् -दिगन्त में फैली हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए उनके क़दम राजनीति के क्षेत्र में उनकी सक्रियता, ज़रूरत मंदों की मदद, उनके व्यवहार की ऊष्मा…यश तो उनका फैलना ही था। पर क्या कभी किसी ने एक क्षण को भी सोचा कि इसमें से बहुत कुछ तो रात-दिन परिश्रम की चक्की में पिसती मेरी माँ के कन्धों पर ही टिका हुआ था। नहीं, किसी ने नहीं सोचा। औरत के लिए सोचता ही कौन था ? इसीलिए माँ के यश की बात तो कैसे कहें, उनकी प्रशंसा में भी कभी किसी ने दो शब्द तक नहीं कहे। माँ के शब्दों में ही कहूँ तो-“औरत जो भी करे वह उसका फ़र्ज़ और पति जो भी करवाए वह उसका अधिकार।“ और अधिकार- सम्पन्न व्यक्ति ही तो यश के भागीदार होते हैं। केवल श्रम ही नहीं, कभी-कभी ख़र्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो पिताजी माँ से उनके एक-दो गहने भी ले लेते और माँ बिना कुछ चूँ-चपड़ किए उनको दे भी देतीं। इतना तो मैं जानती हूँ कि उस ज़माने में औरतों को अपने गहनों से कितना प्यार होता था क्योंकि उसी में उन्हें अपनी सुरक्षा दिखाई देती थी। माँ अपने घर से भी गहने तो लाई ही थीं । इकलौती बहू होने के नाते दादी ने भी उन्हें शादी के मौक़े पर काफ़ी गहने दिए थे।
इन्दौर आते समय दादी ने माँ को उनके सारे गहने सौंप दिए थे। हर औरत की तरह माँ को भी अपने गहनों से प्यार तो ज़रूर रहा होगा पर पिताजी की ज़रूरत उन्हें शायद अपने प्यार से भी ज़्यादा बड़ी लगी होगी और वे चुपचाप गहने निकाल कर देती रहीं। यह अलग बात है कि उनकी भावनाओं की क़द्र कभी किसी ने जानी ही नहीं। यहाँ तक कि बड़ी बहन जी के मुँह से भी मैंने जब-तब यही सुना कि “माँ ने बस, रात-दिन हाड़-तोड़ परिश्रम करना तो ज़रूर जाना पर स्त्रा-सुलभ चतुराई तो उनमें धेले भर की नहीं थी। अरे, इफ़रात के दिनों में उन्हें अपने लिए और गहने बनवा कर रखने थे… रुपए बचाकर, छिपाकर रखने थे। हर औरत करती है यह सब, पर नहीं, बनवाना तो दूर वे तो बस अपने गहने भी निकाल-निकाल कर देती रहीं।“ भावनात्मक रूप से पूरी तरह माँ के साथ जुड़े होने के कारण बहन की इस टिप्पणी पर पहले तो मैं हैरान-परेशान। मन तो होता था कि कहूँ, ‘हाँ, पति के हर संकट के समय या मात्रा उनकी ज़रूरत के वक़्त भी अपने गहने समेट कर बैठ जाने वाली, पति को इनकार कर देने वाली चतुराई तो माँ में सचमुच नहीं थी । उनमें तो पति के हर संकट में उनकी सहायक बनने की मूर्खता ही भरी थी। पर उस समय कहा कुछ भी नहीं। लेकिन आज जब बहुत तटस्थ होकर माँ के व्यक्तित्व का विश्लेषण करती हूँ तो लगता है कि पिता की हर ज़रूरत के आगे कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह लगाए बिना मौन भाव से यों समर्पित होते चलना, उनकी उदारता या सहनशीलता थी या सही-ग़लत पर भी कुछ न कह पाने की उनकी अपनी कातर विवशता दयनीय असमर्थता। शायद यही सही है। कच्ची उम्र में ही दादी के राज में उन्हें जिस तरह दबाया गया… जैसी अमानवीय यातना दी गई उसमें वे बिलकुल सिकुड़ ही नहीं गईं, बुझ भी गईं बल्कि कहूँ कि एक तरह से निर्जीव ही हो गईं। इस निर्जीवता के चलते ही तो वे ज़िन्दगी भर दुलार और दुत्कार, प्यार और फटकार में, कभी अन्तर ही नहीं कर पाईं ।बस, सबको समान रूप से झेलती रहीं। हाँ, पिताजी से ज़रूर आज मेरा एक प्रश्न है… और उनके जीवित रहते, अपनी आँखों से देखने के बाद जिसके लिए मैं उनसे बराबर झगड़ा भी करती रही कि आपकी आकांक्षाओं के लिए जो पत्नी बिना किसी दुविधा और संकोच के अपना सारा श्रम ही नहीं अपना सारा धन भी, बराबर झोंकती रही उसे किसी तरह का श्रेय देना तो दूर, अपनी ज़िन्दगी में मात्र एक सेविका से अधिक किसी तरह की कोई अहमियत क्यों नहीं दी? कभी उसकी इच्छा- आकांक्षाओं के बारे में जानने की कोशिश तक क्यों नहीं की ? जो पिता दूसरों के प्रति बेहद सहृदय, बेहद संवेदन शील और बेहद उदार थे, माँ तक आते-आते क्यों उनकी सारी संवेदनशीलता सूख जाती थी, उदारता सिकुड़ जाती थी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई।
मुझे लगता है कि यदि माँ पिताजी से पहले चली जाती और उन्हें किसी और के यहाँ रहना पड़ता तभी वे शायद अपनी ज़िन्दगी में उनकी अहमियत को, उनके महत्व को समझ पाते, उनकी क़ीमत आँक पाते! पर ऐसा हुआ कहीं। इस सन्दर्भ में अचानक जैनेन्द्र जी की बात याद आ गई। पत्नी की मृत्यु के कोई पन्द्रह-बीस दिन बाद उन्होंने कहा था – ‘मन्नू, जब तक वह जीवित रही, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह भी है ! बस, जैसे है तो है ! – ‘पर जब से वह चली गई, सोते जागते, उठते-बैठते, रात-दिन बस, जैसे वही मेरे आगे-पीछे, मेरे मन में घूमती रहती है ! लगता है जैसे वह थी तो ही मैं ज़िन्दा था ! उसके जाने के बाद तो…. ( यह प्रसंग मैंने अपनी पुस्तक ‘एक कहानी यह भी’ में पूरे विस्तार से लिखा है )। ‘सोचती हूँ इन नामी-गिरामी यशस्वी पुरूषों की सीधी-सरल समर्पित पत्नियों के लिए उनकी ज़िन्दगी में अपनी क़ीमत अँकवाने के लिए, अपना महत्व मनवाने के लिए क्या मृत्यु का वरण ही अनिवार्य है ?
0
पिताजी के इन्दौर से अजमेर आने का जो कारण जाना तो मैं हैरान रह गई। जो व्यक्ति डेबिट- क्रेडिट तक का मतलब तक न जानता रहा हो, वह सट्टा खेले? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर सही है, जब आदमी के पास पैसा होता है तो घेरा बन्दी करने वाले लोगों की कमी भी नहीं रहती। वे लोग समझाते, सब्ज़ बाग़ दिखाते और पिताजी जब अपनी नासमझी प्रकट करते तो कहते कि आपको कुछ कहीं करना होगा, बस पैसा लगाना होगा और जो मुनाफ़ा होगा उसमें से कुछ प्रतिशत हमारा, बाक़ी आपका। शुरू में शायद कुछ कमा कर ही दिखाया होगा और बिना कुछ करे-धरे ही घर में आई इस लक्ष्मी से पिताजी की मति तो भ्रष्ट होनी ही थी, सो हुई। पर जब पासा पलटा तो ऐसा कि पिताजी को बिलकुल कंगाल करके छोड़ दिया। जिन लोगों ने दाँव लगाया था, उन्होंने बहुत समझाया कि दिवाला निकाल दीजिए। सट्टे का रुपया भी कोई चुकाया जाता है क्या? पर पिताजी नहीं माने। जिस इन्दौर में वे इतनी शान-शौकत से रहे, यशस्वी होकर रहे वहाँ दिवालिया बनकर रहते…यह तो उनके अहं और शायद उनकी नैतिकता को भी बर्दाश्त नहीं था। वे नहीं माने और अपने घर का सब कुछ स्वाहा कर दिया उन्होंने। माँ का गहना तो जाना ही था ऐसे में और माँ ने चुपचाप अपना तिनका-तिनका निकाल कर दे दिया और हाथ में काँच की चूड़ियाँ, गले में ‘बजट्टी’(मंगल-सूत्र का पर्याय) और सिर के ‘बोर’ के सिवाय उनके पास कुछ नहीं रहा। इन हालात में पिताजी के लिए इन्दौर में रहना सम्भव नहीं था। सो वे पत्नी, बच्चे और ढेर सारे क़र्ज़े के साथ अजमेर आ गए। अजमेर में आर्थिक रूप से पैर ज़माने के लिए पिताजी को उनकी पुस्तक ‘भारत के देशी राज्यों का इतिहास’ से बड़ी मदद मिली। पिताजी की इस योजना से प्रसन्न कई राज्यों ने अपने इतिहास की सामग्री के साथ-साथ काफ़ी पैसा भी दिया और पुस्तक छपने पर उसकी कई प्रतियाँ भी ख़रीदीं।
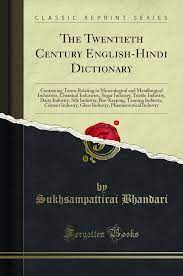
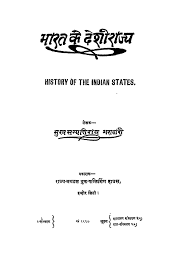
इसमें कोई सन्देह नहीं था कि राज्यों का यह सहयोग संकट के दिनों में पिताजी के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ और जैसे-तैसे उनके पैर अजमेर में जम गए।इस पूरे प्रसंग में पिताजी के अहं, उनके साहस और नैतिकता पर कितने क़सीदे काढ़े गए — बोलकर भी और लिखकर भी। मैं यह नहीं कहती कि उनके लिए जो कुछ भी बोला या लिखा गया वह ग़लत था ! नहीं, वे उसके हक़ दार थे। मेरी शिकायत बल्कि कहूँ कि तक़लीफ़ है तो केवल इतनी कि कोई दो शब्द माँ के लिए भी तो कह-बोल देता। क्यों नहीं कभी किसी ने यह महसूस किया कि माँ अपनी सहनशीलता, अपने धैर्य और हर स्थिति में अपने सहयोग से ही वह ज़मीन बिछाती चली जा रही थी, जिस पर खड़े होकर पिता यह सब कर सके। जिस माँ ने कभी किसी के विरोध में भी एक शब्द तक नहीं कहा, वह अपनी प्रशंसा में क्या कहती भला, पर पिताजी या कोई और तो कुछ कह ही सकता था। पर नहीं, कम से कम उस ज़माने में, जब औरत को ही कोई कुछ नहीं गिनता था तो उसके योगदान को भला कौन गिनता और क्यों गिनता जीवन भर और बाद में भी उपेक्षित रहना ही उनकी नियति थी, सो माँ ने भी उसे सहा और भोगा। अजमेर का मकान दुमंज़िला था।
ऊपर की मंज़िल में पिताजी का साम्राज्य था और नीचे की मंज़िल में हम भाई-बहनों के साथ माँ रहती थी। पिताजी की रियासत तो चली गई थी पर रईसी तो जैसे उनके ख़ून में मिली हुई थी जो अब जितनी भी और जैसे-तैसे निभ रही थी तो केवल माँ के बूते पर। मैंने देखा कि गर्मी के दिनों में पिताजी सोते तो माँ उन्हें पंखा झलने के लिए बैठती। दिन भर के काम से थकी-हारी माँ कभी ऊँघने लगती तो पिताजी की नींद उचट जाती और वे भन्ना पड़ते- “अरे, पंखा क्यों बन्द कर दिया…देखती नहीं, कैसी गर्मी पड़ रही है। “आखि़र एक दिन मैं बिगड़ पड़ी – “गर्मी क्या केवल आपको सता रही है, माँ को नहीं? “बिना कोई काम किए भी आपको तो रोज़ दिन में सोने को चाहिए पर अगर सुबह से मरती-खटती माँ को थोड़ी सी झपकी भी आ जाए तो यह गुनाह हो गया ? सुना तो माँ मुझ पर ही बिगड़ पड़ी – “क्यों करती है ऐसी बातें? उनको आदत है शुरू से सोने की तो सोएँगे नहीं क्या और गर्मी में थोड़ा सा पंखा झल दूँगी तो कौन सा घिस जाऊँगी। “पर लगता है पिता ने ज़रूर अपनी इस ज़्यादती को शायद महसूस किया होगा इसलिए जैसे ही ज़रा से रुपए हाथ में आए, उन्होंने एक छोटा-सा टेबल -फैन ख़रीद लिया।पिताजी ऊपर की मंज़िल से आवाज़ लगाते…अरे सुनती हो ज़रा पानी पिला जाओ तो माँ ख़ुद (नौकर से कभी नहीं) सत्तर सीढ़ियाँ चढ़कर उन्हें पानी पिलाने जाती और दिन में करीब आठ-दस बार उन्हें यह मशक्कत करनी पड़ती। एक बार मुझे ग़ुस्सा आया तो मैंने एक सुराही ले जाकर ऊपर रख दी – “प्यास लगे तो इसमें से निकाल कर पानी पी लीजिए। “पर फिर वही आवाज़। माँ के मना करने पर भी इस बार मैं ऊपर गई – “क्या बात है, सुराही तो रखी है इससे लेकर पानी क्यों नहीं पी लेते आप?” “अरे पर कोई ढालकर तो दे… जानती तो है, मुझसे यह सब नहीं होता।“ “यानी कि आप तो ढालने का काम भी नहीं कर सकते और माँ सारे दिन सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरने की झख मारी करती रहे?” “तू जा नीचे, क्यों जब देखो तब ऐसी-वैसी बातें करती रहती है ? मुझे तो कोई परेशानी नहीं, तुझे क्या परेशानी हो रही है। “पीछे खड़ी माँ सुराही में से पानी ढाल रही थी। “ठीक है आपको यह हम्माली करनी है तो करो। “और मेरा ग़ुस्सा साफ़ पिताजी से माँ की ओर कहूँ कि ग़ुलामी लगती थी, हो सकता है कि माँ को वह अपनी फ़र्ज़ अदायगी लगती हो और इसीलिए यह सब करते हुए उन्हें कष्ट नहीं बल्कि फ़र्ज़ अदायगी का संतोष…सुख ही मिलता हो। इतना ही नहीं, आर्थिक संकट के दिनों में क़र्ज़ माँगने के लिए भी माँ को ही जाना पड़ता था। लोगों को देने के लिए जिस
पिता की हथेली हमेशा उल्टी ही रही हो, माँगने के लिए सीधी होकर वह किसी के सामने फैले, यह उनके अहं और स्वाभिमान को बर्दाश्त ही नहीं था। दो-तीन परिवार थे, जहाँ से रुपए मिल जाते थे। ( रुपया आते ही तुरंत उन्हें लौटा भी दिया जाता था पर माँगना तो माँगना ही था और इस स्थिति से भी गुज़रना तो माँ को ही पड़ता था) एक बार की बात मुझे याद है। पता नहीं, पिताजी का पैसा कहाँ अटका पड़ा था और घर की हालत ऐसी स्थिति पर आ गई कि माँ खाना बनाए तो कैसे घर में सब्ज़ी लाने तक के पैसे नहीं। कोई पन्द्रह दिन से मैं अपनी टूटी चप्पल में कील ठोंक-ठोंक कर काम चला रही थी पर अब वह भी सम्भव नहीं रह गया था। हारकर पिताजी ने माँ को एक परिचित परिवार से पच्चीस रुपए माँगकर लाने को कहा। उम्मीद थी कि इनसे पाँच-सात दिन तो काम चल जाएगा और तब तक रुपया भी आ जाएगा। दोपहर में माँ रुपए माँगकर लाई, पर उसी दिन शाम को कम्युनिस्ट पार्टी के मिस्टर पन्नीकर आ गए और बोले- “भंडारी जी, मुझे दस रुपयों की सख़्त ज़रूरत है, जानता हूँ आपके सिवा कोई मेरी मदद नहीं करेगा, सो… “और पिताजी जब माँ से उन माँगे हुए रुपयों में से दस रुपए माँगने गए तो माँ ने ज़िन्दगी में शायद पहली बार विरोध किया, “अरे, आपको मालूम तो है कि मन्नू पन्द्रह दिन से टूटी चप्पल घसीट रही है, अब कॉलेज क्या नंगे पाँव जाएगी। सब्ज़ी छोड़िए, घर में एक बूँद घी तक नहीं कि दाल छौंक कर ही खिला दूँ। कह दीजिए कि इस समय… “माँ ने वाक्य भी पूरा नहीं किया था कि पिताजी एक़दम बिगड़ पड़े – “बेवकूफों जैसी बात मत करो – कितना विश्वास लेकर आए हैं वे मेरे पास और मैं उन्हें मना कर दूँ? “माँ ने फिर कुछ नहीं कहा, बस, चुपचाप रुपए लाकर दे दिए पर उनके जाते ही मैंने भन्नाना शुरू कर दिया – इस उम्मीद में कि कम से कम आज तो माँ भी मेरे स्वर में स्वर मिलाकर अपनी मजबूरी, अपना दुख ज़रूर व्यक्तकरेगी पर दुख जताना तो दूर उल्टे वे तो मुझे ही समझाने लगीं, “तूने नहीं देखे वे दिन सो कैसे समझेगी ? पर मैंने तो देखे हैं। हालात अच्छे थे तो कैसे दोनों हाथों से ज़रूरत मंदों को पैसा लुटाते थे….जान ले कि यह उदारता तो ख़ून में रची-बसी है इनसे माँगनेवाले को मना करना तो इनके लिए मरने जैसा है। म्हारी ही मत मारी गई थी जो मना करने लगी। “ सुना तो मैं हैरान, परेशान। किस मिट्टी की बनी है मेरी ये माँ, जिन्हें न कभी कोई दुख व्यापता है, न ग़ुस्सा। अभी भी इन्हें दुख हो रहा है तो पिता के बिगड़े हालात पर उनकी मजबूरी पर। लेकिन उनके इस रवैये पर मैं तो एकदम बिफर पड़ी – “दूसरों के लिए तो यह उदारता और घरवालों के लिए केवल फटी चरी। अरे, अब मैं बच्ची नहीं रही, ख़ूब समझती हूँ। दूसरों के लिए करो तो तारीफ़ वाहवाही जो मिलती है। घरवाले क्या तारीफ़ करेंगे और क्यों करेंगे…वह तो उनके फ़र्ज़ के खाते में चला जाएगा। और उन्हें तो हर समय तारीफ़ चाहिए। अब आपको फिर किसी के घर हाथ फैलाने भेजेंगे और आप हैं कि चली भी जाएँगी। कंगली बनकर हाथ फैलाती फिरें आप और उदारता की वाह वाही लूटें वे। “ग़ुस्से में और भी जाने क्या कुछ बोलती रही थी… पर माँ ने तो शायद सुना ही नहीं, वे भीतर चली गई थीं। आ कर उन्होंने मेरे हाथ में दो रुपए रखे… तू इतना ग़ुस्सा मत कर! आज ही नई चप्पल मँगवा ले (उन दिनों में दो रुपए में चप्पल आ जाती थी! ) मुझे नहीं मालूम कि बचे हुए रुपयों से उन्होंने क्या-क्या सामान मँगवाया मालूम है तो केवल इतना कि पिताजी को चार सब्ज़ियों वाला वैसा ही खाना खिलाकर दोपहर में वे बिना पिताजी के कहे ही पड़ोस के घर से पन्द्रह रुपए और माँग लाई और सुचारु रूप से घर की गाड़ी गुड़ काने लगी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि माँ की पक्षधरता के चलते मैं हमेशा पिता के गुणों की अनदेखी ही करती रही। उसका बोध तो मुझे तब हुआ जब बड़े होकर अनेक महत्वपूर्ण लोगों के मुँह से जब-तब उनकी उदारता, उनकी नैतिकता, उनकी सहृदयता और निपट अकेले अपने दम ख़म पर रचे गए उनके ‘अंग्रेज़ी-हिन्दी शब्दकोश’ की मुक्त कंठ से प्रशंसा सुनी। मैंने चाहे उनके गुणों की अवहेलना की हो पर माँ शुरू से ही शायद उनके प्रति सचेत थीं ! केवल सचेत ही नहीं, बल्कि एक भयंकर हीन-भाव से ग्रस्त भी रहती होंगी। बुद्धिजीवी पिता और निरक्षर माँ। पिता के सरोकार थे- देश की राजनैतिक स्थितियाँ…समाज की समस्याएँ और उनका कर्म क्षेत्र था केवल पढ़ना-लिखना। और माँ के लिए उनका घर ही उनका देश था और घरवाले ही उनका समाज, और उनका कर्म क्षेत्र था उनकी रसोई। अब दोनों का तालमेल हो तो किस आधार पर? ऐसी स्थिति में मेरी निरक्षर माँ को पिता की ज़िन्दगी में अपनी सार्थकता सिद्ध करने का शायद एक ही रास्ता दिखाई देता था कि उनकी हर इच्छा को, उनकी आज्ञा और उनकी हर उचित-अनुचित ज़रूरत को, उनका अधिकार समझ कर पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा करती रहे। बुद्धि से नहीं, रात-दिन की अपनी हाड़तोड़ मेहनत, अनन्त धैर्य और सहनशक्ति से ही पति की ज़िन्दगी में कम से कम अपने लिए थोड़ी सी जगह तो बना ले। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जगह तो उन्होंने बना ली थी, बल्कि वे एक तरह से अनिवार्य ही हो गई थीं पिताजी के लिए। पिताजी के सारे काम माँ के ज़िम्मे यहाँ तक कि कोष का नया भाग छपकर आता तो किताबों के बड़े-बड़े पार्सल तक वे ही सीतीं। घर में दो-दो नौकर थे पर पिताजी को किसी का काम पसन्द ही नहीं आता। माँ ने भी ऐसा काम कभी किया तो नहींथा पर सीखा और उनके मन-पसन्द पार्सल तैयार करने लगीं। उनके काग़ज़-पत्तर भी वे ही सँभालती। कभी कुछ गड़बड़ हो जाती तो पिताजी से ‘बे पढ़ी-लिखी , मूरख औरत’ के विषेशणों में लिपटी फटकार तो झेलनी ही पड़ती। ऊपर पिता के पास तीन खानों वाली एक बड़ी-सी राइटिंग टेबल थी. रोज़ शाम को एक टाइपिस्ट भी आता था, क्यों नहीं वे ख़ुद अपने सारे काग़ज़-पत्तर सँभाल कर रखते? नहीं, रखेंगी सब माँ ही। हर काम में हर क़दम पर रात-दिन पिता की हाज़िरी में रहने वाली माँ अनिवार्य तो थी ही पिताजी के लिए, पर किस क़ीमत पर? पिता को अपने हर काम में. हर समय माँ की उपस्थिति अनिवार्य लगती थी तो उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं कि माँ अपनी इच्छा से कहीं आएँ-जाएँ। यों तो उस ज़माने में औरतें वैसे भी ज़्यादा कहीं आती-जाती ही नहीं थीं पर कभी-कभी अपने सगे सम्बन्धियों के यहाँ मिलने….शादी ब्याह में शिरकत करने या जब-तब उपाश्रय में महाराज साहब के बखान (व्याख्यान) सुनने तो जाती ही थीं। पर माँ तो पिताजी की अनुमति मिलने पर ही कहीं जा पाती थीं। पर्यूषण पर्व के अवसर पर ही जब औरतें तो क्या, पुरुष भी चार-पाँच दिन उपाश्रय में ही गुज़ारते हैं माँ को केवल एक दिन जाने की अनुमति मिली हुई थी सो भी केवल तीन-चार घण्टों के लिए। आर्य समाजियों में दीक्षित होने के कारण पिता ने तो जैनियों के धरम-करम कभी माने ही नहीं। पर माँ अपने लिए क्यों कभी नहीं कह सकीं कि इन दिनों तो मैं तीन-चार दिनों तक ज़रूर जाऊँगी। नहीं, पिता की अनुमति तो हमेशा उनके सिर-माथे पर रही, उसके आगे अपनी इच्छा-अनिच्छा की औक़ात ही क्या भला ! लेकिन हद तो तब हुई जब एक बार भतीजे की शादी पर मामा ने बहुत-बहुत आग्रह ही नहीं किया बल्कि बहन को लेने के लिए किसी को भेज भी दिया। पिताजी ने भेजा तो सही पर इस हिदायत के साथ कि चार दिन बाद ज़रूर लौट आना । यहाँ की स्थिति से अनभिज्ञ मामा ने यह कहकर कि बरसों बाद तो आप आई हैं, माँ को दो दिन और रोक लिया। एक सप्ताह बाद जब माँ लौटीं तो
पिता जैसे इस ‘अक्षम्य अपराध’ के लिए आग-बबूला — ‘क्यों आई हो यहाँ…वहीं जाकर रहो…‘ माँ थरथराती रहीं…हाथ जोड़-जोड़कर माफ़ी माँगती रहीं – भाई के दुलार भरे आग्रह के आगे अपनी विवशता की बात बताती रहीं पर पिता के तेवर ढीले नहीं पड़े तो नहीं ही पड़े। पिता तो शायद अपनी शादी के बाद कभी अपने ससुराल गए ही नहीं, पर माँ पर भी ऐसी पाबंदी दोपहर में माँ थाली परोसकर खाने के लिए बुलाने गईं तो इन्कार कर दिया… “नहीं खाना मुझे खाना-वाना…जाओ यहाँ से। “माँ फिर रो-रोकर हाथ जोड़-जोड़ कर माफ़ी माँगने लगीं और बस, इसी बिन्दु पर मेरी सहनशक्ति ने जवाब दे दिया। अपने कमरे से निकलकर चिल्ला कर मैंने भी कहा- ‘क्यों ख़ुशा मद कर रही हैं आप? अरे अपने भाई के घर दो दिन ज़्यादा रह आईं तो क्या यह कोई ऐसा गुनाह है, जिसके लिए हाथ जोड़कर माफ़ी माँगी जाए? ग़ुलाम समझ रखा है क्या आपको? जाइए आप रसोई में। भूख लगेगी, तो अपने आप खाएँगे। “पर भीतर जाने की बजाय माँ के जुड़े हुए हाथ मेरी ओर मुड़़ गए- “क्यों बोल रही है मन्नू तू ऐसी बातें…. भगवान के वास्ते चुप कर और भीतर जा। “ग़ुस्से में मैं भीतर गई। करें भी तो क्या करें ऐसी माँ के लिए? जब-तब मेरे इस तरह के बकने-झखने का प्रतिवाद तो पिता ने कभी नहीं किया (करते भीभला किस आधार पर! ) पर बस मुझसे बोलचाल बन्द कर देते थे और यह अबोला कभी-कभी तो महीने भर तक भी चलता रहता।1947 में इण्टर पास करने के बाद मैं ख़ुद अजमेर छोड़कर भाई-बहनों के साथ रहने कलकत्ता चली गई। सोचा था वहीं से बी.ए करूँगी पर सितम्बर में जाने के कारण एडमिशन नहीं मिला तो प्राइवेट की तैयारी करने लगी। इस दौरान मैं अजमेर-कलकत्ता के बीच आती-जाती रही। जितने समय अजमेर रहती, कोशिश यहीकरती कि माँ-पिताजी के सम्बन्धों परबात न करूँ। बात भी क्या करती, उनके सम्बन्धों का तो वही पुराना ढर्रा और उन दोनों काअपना वही पुराना रवैया। फिर भी एक घटना का उल्लेख ज़रूर करूँगी। माँ के तीनों लहँगे काफ़ी फट चुके थे। कपड़े बेचने जो मदन फेरीवाला घर आया करता था वह दो-तीन महीनों से आ ही नहीं रहा था। उस ज़माने में मैं भी अजमेर में अकेले बाज़ार नहीं जाती थी तो एक दिन मैंने ही पिताजी से कहा कि शाम को जब आप बाहर जाते हैं तो माँ के लिए जैसे भी हो, दो लहँगों का कपड़ा ज़रूर लेते आएँ। उन्हें दुकान समझाई, किस तरह का कपड़ा लाना है, कितना लाना है, सब लिखकर दे दिया। वे भी बड़ी ख़ुशी से तैयार ही वहीं हुए बल्कि यह भी कहा, “अरे तुम्हारे लहँगे फट गए तो कहा क्यों नहीं… मैं लेकर आता। “तत्परता से दी गई इस स्वीकृति ने तो माँ के चेहरे पर दस गुना ज़्यादा ख़ुशी पोत दी। मैं और माँ पिता के लौटने की प्रतीक्षा में बैठे थे। कोई दो घण्टे बाद पिता लौटे…उनके हाथ में एक बंडल भी था। जैसे ही मैं उछल कर बाहर आई वे बोले – “अरे मन्नू’ देख तो आज क्या किताबें मिली हैं..कब से कृष्णा ब्रदर्स में इनको मँगाने के लिए कह रखा था- मँगाकर ही नहीं दे रहा था…आखि़र आज जाकर मिली हैं । तुझे तो इन विषयों में कोई दिलचस्पी ही नहीं पर अब बी.ए में आ गई है,पढ़ा कर कुछ ऐसी चीज़ें भी “ गदगदाते स्वर में वे बोले जा रहे थे।उनको बीच में ही टोककर मैंने पूछा- “और माँ का लहँगा?”
“अरे! “ वे जैसे असमान से गिरे – “ किताबें देखकर मैं तो एकदम ही भूल गया। कल- बस,कल ज़रूर ला दूँगा।“
मैं भी क्या कहती-फिर भी इतना तो ज़रूर कहा – “ज़िन्दगी भर माँ आपके लिए मरती-खपती
रहीं और आप आज पहली बार उनके लिए कुछ लेने गए और वह भी भूल गए।“
“अरे कहा न कल ज़रूर ला दूँगा।“ और वे अपनी नई किताबों में डूब गए।
मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, दूसरे दिन नौकर से ताँगा मँगवा कर मैं ख़ुद बाज़ार गई और माँ के लिएदो ओढ़नी और तीन लहँगों के कपड़े ले आई। माँ को कपड़े तो मिल गए पर जानती हूँ, यही काम यदि पिता ने किया होता तो । पर कैसे करते! मैं और माँ शायद भूल ही गए थे कि पिता ने तो अपने कपड़े तक कभी नहीं ख़रीदे। उनके कपड़े ही क्या, ता ज़िन्दगी खादी ही तो पहनी सो माँ ही भाइयों को खादी-भण्डार भेजकर उनके कमीज़-पाजामे के लिए खादी और सर्दी में गरम कोट के लिए पट्टू मँगवाती थीं।
0
एम.ए. करते ही मुझे कलकत्ता में ही नौकरी मिल गई तो अब साल में कुल दो बारछुट्टियों के दौरान ही अजमेर आ पाती और राजेन्द्र से शादी करने के कारण पिता की नाराज़गी के बाद तो वह भी छूट गया।
हाँ, उनके समाचार तो मिलते ही रहते थे। पिताजी को किस तरह अजमेर का घर छोड़कर भानपुरा जाना पड़ा और फिर बीमारी के कारण बड़े भाई के पास इन्दौर आना पड़ा, यह एक लम्बी कहानी है। बीमारी निकली — फूड पाइप में कैन्सर।सुना तो मुझे भी धक्का लगा। जानती थी कि मात्रा सौ डिग्री बुख़ार होने पर भी वे लेट कर जिस तरह माँ को सारे वक़्त सिरहाने बिठाकर रखते थे… ज़रा सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त न कर पाने के कारण ख़ुद तो परेशान होते ही थे, माँ को भी परेशान करते थे… वे कैन्सर की तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करेंगे? इस बीमारी के नाम से ही क्या हाल हो रहा होगा उनका और क्या हाल कर रखा होगा उन्होंने माँ का ! तभी उनके हाथ का लिखा एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें उन्होंने ज़िन्दगी के आखिरी दिनों का हवाला देकर मिलने के लिए बुलाया था। मैं और सुशीला उन्हें देखने गए पर जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं मिला… सिरहाने कैन्सर से सम्बन्धित कुछ किताबें और जर्नल्स रखे थे जिन्हें वे पढ़ते रहते और दो दिन
रहकर ही इतना तो समझ में आ गया कि वे यहाँ रहकर ज़रा भी ख़ुश नहीं थे। जिसने हमेशा दूसरों को अपने घर रखा हो, उसे जब मजबूरी में दूसरों के घर रहना पड़े तो उसकी तकलीफ़ का अन्दाज़़ मैं लगा सकती हूँ। यों अपना ही बेटा दूसरा तो नहीं होता पर भाभी का व्यवहार ही कुछ ऐसा था कि…। भाई तो सारा दिन नई खोली अपनी फैक्ट्री में जूटे रहते, उन्हें पता ही नहीं कि पीछे क्या होता है। बीमारी की तकलीफ़, दूसरे के घर रहने की तकलीफ़– ग़ुस्सा बनकर निकलती थी माँ पर। सुशीला जब पाँच-छह दिन बाद कलकत्ते के लिए रवाना हुई तो मैंने ग्यारह महीने की टिकूँ को उसके साथ ही भेज दिया, जिससे मैं पूरी तरह इन लोगों के साथ रह सकूँ माँ की तकलीफ़ में थोड़ी भागीदार बन सकूँ। उस समय माँ की असहायता — एक तरफ़ पिता की बीमारी और वहाँ रहने की तकलीफ़ से उपजा ग़ुस्सा, दूसरी तरफ़ भाभी की परेशानी भरी खीज से उपजती कटुता और दोनों के बीच पिसती मेरी माँ। न पति से कुछ कह सकती थीं, न बहू से, बस दोनों के सामने रिरियाती रहती थीं। किसी चीज़़ की ज़रूरत होती तो वे बहू से साधिकार नहीं माँग सकती थीं। उनके माँगने में तो ऐसी याचना भरी रहती थी मानो वे कोई अपराध कर रही हों। मुझे आज भी उनका वह याचना भरा स्वर, उनके चेहरे का वह अपराध भाव सब ज्यों-के-त्यों याद हैं। पिता के छाती के ऊपरी हिस्से में और गर्दन के नीचे के हिस्से में पता नहीं जलन होती थी या दर्द कि वे सारा समय माँ से वहाँ बाम लगवाया करते थे। बाम का सिलसिला ख़तम होता तो वे पैर दबातीं। यह सिलसिला रात भर, दिन भर चलता रहता । न समय से उन्हें खाना मिलता, न सोना ।

हाँ, जब लोग- बाग़ शाम को उनसे मिलने आते तो ज़रूर माँ को राहत मिलती। एक दिन मैंने माँ से कहा, आप जाकर खाना खाओ… मैं रगड़ती हूँ बाम। पर जैसे ही पिता के सिरहाने बैठी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। माँ जैसे-तैसे दो रोटी निगल कर वापस
उनकी हाज़िरी में आ बैठी। उन पन्द्रह दिनों में मैंने माँ को न जाने कितने बिन खाए दिन और अन सोई रातों से गुज़रते देखा । उम्र तो आखि़र उनकी भी थी ही पर उनके चेहरे पर मैंने न कभी थकान देखी, न परेशानी। हाँ, मिलने वालों के लिए रसोई में चाय-नाश्ता लाते समय, ज़रूर मैंने कभी-कभी उनकी आँखों में तराइयाँ देखी पर बस, शब्दों में उनके मुंह से कभी कुछ नहीं सुना। उन्होंने ज़िन्दगी भर दूसरों का केवल सुना ही सुना …सुनाया तो कभी किसी को कुछ नहीं।
0
कलकत्ता लौटने के कुछ दिन बाद ही मैंने सुना कि पिताजी नर्सिंग होम में शिफ्ट हो गए । उन्हें तो वहाँ जाकर बहुत राहत मिली पर माँ को ? नहीं, माँ को वहाँ भी राहत नहीं थी। विशेष अनुमति लेकर उन्होंने वहाँ भी माँ को रात-दिन अपने साथ ही रखा। बिना माँ के तो वे जैसे रह ही नहीं सकते थे। नर्स का जो काम होता वह कर देती पर रात-दिन की अनवरत सेवा-सुश्रुषा तो माँ के ही ज़िम्मे। तीन महीने नर्सिंग होम में रहकर नवम्बर के महीने में उन्होंने प्राण त्यागे। कलकत्ता में मेरे छोटे भाई उनकी बीमारी के दौरान बराबर इन्दौर के चक्कर लगाते रहे और आखिरी समय में भी वहीं थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि आखिरी दिन उन्होंने रात को अख़बार सुना। सन् 1962 के चीनी आक्रमण और साधन-हीन सैनिकों
की दिल दहला देने वाली दुर्दशा और करारी शिकस्त को लेकर वे बहुत दुःखी थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने प्राण त्याग दिए। मैंने छूटते ही पूछा था – “आखिरी समय में उन्होंने माँ से कुछ कहा?” “नहीं, कहा न, उनकी आवाज़ ही चली गई थी।“

पता नहीं, उस समय ख़याल आया था या नहीं पर आज ज़रूर सोचती हूँ कि आवाज़ चली गई थी तो क्या मात्रा एक स्नेहिल स्पर्श से ही वे माँ की ज़िन्दगी भर की गई सेवा के लिए कम से कम अपनी कृतज्ञता तो जता ही सकते थे? पर नहीं, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। उनकी सोच, उनकी चिन्ता तो देश के साथ जुड़ी थी। ठीक ही तो है, जिन लोगों के सरोकार बड़े सन्दर्भों के साथ जुड़े रहते हैं, परिवार वाले तो हमेशा उपेक्षा का पात्र रहने के लिए अभिशप्त ही होते हैं। कितने साल गुज़ारे थे उन्होंने उस घर में। उस घर का कण-कण जैसे उनकी आत्मा में बसा हुआ था। वहाँ के दुकानदार, फेरीवाले, पास-पड़ोस वाले, सब की बातें करती, पर सबसे ज़्यादा बातें करती पिताजी की। कटुता तो दूर की बात रही, पिताजी को लेकर कभी कोई शिकायत तक नहीं थी उनके मन में। मैं हैरान होकर सोचती कि जिस पिता ने ता ज़िन्दगी उन्हें एक सेविका की तरह ही रखा, उसके लिए भी ऐसी सद्भावना, ऐसा लगाव? पर नहीं, यह तो मेरासोचना है, वे तो शायद यही सोचती थीं कि यह पिता का उनके प्रति अटूट प्रेम ही था जो वेअपना हर काम माँ से ही करवाना चाहते थे, माँ पर इतना निर्भर रहते थे कि उनके बिना जैसे रह ही नहीं सकते थे। इसलिए तो नर्सिंग होम में भी ज़िद करके वे माँ को अपने साथ ही ले गए। माँ के लिए पिता की यह निर्भरता उनके प्रेम का प्रतीक थी तो रात-दिन पति कीसेवा में लगे रहने को माँ ने कभी अपनी मजबूरी नहीं समझा…यह शायद पति के लिएउनका गहरा प्रेम था।
पीढ़ियों का अन्तराल जहाँ बाहर बहुत कुछ बदलता है, वहीं सोच और परिभाषाएँ भी बदल ही
देता है।
मन्नू भंडारी
32 .In Memory of My Father : सेंचुरी बनाने से चूक गए पापा-सुधा अरोड़ा
34. In Memory of My Father-Dr. Chandrakant Devtale: मेरे पिता असाधारण कवि,अद्वितीय व्यक्तित्व







