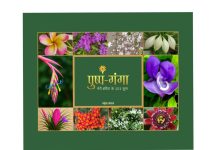Story : फिरा न मन का फेर
“नन्दू….”
फिर वही धीमी, सकुचाई, संशय से भरी पुकार, किसी अलंकरण या आलाप से रहित महज एक शब्द की धीमी पुकार। मैं घबराकर आँखे खोल देती हूँ। कमरे में गहन अंधकार है पर उस घोर अंधेरे में दमकता है उसका नन्हा गोल चेहरा। भरे गाल और गोल आँखों वाला वही नन्हा चेहरा जब वह मुझसे पहली बार मिली थी। उस चेहरे पर पसरे वही डर, हिचक, अपराधबोध के मिले जुले भाव जो हमारी पहली मुलाकात में थे।
विचित्र है न जीवन। कुछ लोग, कुछ घटनाएँ अपनी बुनावट में इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतना दुःख या इतना वैचित्र्य समेटे होते हैं कि उन्हें किस्से कहानी में बांध पाना कभी सहज नहीं होता। उनकी स्मृतियाँ तक इतनी दुखदायी होती हैं कि कभी छूने भर से समूचा मन पीड़ामय लौटना जैसे जानते बूझते नँगे पाँव कांटों की रहगुज़र से गुजरना और तार तार हो जाना या फिर जीते जागते किसी अगनपाखी में बदल जाना जिसके इर्द गिर्द अग्नि केवल अग्नि की लपटें है, कहीं कोई शीतलता का कतरा नहीं।
वह उसी अबोध रूप में मेरी स्मृतियों में बहुत धीमे से प्रविष्ट होती है और मैं जैसे किसी अजाब की गिरफ़्त में उन्ही पलों को जीते हुए हर बार गहन पीड़ा से गुजरती हूँ। हर बार उतनी ही विवश, उतनी ही क्रोधित और उतनी ही निराश जितनी हर बार महसूस करती रही। उन स्मृतियों से मुक्त होना सहज तो नहीं या फिर मैं खुद नहीं चाहती कि कभी मुक्त हो पाऊँ।
“मीना” यही नाम बताया था उसने अपना। ‘वे लोग’ उसे कभी मिन्नी पुकारतीं, कभी मीनू और कभी-कभी क्रोध से मीना भी जो उसका असली नाम था। कैसा असली नाम जबकि जो भविष्य उसके लिये तय कर दिया गया था वहाँ किसी साधारण दुनियावी नाम की गुंजाइश ही कहाँ थी। विशेषकर उस नाम की जो उसे जन्म देने वाले माँ-बाप ने दिया। ये नाम भी उसे उसके माँ बाप ने नहीं ‘उन्होंने’ दिया जिनकी झोली में उसे डाल दिया गया परमपिता के नाम पर। अब कोई पुकारू नाम तो चाहिये ही था तो फ़िलहाल के लिए ये पुकारू नाम था मीना!
यूँ किसी भी व्यक्ति का नाम उसका जीवनभर का साथी होता है। ये और बात है कि बहुत-सी स्त्रियाँ अपने नाम और पहचान को कहाँ जीवन भर सहेजकर रख पाती हैं। एक दिन नाम और पहचान खो जाती है। तब किसी और के नाम और पहचान को अपने वजूद पर चस्पा कर स्वयं नामहीन हो जाना स्त्रियों की नियति रही है। जैसा मेरी देवकी बुआ का नाम बदल दिया गया विवाह के बाद क्योंकि फूफाजी का नाम गोविन्द था! अब गोविन्द की पत्नी देवकी कैसे हो सकती हैं तो बुआ को नया नाम मिला – रुक्मणी! जीवनपर्यन्त वे इसी नाम से जानी गयीं! भले ही मायके में सब देवकी ही बुलाते रहे पर एक वक़्त के बाद स्त्री का स्थायी घर और स्थायी नाम दोनों ससुराल से जुड़े होते हैं!
पर मीनू तो अभी महज आठ साल की नन्ही बालिका थी पर इतनी कुशाग्र बुद्धि कि जानने लगी थी कि उसका नाम और पहचान दोनों अस्थायी भ्रम हैं। इन पर उसका कोई हक़ है ही नहीं। तभी तो किसी नाम की भी पुकार पर दौड़ पड़ती थी। कभी कभी तो तो पुकार नामहीन भी होती वह पुकार के आभास भर पर चौकन्नी हो उठती।
इस उम्र के बच्चे कितना खिजाते हैं अपनी माँ को पर उसके अवचेतन में तो बसी थी ये अतिरिक्त सतर्कता कि उसके कान सदा किसी पुकार की प्रतीक्षा में खड़े रहते और इन्द्रियाँ सहजता से परे खास मुद्रा में तनी रहतीं जैसे चौबीस घण्टा किसी कैमरे की जद में हो। मुँह में जिव्हा के अग्रभाग पर टिके रहे ये शब्द, “हाँजीsssss” जिन्हें उच्चारते हुए वह हड़बड़ाकर आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ती थी। इतना हड़बड़ाकर कि जैसे एक क्षण की भी देरी पर उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। जाने किससे डरती थी वह। ऐसा लगता था उसका ये डर कोई धूसर आवरण है जिसने उसके पूरे वजूद को अपने कब्ज़े में ले लिया है।
मेरी और उसकी दोस्ती की कहानी भी विचित्र थी। किसी आकस्मिकता की कोख से निकला था हमारे घर में उसका ये प्रवास। वरना उसे तो ‘गृहस्थों’ से सदा दूर रखा जाता। उसका लालन पोषण जिस कड़े अनुशासन में हो रहा था उसमें ‘वे लोग’ शायद किसी तरह की कोई बाधा नहीं चाहती थीं! या शायद जिस तरह के विशिष्ट जीवन को मीना के भविष्य हेतु चुन लिया गया उसमें यही उसके हित में था कि वह जीवन में हर साधारणत्व से अछूती और अनजान रहे!
पर जीवन की अनिश्चित्तता सब सोचे समझे गए को पीछे छोड़ देती है तो एक आपातकालीन स्थिति में वे लोग यानी ‘माताजी’, जो मेरी माँ की आध्यात्मिक गुरु थी और ‘आनंदी बाईजी’ जो उनकी असिस्टेंट टाइप सेविका थीं, दोनों को पंजाब के एक शहर में स्थित अपने एक अन्य आश्रम में अनिश्चितकालीन प्रवास के लिए जाना पड़ा। आनंदी, संभवतः उनका गृहस्थ दिनों का नाम रहा होगा वैसे तो उनकी सन्यास के बाद नाम था संपूर्णानन्द जैसे माता जी का नाम था अभेदानन्द जी महाराज।
यक़ीनन उस यात्रा में हमारा घर एक सुरक्षित पड़ाव रहा होगा जहाँ मीना यानी मीनू को कुछ दिन के लिये रख दिया गया। माँ की सादगीभरी और अनुशासित जीवनशैली के प्रति उनका यह भरोसा माँ के लिये कितनी बड़ी उपलब्धि रहा होगा, उस समय मुझे इसका कतई भान नहीं था। होता भी कैसे, नौ बरस की मैं, तो केवल इसी बात से खुश थी कि मीनू हमारे घर में हमारे साथ रहेगी, मेरी दोस्त बनकर।
पंजाबी परिवेश के हिसाब से माताजी को सदा बहुवचन में सम्बोधित किया जाता था। तो जब माताजी पंजाब वाले आश्रम में गए तो मीना गुमसुम उन्हें जाते हुए देख रही थी। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने बाईजी के सिर पर लपेटे हुए ओढनीनुमा गेरुए वस्त्र का छोर पकड़ लिया। पर माताजी की सख़्त फटकारनुमा पुकार पर वह सहमकर एक कदम पीछे हट गई। उसकी आँखें डबडबा जरूर गईं पर उनमें छलछला आये अश्रुओं ने आँखों के हर अनुशासन का सम्मान किया।
पहले दिन वह सहमी और उदास दिखाई दी। नितांत अपरिचित माहौल में स्वाभाविक तरह से चुप और डरी हुई। शाम होते ही जब मैंने उसे रस्सी कूदने के खेल में शामिल किया तो इनकार करते हुए वह किनारे बैठकर हम बच्चों को देखती रही। मेरे लिये इस उम्र के किसी बच्चे का इस कदर गम्भीर या निस्पृह होना कल्पनातीत अनुभव था पर था तो यह सच ही न।
शुरुआत में मीनू के ऊपर चढ़ा काठ का वह खोल इतना सख़्त था और इतना दुरूह था उस खोल के भीतर से उसे निकाल पाना कि मेरा कोमल और मासूम मन थककर मुरझा जाता। जैसे कोई घोंघा चुपके से अपने खोल से बाहर झाँक रहा हो और अपरिचित आहट से डरकर फिर उसी में घुसकर छिप जाये। पर मेरा जिद्दी स्वभाव, मेरी अंतहीन जिज्ञासा और जुझारू प्रवृति ने घुटने टेकने से साफ़ इनकार कर दिया। संभवतः इसमें मेरी उम्र का भी कुछ हाथ अवश्य रहा होगा। समझ आने पर मैं शायद ही इस कदर आग्रही हो पाती।
इस खोल के चटकने में वक़्त लगा पर बहुत अधिक नहीं। खोल चटका और इसमें हमारे छत के कोने में बिताए समय का बहुत महती योगदान है जहाँ दुनिया भर की औपचारिकताओं से परे हम केवल हम होते, दो अबोध बच्चियाँ नन्दू और मीनू।
किसी बंद कमलिनी की तरह था उसका व्यक्तित्व जिसके खुलने की अधीर प्रतीक्षा मेरे वश के बाहर थी। उस कमउम्र में भी ये समझ आने लगा था कि परिस्थितियों ने उस कमलिनी को खिलने से पहले ही मुरझाने पर मजबूर कर दिया है। महज कुछ समय पहले तक वह मेरे लिये एक अजूबा थी।
मतलब आठ साल की बच्ची, हर उस चीज़ के लिये जिज्ञासा से भरी जो उसका स्वतः ही ध्यान खींच लेती पर ये जिज्ञासा भी कैसी कि उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें मासूम सी कामना की चमक से भर उठती, ये पुलक उसके गालों पर झिलमिलाती पर उसके होंठ जैसे कोई ताला लगा हो।
उसके हावभाव इतने संयत थे कि जैसे उस अबोध उम्र में केवल वैराग्य ही उसका जल और वायु हो लेकिन अकेले में इधर उधर फिरती उसकी चोर निगाहें मुझसे छिपी नहीं थी। शायद वह मुझसे भी छिपाने का यत्न करती अगर जिस दिन वह आयी, वह न घटा होता! मैं किसी काम से अपने कमरे में गई तो उसे मेरे खिलौना किचन सेट को उलटते-पलटते देखा! मुझे देखते ही वह तुरन्त वहाँ से निगल भागी! उसी दिन सबकी नज़र बचाकर मेरी विदेश से आई विलायती गुड़िया को उसने धीमे से उठा लिया! उसे पलकें झपकते देख बार-बार मीनू को गुड़िया को सोते-जगाते न देख लेती तो मैं यकीन न करती कि उसने ऐसा किया। मैं ध्यान से उसे देख रही थी, उसके काठ जैसे भावहीन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, शायद उसका डर उसके आनंद से कहीं अधिक सशक्त था पर उसकी आँखों ने उसे धोखा दे दिया! उन मुस्कुराती आँखों से झलककर एक कतरा ख़ुशी उसके गालों से होकर उसके होंठों के किनारे पर झलकी और विलुप्त हो गई!
मैंने चैन की साँस ली उसके इस सहज और प्राकृतिक व्यवहार पर। ठीक उसी समय उसकी नजर मुझ पर पड़ी! अपने पकड़े जाने और मुझे खुश देखकर वह तनिक झेंप गई और गुड़िया पलंग पर फेंक दी पर फिर जब मैंने स्वयं गुड़िया उसके हाथ में पकड़ाई तो वह उसे ऐसे छोड़कर कमरे से भागी जैसे कोई जलता अंगारा उसकी हथेली पर रख दिया हो। मन बुझ गया मेरा। क्या गलती हुई मुझसे। मैं तो केवल उस क्षणिक मुस्कान की आकांक्षा से भरी थी जो पिछले कुछ क्षणों में कौंध की तरह झलकी थी।
दुनिया भर के कामों में व्यस्त माँ के पास मेरी अंतहीन जिज्ञासाओं का कोई समाधान मुश्किल से ही मिलता पर इस बार उन्होंने मुझे निराश न किया।
“मीना का भविष्य इन खिलौनों में नहीं है। यह सब उसके लिये वर्जित नहीं हैं पर उसे किसी भी मोह के जागने से बचना होगा क्योंकि उसे तो साध्वी बनना है।” उस रात माँ ने बताया और मुझे चादर ओढ़ाकर एक उबासी ले वे नींद के झूले में झूलने लगी ।
“साध्वी…? वो कैसे माँ….” मेरी जिज्ञासा ने फिर सिर उठाया।
“उहूँ… अरे मतलब बाईजी। चलो अब सो जाओ। तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होते। सुबह जल्दी उठना है मुझे।” कुनमुनाते हुए माँ ने मुझे एक चिरपरिचित रिदम में थपथपाते हुए पूरी तरह नींद के आगोश में चली गयीं।
कितना काम करती हैं माँ। बेचारी थक गई होंगी। मेरे पास भी सो जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था पर देर रात तक मैं जब भी आँखे बंद करती, मेरे सामने बाईजी बनी नन्ही सी मीनू की छवि आ जाती। भगवा कुरता, नीचे भगवा तहमदनुमा धोती, मुंडे हुए सिर पर ढका एक भगवा वस्त्र जिस पर सिर और कंधों पर कसकर लपेटा हुआ था फिर एक भगवा वस्त्र। साध्वी मीनू और उसके भावहीन काठ से सपाट चेहरे पर वही गोल-गोल आँखें पर इस बार मुझे उनमें छटपटाकर दम तोड़ता कामना का पंछी दिखाई पड़ता और मैं घबराकर आँख खोल देती।
तो मैं बता रही थी कि माताजी और बाईजी के चले जाने के बाद मीनू से मेरी दोस्ती का रास्ता कुछ सहज हो गया! हम साथ खेलते, साथ खाते पीते, दिनभर मस्ती करते! दो तीन दिन बाद उसके भीतर की छोटी बच्ची खुलने लगी! अब मेरे सामने थी धीमी आवाज़ में, पंजाबी लहजे में बतियाती मीनू जिसके पास कहने को बहुत कुछ था पर झिझक की ओट में मेरे प्रोत्साहन की प्रतीक्षा करता था और तनिक से प्रयास से छलक पड़ता। छत पर बने उस कोने में बने सीमेंटनुमा पटरे पर बैठे वह एक सर्वथा नई और अनजान दुनिया का द्वार मेरे लिये खोल देती थी।
हम दोनों मिलकर लँगड़ी टांग खेलते, रस्सा कूदते, कुलिया में भीगा बाजरा खाते, गुड़ियों के किचन सेट से खाना बनाते, उसके लिये भी ये सब कुछ कौतूहल से भरा हुआ था। उसे जो सिखाया गया था वह भी मुझसे बाँटती। मेरे अनुरोध पर वह मुझे धीमी पर बड़ी मीठी आवाज़ में भजन सुनाती,
“एक हार बना सोहणा, सतगुरां दे गल विच पांवा,
बुहा खोल पुजारिया वे, सतगुरां दे दर्शन पांवा।”
मुझे अक्सर ख़याल आता, उसका भी एक परिवार रहा होगा पर उसे उनकी कोई याद नहीं थी। पूछने पर उसकी गोल गोल आँखें विचित्र से खालीपन से भर जाती थीं। माँ ने बताया था मुझे कि जब मीनू गोद में ही थी कई बेटियों वाले उसके परिवार ने उसे गुरु महाराज की सेवा में देकर जाने पुण्य कमाया था या उससे छुटकारा पा लिया था ताकि एक और बेटी को पालने से बोझ से मुक्ति मिले।
“ये लोग बेटी ही सेवा में क्यों देते हैं माँ? क्या बेटे की तरह बेटी भी बड़ी होकर उनका सहारा नहीं बन सकती?”
“गरीब थे बहुत नन्दू। खाने को अनाज नहीं था। पाँचवी बेटी को कैसे पालते?”
रात में दूध का गिलास थमाते हुए जब माँ ने ये कहा तो नन्दू पहले ही सोने जा चुकी थी।
मैं पूछना चाहती थी कि पाल नहीं सकते तो भगवान से बेटी ली ही क्यों पर पूछ न सकी। मेरा सवाल दूध में उठे बुलबुलों सा सतह पर बैठ गया पर मेरा मन दूध का शांत गिलास नहीं था। उसमें तो किसी शांत झील के भीतर होने वाली हलचल सिर उठाये हुए थी।
बच्चे भगवान के घर से आते हैं जिन्हें माँ बाप झोली पसारकर माँग लेते हैं, ये माँ ने ही तो बताया था मेरे जन्मदिन पर मेरे ही सवालों के जवाब में। तब भगवान से लिये गए बच्चे को भगवान को ही सौंप देने का ये कौतुक मेरी समझ से परे था।
“तुम्हे अपने घरवालों की याद नहीं? माँ की कोई याद?” सुबह जब मैं और मीनू हमारी पसंदीदा जगह पर बैठे गिट्टे खेल रहे थे तो पूछा था मैंने।
“गुरु महाराज ही मेरी माँ, वही पिता और वो ही मेरा परिवार हैं।” उसने लगभग रटे रटाये अंदाज़ में कहा।।
“कभी तुम्हारा मन नहीं होता अपने परिवार से मिलने का…. अपनी माँ से मिलने का…” मैंने ढीठ होकर फिर पूछा। मेरी कमउम्र समझदानी में पता नहीं क्यों ये बात नहीं घुस रही थी कि उस अबोध की भावनाओं की शांत झील में मैं अपनी जिज्ञासा के कंकड़ फेंककर उसके सर्वनाश पर तुली हुई हूँ।
“नहीं आती याद… नहीं मिलना किसी से जिन्होंने मुझे….मेरा कोई नहीं।” कहते हुए उसका चिरपरिचित निस्पृह भाव कहीं खो गया था। उसकी गोल आँखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। चेहरा खिंच गया था और जबड़ा भींचकर उसने कहा और गिट्टे फेंककर वहाँ से उठकर भाग गई।
उस दिन बहुत अनमनी और उदास लग रही थी वह। बिल्कुल पहले दिन जैसी मीनू। मुझे पश्चाताप हो रहा था। अपनी गलती का पूरी तरह अहसास तो नहीं था मुझे पर इतना समझ गई थी कि कुछ अनुचित अवश्य कहा या किया मैंने। इसी कारण पूरा दिन बीत गया पर मैं माँ से भी ज़िक्र नहीं कर पायी।
उसका दिल दुखाने वाली अपनी गलती का प्रायश्चित यही समझ आया मुझे कि उसका मन बहलाने का अधिक प्रयत्न करने लगी थी मैं। उसे अपने खिलौने खेलने को देती। अपने चॉकलेट, टॉफी आदि से उससे बाँटती। यहाँ तक दोपहर में जब माँ झपकी लेतीं तो उनसे छुपाकर पहनने के लिये अपने नए नए कपड़े उसे देती। कभी वह मेरी जन्मदिन वाली ड्रेस पहनकर शरमाती तो कभी मेरा जयपुर से आया लहंगा चुन्नी पहनकर इठलाती। पँखों वाला हेयर बैंड, रंग-बिरंगी खिलौना घड़ी, नाचने वाली गुड़िया, ताली बजाता बन्दर, बंजारन से आटा देकर लिये गए मिट्टी के छोटे छोटे बरतन और भी बहुत कुछ। उसकी बेजान आँखों में कई सपने थिरकने लगे थे। उसके चेहरे पर मुस्कान का भब स्थायीपन की ओर बढ़ रहा था। विडंबना ये थी कि हर वो बात जो मुझे खुशी से भर रही थी शनै-शनै उसे उस जीवन के नज़दीक ले जा रही थी जो उसके लिये वर्जित तय किया गया था।
इधर अनजाने ही मैं एक पाप की भागीदार बन रही थी। पाप इस मायने में नहीं कि ये सब मीनू के लिये वर्जित होना चाहिये था, मेरा अपराध ये था कि जिस कंडीशनिंग में उसे दुधमुंही वय से डाला गया था, मेरे इन प्रयासों से उसमें सेंध लग गई थी। उससे भी बड़ा अपराध ये था कि जीवन के प्रति ललक से भरे जो सपने मैं उसे सौंप रही थी निकट भविष्य में वह सब उससे छिनकर उसे वापिस उसी त्याग, वैराग्य और संन्यास की दुनिया में लौट जाना था। और यही हुआ भी, एक दिन वह अपनी सारी यादों को मुझे सौंपकर आश्रम लौट भी गई। पर जाते जाते चुपके से मुठ्ठी भर सपने अपनी आँखों मे छुपाकर ले गई जो दुनिया भर की आँखों में किरकिरी की तरह रड़कने वाले थे।
मेरे उस अपराध का भान मुझे आने वाले जीवन में एक बार नहीं बार-बार होता रहा जब मैं सुनती कि मीनू उद्दंड हो गई है या मीनू आश्रम के जीवन से सामंजस्य नहीं बिताना चाहती। कभी वह चोरी से मिठाइयाँ खाती पकड़ी जाती तो कभी गृहस्थों सत्संगियों के लिये रखे अचार चुराती मिलती। जाने कैसा संताप था उसके अंतर्मन में कि वह कुछ न कुछ ऐसा करती मिलती जो उससे कतई अपेक्षित नहीं था। सादा खाना, सादा रहन सहन और कठोर जीवन शैली में मुरझा गया था उसका बचपन। वह विद्रोह करती तो सज़ा मिलती थी। सुना मैंने कि उसकी ‘उद्दंडता’ इतनी बढ़ती गई कि वह उनके लिये सिरदर्द बन गई।
मुझे मीनू का ही सुनाया वह भजन याद आने लगा,
‘भजन करो रुत भजन की आयी रे
भजन बिना मीरां बावरिया….”
उस भजन में जहर का प्याला पीती, साँप-पिटारे को खोलती, काँटों की सेज पर सोती मीरां की छवियाँ मेरे अबोध मन में कौंधती रही। ख़याल आता रहा कि जैसे मीनू भी आज के समय की मीरां है जो किसी गिरधर गोपाल के लिये नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के लिये संघर्षरत है।
फिर एक दिन जब माताजी और बाईजी फिर हमारे घर आये तो मेरी निगाहें उसे ढूंढ रही थीं पर मीनू उनके साथ नहीं थी।
“बदतमीज़ हो गई है। आश्रम के नियम तोड़ती है। उसकी यही सज़ा है कि कभी आश्रम से बाहर नहीं जाएगी।” माँ के पीछे छुपे हुए मैंने आनंदी बाईजी को कहते सुना था और काँप गई थी इस ख़याल से कि अब मीनू से कभी मिलना न होगा। अजीबोगरीब ख़्याल आते रहे मुझे। क्या माँ को नहीं कहना चाहिये कि मीनू अभी बच्ची है या कि ऐसे नियम उसके लिये बहुत कठोर हैं। उसे दण्ड देना अनुचित है। पर न माँ ने कुछ कहा न मैं कह पायी। सुनती थी मैं, सजाओं का कोई असर नहीं होता मीनू पर। बहुत ढीठ हो गई है। कभी कभी मुझे महसूस होता था आनंदी बाईजी उसे पसंद नहीं करतीं यही कारण है उसकी हर गलती राई से पहाड़ बन जाती है। बहुत समझ नहीं थी मुझे पर मैं बहुत परेशान थी ये सब जानकर। हर समय आत्मा, परमात्मा की बात करने वाले लोग जीवित व्यक्ति की आत्मा को कैसे कष्ट पहुँचा सकते हैं, मैं यह भी पूछना चाहती थी। पंचतत्वों से बना शरीर इतना निस्पृह, कामनाहीन, अनुशासित और सधाव से भरा क्यों होना चाहिये? क्या उन तत्वों को कभी कोई बांध पाया है?
इसके कुछ साल बाद हम लोग सपरिवार आश्रम गये थे। मैं उत्साह से भरी थी कि मीनू से मिलूँगी। अलवर के बस अड्डे के करीब था ये आश्रम। हम जब पहुँचे तो दिन छिप चुका था। हमारा सामान एक बड़े से आंगन में रखा था। उसे उठाने के लिये कुछ कमउम्र बाईजी लोग आयी थीं। मैंने अंधेरे में भी उस छाया को पहचान लिया था। बिल्कुल बाईजी की तरह के कपड़े थे उसने। कुरता, धोती, ढका सिर और उस पर ओढ़ कर रखा शालनुमा एक कपड़ा पर उसके वस्त्र भगवा नहीं श्वेत थे। संन्यास लेने से पहले तक यही श्वेत पोशाक पहनी जाती है माँ ने बताया था मुझे। ये भी कि कुछ समय बाद उसे भगवा वस्त्र पहनने होंगे सदा के लिये। अब वह मीनू या मिन्नी नहीं ‘मीना बाईजी’ के नाम से पुकारी जाती थी। अपने अवांछित जीवन की ओर बढ़े इस कदम ने उसके जीवन को बहुत बदल दिया था। वह पहले की तरह रंगीन कपड़े नहीं पहनती थी। आम लड़कियों की तरह सलवार सूट या फ्रॉक भी नहीं। मेरा मन उसे ऐसे देख धक से रह गया। जबकि मैं, केवल मैं जानती थी उसे रंगों से कितना प्रेम था। चटख गुलाबी रंग तो कितना पसंद था मीनू को।
“मीनूsssss”
मेरी धीमी पुकार अनसुनी नहीं रही। उस श्वेतवसनी साये ने मुड़कर देखा। होले से कौंधी थी उसकी हल्की सी मुस्कान जिसे मेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख पाया था क्योंकि वह थी भी केवल मेरे लिये। वह सिर झुकाकर हाथ में अटैची लिये अपनी लकड़ी की खड़ाऊं खड़काती हुई वहाँ से चली गई।
दो दिन हम वहाँ रहे पर एक बार भी मीनू से एकांत में बात करने का मौका नहीं मिल पाया। वह ऊपर के तल में बने रसोईघर या काम की अलग अलग जगहों पर व्यस्त रही। शायद उसे इज़ाज़त नहीं थी हम लोगों के पास आने की। जाने क्यों उसे देखकर लगा उम्र की कई सीढ़ियाँ उलांघकर वह बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। मुझसे भी खासी बड़ी। दो दिनों में उसे एकाध बार इधर से उधर जाते देखा पर न तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी न ही फिर वह मुस्कान मुझे देखने को मिली जो आश्रम में उस पहली मुलाकात में मिली थी। उससे मिलकर बतियाने की साध लिये मैं लौट आयी।
इस बीच मालूम चला कुछ समय के लिये मीनू को पंजाब के आश्रम भेज दिया गया था। फिर वापस अलवर लौटने पर उससे फिर कोई बड़ी गलती हुई और उसे उसके घर भेज दिया गया। क्या रही होगी वह ग़लती मैं कभी नहीं जान पायी। एक सामान्य लड़की की तरह जीने की इच्छा से बड़ी उनके लिये और क्या गलती हो सकती थी जो उसे साध्वी बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अपने मन को न मार पाने की सज़ा, इच्छाओं और कामनाओं के जीवित रहने की सज़ा, अपने मासूम बचपन के बार-बार सिर उठाने की सज़ा और सर्वथा वर्जित दुनिया के सपने देखने की सज़ा उसे मिल गई थी। यही तो थे इसके अक्षम्य अपराध जिसे उनकी दुनिया ने स्वीकार न किया। मेरा मन हाहाकार कर उठा। माला फेरने वाले वे कैसे संन्यासी हाथ थे जो एक अबोध का मन न सहेज सके।
और कैसा परिवार था जहाँ उसे भेज दिया गया था वे लोग जो पहले ही उससे गुरु के नाम पर सौंपकर पीछा छुड़ा चुके थे उसे कैसे स्वीकार करते। फिर जिस जीवन में उसकी परवरिश हुई थी वह कैसे उन भाई बहनों के साथ रह पाती होगी, क्या उन्होंने उसे स्वीकार किया होगा जो कभी उनका हिस्सा रही ही नहीं, सोचकर मेरी रूह बेचैन हो जाती थी। इसके बाद मैं पढ़ाई के लिये होस्टल में चली गई। जीवन अपनी गति से चलता रहा। कभी कभार उसकी याद आती पर मेरी अपनी व्यस्तताएँ मुझे घेरे रहीं।
कुछ वर्षों बाद जब लौटी तो एक दिन बातों ही बातों में जो सत्य मेरे समक्ष अनावृत हुआ उसने मेरा सुख चैन दोनों छीन लिये। पता चला भाई बहनों और परिवार ने उसे मन से कभी स्वीकार नहीं किया। उनके लिये अनामंत्रित बोझ बनी, उनके दुर्व्यवहार को झेलती, अपने ‘अपराधों’ के लिये प्रताड़ना और लानतें सहती मीनू कुपोषण और अवसाद में घिरकर बहुत बीमार हो गई थी। बीमारी की उस अवस्था में उसके घर वाले उसे आश्रम छोड़ गए क्योंकि उनके हिसाब से मीनू उनकी नहीं आश्रम की जिम्मेदारी थी।
दुर्भाग्य जो जन्म से उसे घेरे था, उसने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। उन्ही दिनों एक और दुर्घटना घटी जिसने मीनू के दुखभरे जीवन पर गहरा असर डाला। माताजी बहुत बीमार होकर निर्वाण को प्राप्त हो गए और आनंदी बाईजी ने उनके उत्तराधिकारी के तौर पर गद्दी पर बैठते ही मीनू को फिर वापिस उसके घर भिजवा दिया। उन्होंने आश्रम में कई बदलाव किये। उन्हें सिर झुकाए रहने वाले फरमाबरदार सेवक चाहिये थे। मीनू की उन्मुक्तता नहीं उन्हें तो अपनी धर्मसत्ता की स्थापना के लिये कटी जबानें और अनुशासित कंधे चाहिये थे। उन्हें बिलकुल पसंद नहीं थी। उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिये वे हरगिज़ तैयार नहीं थीं। नतीज़ा ये हुआ कि कौए और मोर की कहानी की तरह मीनू कहीं की नहीं रही। वह न तो साध्वी हो सकी और न ही गृहस्थ जीवन में कहीं कोई स्थान उसके लिये बन सका।
अपमान की अग्नि में सतत झुलसते टूटे मन, रोगी तन ने इस बार-बार के देशनिकाले के आगे घुटने टेक दिए और एक दिन उसका मन पखेरू सारे पिंजरे तोड़कर उड़ गया। धर्म के चंगुल, अज्ञानता और गरीबी के दुर्भाग्यपूर्ण गठजोड़ ने उस मासूम की बलि ले ली जो अभी जीने का सही अर्थ भी न सीखी थी। पंचतत्व, पंचतत्वों में मिल गये। जिस तथाकथित ईश्वर के नाम पर उससे जीने का हक़ छीन कर बार बार अपराधी ठहराया गया वह सबसे परे उसी में विलीन हो गई। जिस मोक्ष के नाम पर धर्म का सारा कारोबार चलता है उसे मीनू ने पाया या नहीं ये तो नहीं मालूम पर अपने जीवन को अपनी तरह जीने की उसकी ललक को कम से कम जीते जी कोई नहीं छीन पाया, यही उसका मोक्ष था और यदि सद्गति भी। उसकी मृत्यु ने उसे तो सदा के लिये इस अनचाहे जीवन से मुक्ति दे दी पर मैं यही छूट गई सदा के लिये, उसकी स्मृतियों और अपने अपराधबोध के साथ जिनसे मैं कभी मुक्त न हो सकी।
कभी लगता है उसे वे वर्जित सपने दिखाने का मुझे कोई हक़ नहीं था। तब तो मैं अबोध थी पर होश सँभाल लिया तब भी अपनी उस प्यारी मासूम दोस्त के लिये मैं कुछ न कर सकी सिवाय उसे धीरे धीरे मौत के मुँह में जाते देखने के। पर क्या मीनू की अपराधी केवल मैं ही थी? मीनू दुनिया से बेशक़ चली गई पर मेरी स्मृतियों में उसका बसेरा आज भी है जहाँ मेरे स्नेह, मेरी विवशता, मेरी हताशा और ग्लानि के साथ वह आज भी जीवंत है, अपनी उन्मुक्त मुस्कान और भयातुर आँखों के विरोधाभासी अस्तित्व के साथ। उसकी अंधेरे में कौंधती वह मुस्कान मेरा दामन खींचती है और उसकी फुसफुसाहट भरी आवाज़ आज भी जब तब मुझे नींद से जगाकर कहती है,
“नहीं मिलना किसी से मुझे…मेरा कोई नहीं।”
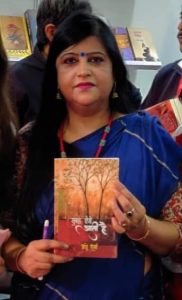
—अंजू शर्मा,कथाकार
नयी दिल्ली
पौराणिक मिथकों को आधुनिक संदर्भ में लिखना साहस का काम है- गिरीश पंकज