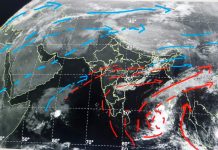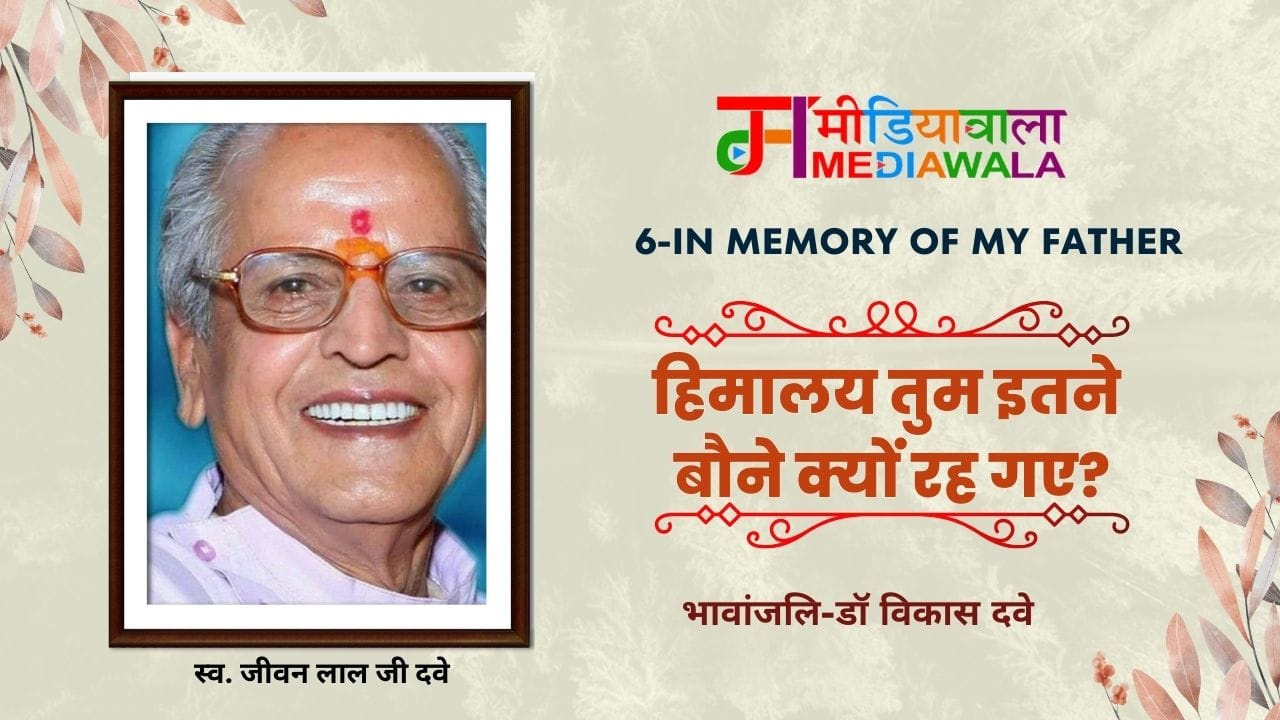
In Memory of My Father / मेरी स्मृतियों में मेरे पिता
पिता को लेकर mediawala.in में शुरू की हैं शृंखला- मेरे मन /मेरी स्मृतियों में मेरे पिता। इसकी {6} छठवीं क़िस्त में डॉ विकास दवे अपने पिता के व्यक्तित्व की विराटता पर एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग याद करते हुए उन्हें सेल्यूट कर रहे हैं –
युग-युग अजेय, निर्बंध, मुक्त,
युग-युग गर्वोन्नत, नित महान्,
निस्सीम व्योम में तान रहा
युग से किस महिमा का वितान?
कैसी अखंड यह चिर-समाधि?
यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान?
तू महाशून्य में खोज रहा
किस जटिल समस्या का निदान?
उलझन का कैसा विषम जाल?
–रामधारी सिंह दिनकर
6.In Memory of My Father : हिमालय तुम इतने बौने क्यों रह गए??
डॉ विकास दवे
मेरे आज के इस शीर्षक को पढ़कर शायद पाठकों का चौंकना स्वाभाविक है। जिस विराट हिमालय को हम ऊंचाइयों की पराकाष्ठा के लिए संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रतीक के रूप में रखते हैं उसे बौना कहकर में आखिरकार विराट किसे बताना चाहता हूँ? दरअसल हिमालय बौना तब हो जाता है जब हम इसे प्रतीक के रूप में अपने पिता के समक्ष खड़ा कर देते हैं। सचमुच पिता से विराट दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज बहुत लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए अपने जीवन के एक अत्यंत दुखद अध्याय का एक करुण पृष्ठ आप सबके समक्ष बाँचना चाहता हूँ।

यह वह समय था जब मैं लगभग दसवीं ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था। मुझसे बड़े भैया विश्लेष दवे जो दिखने में अत्यंत हष्टपुष्ट और सौंदर्य के सभी मानकों पर खरे उतरने वाले एक तेजस्वी युवा की तरह थे, पर अनायास प्रकृति का कहर टूट पड़ा। बड़े भैया के रुग्णता के दौर में जांच से यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें बड़ी आंत में एक ट्यूमर हुआ है और वह ट्यूमर कैंसर का रूप धारण कर चुका है। पूरा परिवार कभी भी किसी भी प्रकार के व्यसन को पैर से भी छूना पसंद नहीं करता था। खान-पान में अत्यधिक सात्विकता के बाद भी अचानक इतनी बड़ी बीमारी का घर के एक युवा सदस्य की देह में प्रवेश कर जाना हम सबके लिए एक बड़े झटके से कम नहीं था। जैसा आमतौर पर होता है पूरा परिवार भैया के उपचार में जुट गया। उपचार तो क्या होना था एक प्रकार से ईश्वर और सृष्टि के समक्ष आत्मसमर्पण किए हुए एक माता-पिता और लगभग समझ के विकसित होने की प्रतीक्षा करता एक छोटा भाई क्रमशः निकट आती मृत्यु को भैया से परे धकेलने का असफल प्रयास कर रहे थे।
उस पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से इस समय चर्चा नहीं कर रहा किंतु केवल इतना भर बताता चलूं कि शायद दुनिया की ऐसी कोई पैथी और चिकित्सा पद्धति की दवाई नहीं होगी जिसे प्रयोग के तौर पर उपचार के लिए उपयोग में ना लाया गया हो। इसमें अत्यधिक अर्थसाध्य और श्रमसाध्य उपचार भी सम्मिलित थे तो कठिनतम प्रक्रिया के उपचार भी। किसीने कहा विदेश से कुछ अत्यंत महंगे इंजेक्शन लाकर यदि लगाये जाएं तो वह कैंसर की कोशिकाओं को समाप्त करने में समर्थ सिद्ध हो सकते हैं। बड़ी भारी कीमत चुका कर वे इंजेक्शन भी उस युग में फ्लाइट से बुलवाए गए और लगवाए गए जिस युग में हम रोडवेज की बसों में बैठने से पहले भी चार बार खिड़की पर किराया पूछा करते थे।
चिकित्सा पद्धतियों का जहाँ तक प्रश्न है एलोपैथी से लेकर आयुर्वेदिक तक, होम्योपैथी से लेकर यूनानी तक सभी चिकित्सा पद्धतियों को आजमाया गया। इतना ही नहीं तो अपरंपरागत चिकित्सा पद्धतियों यथा रंग चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा,गेहूं घांस पद्धति और ऐसी अनेक पद्धतियां जिनके बारे में उससे पहले तक हम लोगों ने कभी सुना तक नहीं था, उन सबको भी उपयोग करने के लिए पिताजी सिद्ध थे। एक ही लक्ष्य था अपने युवा पुत्र को मृत्यु के मुख से बचा ले जाना। बाल्यकाल में पौराणिक आख्यानों में जब मैं सती सावित्री के प्रसंग पढ़ा करता था तो मुझे आश्चर्य लगता था कि क्या कोई मानवी यमराज से संघर्ष करके अपने परिजन को बचाने का प्रयास भी कर सकती है? किंतु पिताजी को जिस जिजीविषा से भैया के उपचार में लगे देखा था वे अनुभव मेरे जीवन के अत्यंत मार्मिक, संघर्षशील और धैर्यवान बनाने वाले अनुभव थे। इन्हीं पद्धतियों को तलाशते- तलाशते अचानक उस समय के प्रख्यात गांधीवादी चिंतक और वैद्य श्री कुंदनमल जी जैन ने पिताजी को विसर्जन आश्रम के श्रद्धेय मानव मुनि जी से मिलवाया। मानव मुनि जी ने पिताजी से कहा कि गांधी जी और मोरारजी देसाई ने अत्यंत शोध पूर्वक संपूर्ण विश्व को प्रदत्त स्वमूत्र चिकित्सा पर पर्याप्त काम किया है और विश्व के हजारों लाखों प्रसंगों में इस स्वमूत्र चिकित्सा के चमत्कारी परिणाम प्राप्त हुए हैं। नासमझ लोगों ने भले इस पद्धति का मजाक बनाया हो घृणा की हो पर यह अत्यंत चमत्कारी परिणाम देने वाली पद्धति है।

देखते ही देखते मुंबई से पुस्तक बुलवाई गई। ‘स्वमूत्र चिकित्सा के अनुभूत प्रयोग’ पुस्तक लगभग 300 – 400 पृष्ठ की थी किंतु उसमें प्रकाशित हर तथ्य, प्रमाण और प्रसंग को पढ़ते समय एक आस मन में जागती थी कि दुनिया की गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज इस चिकित्सा पद्धति से संभव है। किंतु पद्धति का तरीका सुनकर ही पूरा परिवार सकते में था। विशेष कर भैया ने तो जब यह सुना कि इसमें अपने ही विसर्जित मूत्र को पीना पड़ता है, तो यह घोषणा कर दी कि भले ही मृत्यु का वरण कर लूंगा किंतु इस चिकित्सा पद्धति को प्रयोग में नहीं लाऊंगा।
पिताजी बिना विचलित हुए भैया को रुग्ण शैय्या पर लगातार उस पुस्तक के अनुभूत प्रसंग पढ़-पढ़ कर सुनाते रहे किंतु भैया को टस से मस नहीं होना था वह नहीं हुए। पिताजी ने अंतिम रूप से प्रयास करते हुए भैया से केवल इतना आग्रह किया कि तुम रोज जब भी लघुशंका के लिए जाते हो तो एक स्वच्छ गिलास में स्वमूत्र लाकर टेबल पर रख लिया करो। मैं तुम्हें पीने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं करूंगा। पिता के अत्यधिक आग्रह को स्वीकार कर भैया ने यह उपक्रम प्रारंभ कर दिया। वह दृश्य ही हम सब लोगों को द्रवित करता था। भैया प्रतिदिन ग्लास लाकर ढंककर रख देते थे और कई बार पिताजी के मौन चेहरे के आग्रह को देखकर उस ग्लास को चेहरे के निकट लाते और सूंघकर वापस रख देते। पीने की हिम्मत होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था सूंघने मात्र से उनको जो उबकाई आती तो घंटों थमने का नाम न लेती थी।
यह क्रम एक लंबे समय तक चलता रहा। यह एक पिता का संघर्ष था पुत्र के जीवन की वापसी के लिए। उन मार्मिक मनोभावों को किसी भी साहित्य की विधा में शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना कठिन ही नहीं असंभव लगता है।
एक दिन अनायास एक अद्भुत घटनाक्रम हुआ।भैया ग्लास लेकर गए हुए थे कि पिताजी ने माताजी और मेरी उपस्थिति में चुपचाप चौके में आकर एक अनोखी घोषणा की। उन्होंने कहा -“आज से विश्लेष इस चिकित्सा को करना प्रारंभ कर देगा।” हम सबकी आंखों में आंसू थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि जिस कार्य के लिए भैया बिल्कुल मना कर चुके हैं उसे वे कैसे करेंगे और पिताजी आखिर करना क्या चाहते हैं? माँ ने इतना ही कहा -” मेरी।करबद्ध प्रार्थना है उसके साथ कोई जबरदस्ती मत करना।”


मौन रहकर माताजी और मैं पिताजी के प्रयासों का समर्थन भी कर रहे थे पर हमसे ही कोई कहता तो शायद हम भी यह उपचार नहीं कर पाते। भैया ने प्रतिदिन की तरह स्वयं के मूत्र से भरा वह ग्लास लाकर टेबल पर ढंककर रख दिया। पिताजी ने कक्ष में प्रवेश किया। हम भी पीछे-पीछे उनके उस अंतिम प्रयास को देखने के लिए साथ-साथ जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने भैया के उस ग्लास को हाथ में लेकर कहा -“यह अपने ही शरीर से उत्सर्जित एक ऐसी औषधि है जिसे पश्चिमी जगत में बिल्कुल हानिप्रद नहीं माना है और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट हैं। इससे अधिक घृणित तत्व दवाइयों में हम बिना जाने ग्रहण कर लेते हैं जबकि हमें पता ही नहीं होता कि उनके परिणाम सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। तुम अपने ही शरीर के मूत्र से इतनी घृणा कर रहे हो जबकि यह तुम्हें जीवन दे सकता है। यदि ईश्वर करें जो बीमारी तुमको मिली है वह बीमारी मुझे हो और तुम स्वस्थ हो तो मुझे यह उपचार करने में बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे भी एक औषधि की तरह ही स्वीकार करूंगा। इतना ही नहीं मुझे तो अपने जीवन के इस अमूल्य हिस्से अर्थात तुम भी उतने ही निरापद लगते हो और तुम्हारे शरीर से उत्सर्जित यह औषधि भी। मुझे अपना मूत्र तो ठीक है तुम्हारे मूत्र से भी औषधि के रूप में कोई परहेज नहीं।”
ऐसा कहते कहते एक झटके से पिताजी ने वह ग्लास उठाया और गट-गट करके पूरा पी लिया। भैया अत्यंत अशक्त थे इसलिए झटके से उठना चाहते थे पर वे उठकर खड़े होते तब तक यह प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। अब बारी परिवार के चारों लोगों के रुदन की थी। हम चारों उस दिन गले मिलकर खूब रोए। किंतु आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि उस दिन के बाद भैया ने बिना किसी ना नुकुर के इस कठिन तपस्या को भी प्रारंभ कर दिया। हमने उसके बाद उनको कभी उबकाई खाते तो नहीं देखा पर आंखें झर- झर बहते रोज देखते थे।
हालांकि ईश्वर को जो स्वीकार था वही हुआ। लगभग कुछ माह बाद भैया की उस भयावह कर्क रोग से मृत्यु हुई। पूरे परिवार ने उस दुःख को एक लंबे मानसिक संघर्ष के पश्चात ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार किया किंतु उस दिन का वह घटनाक्रम हम लोगों के लिए एक ऐसी घटना थी जो हम कभी किसी के समक्ष बता नहीं पाए। ‘मीडिया वाला’ पोर्टल ने अभी जब 2 अक्टूबर से पिता की विराटता को प्रदर्शित करने वाले संस्मरण और रेखाचित्रों के प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया और साहित्य संपादक स्वाति तिवारी जी ने जब मुझे यह आग्रह किया कि इसमें मैं भी एक प्रसंग की आहुति दूं तो हृदय के किसी कोने में आंसुओं से सराबोर यह प्रसंग अनायास पृष्ठों पर उतर आया है। यह प्रसंग कलम में स्याही नहीं अश्रुजल भरकर लिखना पड़ा है। सचमुच उस दिन मैंने जिन पिताजी को यह सब करते देखा था तब से मुझे पिता शब्द के समक्ष हिमालय भी बौना लगने लगा है। माँ निर्विवादित रूप से सृष्टि की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है और हैं भी किंतु पिता के मौन तप और अत्यंत संघर्षशील मनोवृत्ति को शायद ही दुनिया के कोई मानक आकलित कर सकें। पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं 29 अप्रैल 2017 को वे नहीं रहे पर हिमालय से ऊँची उनकी वह जिजीविषा आज भी कही है यही कहीं मैं महसूस करता हूँ .इसलिए दोनों दिवंगत आत्माओं को प्रणाम करता हूँ और अंत इसी बात से कर रहा हूँ कि- “हे हिमालय!!! तुम इतने बौने क्यों रह गए? काश ईश्वर और सृष्टि तुम्हें भी पिता की ऊंचाई प्रदान कर पाते।”

डॉ विकास दवे
निदेशक,
साहित्य अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल
In Memory of My Father: नारियल जैसे बाबूजी