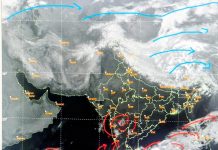इंदौर की त्रासदी: रैंकिंग में चमक, नलों में ज़हर!
सबसे गंभीर सवाल जवाबदेही का!
श्याम यादव की त्वरित टिप्पणी
शहर स्वच्छता में अव्वल है, इसलिए पानी गंदा कैसे हो सकता है? अगर गंदा है भी तो तकनीकी रूप से। तकनीकी शब्द सुनते ही आम आदमी समझ जाता है कि अब दोष किसी व्यक्ति या संस्था का नहीं, बल्कि किसी अमूर्त प्रक्रिया का है। और प्रक्रिया की सबसे सुरक्षित विशेषता यह होती है कि उसे कभी निलंबित नहीं किया जाता, न उस पर कोई कार्रवाई होती है।
इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें महज एक स्थानीय हादसा नहीं हैं। यह उस शहरी विकास मॉडल की परिणति हैं, जिसमें उपलब्धियों का मूल्यांकन रैंकिंग, पुरस्कार और प्रचार अभियानों से तय होता है, न कि नागरिक के रोजमर्रा के अनुभव से। शहर कितना “स्मार्ट” है, यह कैमरे और आंकड़े बताते हैं; लेकिन नल खोलते ही जो डर और अनिश्चितता बहती है, उसका कोई सूचकांक नहीं बनता।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया का ढांचा अब लगभग स्वचालित हो चुका है। घटना होते ही कहा जाता है—नमूने लिए गए हैं, जांच जारी है, रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी। यह प्रक्रिया आश्वासन ज्यादा देती है, समाधान कम। सवाल यह नहीं रह जाता कि पानी कैसे दूषित हुआ, बल्कि यह बन जाता है कि मामला कितने दिन में शांत हो जाएगा। रिपोर्ट के आने तक समय खरीदा जाता है, और समय के साथ सवालों की धार कुंद पड़ जाती है।
पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा अगर नागरिक के लिए जोखिम बन जाए, तो यह किसी एक विभाग की विफलता नहीं, पूरे शासन तंत्र की प्राथमिकताओं पर सवाल है। पानी कोई वैकल्पिक सेवा नहीं है कि खराब होने पर उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। यह जीवन से जुड़ा विषय है। इसके बावजूद व्यवस्था का भरोसा टैंकरों, अस्थायी इंतजामों और सलाहों पर टिका दिखता है—पानी उबालकर पीजिए, बाहर से मंगाइए, सावधानी बरतिए। मानो सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सावधान रहना नागरिक की जिम्मेदारी हो।
स्वच्छता रैंकिंग ने नगर निकायों को एक खास किस्म की मानसिकता में ढाल दिया है। सड़कें चमकें, दीवारें रंगी हों, कचरे के ढेर कैमरे से दूर रहें—यही स्वच्छता का दृश्य रूप है। लेकिन भूमिगत पाइपलाइन, सीवेज नेटवर्क और जलशोधन संयंत्रों की स्थिति पर शायद ही उतना ध्यान दिया जाता है। ये वे हिस्से हैं जो दिखते नहीं, तस्वीरों में नहीं आते और पुरस्कार समारोह में तालियां नहीं दिलाते। नतीजा यह कि शहर ऊपर से साफ दिखता है और नीचे से धीरे-धीरे सड़ता रहता है।
इंदौर की घटना यह भी बताती है कि शहरी बुनियादी ढांचे में रखरखाव को लगातार टालने की कीमत आखिरकार नागरिक चुकाता है। पाइपलाइनें पुरानी हैं, कई जगह पीने के पानी और सीवेज की लाइनें साथ-साथ चल रही हैं, निगरानी व्यवस्था ढीली है। ये सब बातें नई नहीं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक नुकसान आंकड़ों में तब्दील नहीं होता, तब तक इसे “तकनीकी समस्या” मानकर टाल दिया जाता है।
सबसे गंभीर सवाल जवाबदेही का है। मौतें होती हैं, बयान आते हैं, कभी-कभार मुआवज़े की घोषणा होती है और फिर व्यवस्था आगे बढ़ जाती है। शायद ही कभी यह तय होता है कि लापरवाही कहां हुई और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। जब दोष तय नहीं होता, तो सुधार भी अधूरा रह जाता है। जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्टें आती हैं और फिर अगली घटना तक सब कुछ जस का तस बना रहता है।
यह भी गौर करने वाली बात है कि ऐसी घटनाओं के बाद सार्वजनिक विमर्श अक्सर भावनात्मक राहत तक सीमित रह जाता है। कुछ दिन गुस्सा, कुछ दिन दुख, फिर सामान्य स्थिति। लेकिन नीतिगत स्तर पर यह स्वीकार करने का साहस कम ही दिखता है कि मौजूदा प्राथमिकताएं गलत दिशा में हैं। विकास अगर नागरिक की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा, तो उसकी चमक पर सवाल उठना ही चाहिए।
इंदौर की यह त्रासदी सिर्फ इस शहर की कहानी नहीं है। देश के कई शहर इसी रास्ते पर हैं—रैंकिंग में ऊपर, लेकिन बुनियादी सेवाओं में असुरक्षित। स्वच्छता, स्मार्ट सिटी और अमृत जैसी योजनाओं का असली मूल्यांकन तब होगा, जब नागरिक नल का पानी बिना डर के पी सके।
आखिरकार, स्वच्छता का अर्थ सिर्फ साफ दिखाई देना नहीं है। इसका मतलब है सुरक्षित पानी, भरोसेमंद व्यवस्था और स्पष्ट जवाबदेही। अगर नलों से ज़हर बहने के बाद भी हम इसे तकनीकी शब्दों में ढकते रहेंगे, तो सवाल सिर्फ पानी का नहीं रहेगा। सवाल यह होगा कि क्या इस विकास मॉडल में नागरिक की जान की कोई वास्तविक कीमत है भी या नहीं।