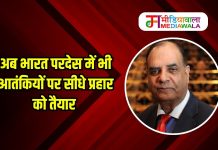कानून और न्याय: मानवाधिकार आयोग को सजा देने का अधिकार भी मिले!
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण के मामले में देश की सर्वोच्च संस्था है। ऐसी ही संस्थाएं राज्यों में भी हैं। यह एक कानूनी संस्था है, जिसका गठन 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुसार हुआ। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयोग स्वयं अपनी पहल पर या पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। इस आयोग के कार्य-क्षेत्र में जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करना, न्यायिक व पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जाॅंच-पड़ताल करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और लोगों के गायब होने आदि मामलों की जाॅंच करना शामिल है। साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना या शोध को बढ़ावा देना और लोगों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना भी इस आयोग के कार्यों में शामिल है। आयोग मानवाधिकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और रिपोर्ट्स का अध्ययन कर उनके प्रभावी अनुपालन की सिफारिश भी करता है। इनके अलावा भी मानव अधिकारों से संबंधित एवं इन क्षेत्रों में आयोग के कई कार्य हैं।
आयोग की तुलना बिना नाखूनों और बिना दाॅंतों वाले शेर से की जाती है, जो कहने को तो शेर होता है, लेकिन उसके पास वास्तविक शक्तियाॅं नहीं होती हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में यह आयोग न तो किसी को दंडित कर सकता है और न ही किसी को मुआवजा दे सकता है। यह केवल अपनी जांच के आधार पर सरकार या न्यायालय से मुकदमे की सुनवाई की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारें आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। आयोग उन शिकायतों की जाॅंच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई गई हों। साथ ही, आयोग के पास सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों की जाॅंच का अधिकार भी नहीं है। बड़ी संख्या में पदों का खाली पड़े रहना, संसाधनों व धन की कमी, आयोगों के अंदर सदस्यों का नौकरशाही ढर्रे पर काम करना, पुलिस व अन्य जाॅंच एजेंसियों का पूरी तरह से सहयोग न करना आदि आयोग की राह में रूकावट का बड़ा कारण हैं।

भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के आंकड़े चिंताजनक है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आयोग ने बीते पाॅंच सालों में क्रमश : अर्थात 2017 में 82,006, साल 2018 में 85,950, साल 2019 में 76,585 और साल 2020 में 75,064, साल 2021 में 1,06,022 शिकायतें दर्ज की हैं। वहीं वर्ष 2022-23 में मई माह तक 16,504 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से 17,043 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। आयोग के समक्ष आज भी हजारों मामले विचाराधीन हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक मजबूत और शक्तिशाली संस्था बनाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों का विवरण इस तरह से दिया जाना चाहिए कि विभिन्न आयोगों के बीच आंकड़ों का ताल-मेल ठीक रहे। इसके अलावा शिकायतों के जल्द से जल्द समाधान के लिए आयोग की शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही आयोग में संसाधनों व धन की कमी को दूर किया जाना भी आवश्यक है। आयोग में एक कार्यकारी समूह का गठन भी किया जाना चाहिए, जो अविलंब कार्रवाई कर सके। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारों, पुलिस, न्यायपालिका व अन्य जांच एजेंसियों द्वारा आयोग के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए ताकि आयोग अपना कार्य बिना किसी बाधा के कर सके।
लेकिन, अधिकार संपन्न होने के बाद भी केवल मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों का निवारण करने से ही मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं हो सकेगा। लोगों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना होगा। हमें समझना होगा कि जो आजादी, समानता, प्रतिष्ठा, शांति आप अपने लिए चाहते हैं, वह दूसरों को भी दें। तभी हम अपने मानवाधिकारों का समुचित विकास और संरक्षण कर पाएंगे।
भारत के संविधान में संबंधित प्रावधानों के साथ मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों में, कानून के समक्ष समानता, समान सुरक्षा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के उपाय, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण, संपत्ति का अधिकार, अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और किसी भी धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करना, बोलने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सेवा के अवसर में समानता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। राजनीतिक और नागरिक अधिकारों तथा सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 1966 पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में निहित कई नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी भारत के संविधान के भाग तीन में निहित हैं। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर और इनकी पुष्टि की है।
संविधान के अधिनियम के समय इस घोषणा में जितने अधिकार उपलब्ध थे, उतने मौलिक अधिकार उपलब्ध नहीं थे। न्यायिक व्याख्याओं ने भारतीय संविधान में उपलब्ध मौलिक अधिकारों के दायरे को निरंतर विस्तृत किया है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया कि भूमि का कानून भारतीय संविधान में विशेष रूप से प्रदान किए गए अन्य प्राकृतिक या सामान्य कानून अधिकारों को मान्यता नहीं देता है। बाद में, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने अनुच्छेद 21 में अभिव्यक्ति एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता विस्तृत विश्लेषण किया तथा इसमें कई तरह के अधिकार शामिल माने। ये अधिकार मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिये होते हैं। इनमें से कुछ को अलग मौलिक अधिकारों की स्थिति में माना गया और अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। अनुच्छेद 19 के तहत कोई भी व्यक्ति विदेश जाने के अपने अधिकार से तब तक वंचित नहीं रह सकता है, जब तक कि राज्य द्वारा उसे वंचित करने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला कोई कानून न हो।
मेनका गांधी प्रकरण के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों मामलों में मौलिक अधिकार की न्यायिक व्याख्याएं कर इसे व्यापक बनाया तथा कई अधिकार एवं छूट नागरिकों को प्रदान की। इनमें मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, शीघ्र परीक्षण का अधिकार, निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आजीविका का अधिकार, भोजन का अधिकार, चिकित्सा देखभाल का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे अनेक अधिकार सम्मिलित हुए।