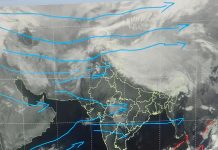‘गांधी के बिना मेरा काम नहीं चल सकता’
सत्यानन्द निरुपम की गिनती एक कुशल पुस्तक संपादक के रूप में होती है। प्रतिष्ठित प्रकाशनों से जुड़े रहे निरुपम फिलहाल राजकमल प्रकाशन समूह के संपादकीय निदेशक का दायित्व निभा रहे हैं। वे चंडीगढ़ आए तो पुस्तक संपादन के विभिन्न पहलुओं और प्रकाशन से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत हुई। अपनी संपादन यात्रा के बारे में बताते हुए सत्यानंद निरुपम ने बताया कि यह उन दिनों शुरू हुई जब जेएनयू से पीएचडी की तैयारी कर रहा था।
उस दौरान जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रहा था। उसी समय यात्रा बुक्स से प्रस्ताव आया कि क्या मेरी संपादन में दिलचस्पी है। मैंने कहा कि कभी सोचा नहीं, लेकिन मैनेजर पांडेय की दो किताबों के संपादन से जुड़ा रहा हूं, एक रिसर्च एसोसिएट की तरह। लेकिन प्रोफेशन के रूप में नहीं सोचा। यह बातचीत निर्णायक थी। तब तो मैंने जॉइन नहीं किया, क्योंकि उन दिनों एनसीईआरटी में जूनियर रिसर्च फेलो भी था। तभी पेंगुइन के एडिटर-इन-चीफ रवि सिंह की तरफ से मुलाकात का प्रस्ताव आया, यह बातचीत लम्बी चली। आकर्षक मानदेय के साथ संपादक का नया दायित्व मिला। एक ही महीने में दो जगह से नौकरियों प्रस्ताव, यह मेरे आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ।
अब जहां तक परिवार में पढ़ाई-लिखाई के माहौल की बात है तो मेरे बाबा परमात्मा सिंह को पढ़ने का खासा शौक था। तमाम साहित्यिक पत्रिकाओं के अंक आते थे। पड़ोस के दादाजी की भी समृद्ध लाइब्रेरी थी। जिसमें पहली बार किसी लेखक का पत्र भी देखने का सुयोग बना, वियोगी हरि जी का पत्र। उनकी एक अलमारी थी, जिसमें हर धारा का लेखन मौजूद था, अकादमिक भी और पापुलर साहित्य भी। पड़ोस में एक और दादाजी थे जो कबीर साहित्य के मर्मज्ञ थे। पिताजी मेरे लिए सभी बाल पत्रिकाएँ ले आते। उन्हें भी पढ़ने का शौक था। पढ़ने की लालसा ऐसी थी कि एक समय जब पढ़ने को घर और पास-पड़ोस में कुछ भी नया शेष नहीं बचा था तो भीष्म साहनी का उपन्यास ‘तमस’ ही पढ़ गया और उसके बाद हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनामदास का पोथा। यह आठवीं क्लास की बात है। आठवीं-नौवीं में एक हस्तलिखित वार्षिक पत्रिका निकाली -तरंगिणी। होली से पहले बसंत की बयार। निराला जी की रचनाओं का अक्स था। इससे पहले हस्तलिखित पत्रिका देखी-पढ़ी नहीं थी।
नागार्जुन बोलते, मैं लिखता जाता
कालांतर में दसवीं में पढ़ता था तो नागार्जुन को चिट्ठी लिखी। नागार्जुन जी ने बुलाया भी। नागार्जुन ने ही बाद में मैनेजर पांडेय से मिलने को कहा। उनसे ग्रेजुएशन के दौरान मिलने जाता था, कभी वे बुला भी लेते थे। पूछते थे, क्या पढ़ा, ये भी पढ़ो। एक बार पूछा, क्या तुम मेरे लेख का डिक्टेशन लेना चाहोगे। उनका लिखने का मन नहीं था। उन्हीं दिनों उनके बेटे की हत्या हुई थी, व्यथित थे। मैंने हामी भर दी। इसके बाद वे बोलते थे, मैं लिखता जाता। उनके इस भरोसे से उनकी लाइब्रेरी तक पहुंच बनी। उनकी ‘आलोचना की सामाजिकता’ किताब बनाने में भी भूमिका निभायी। यह एक तरह से संपादन की ट्रेनिंग थी। दरअसल, मेरा करियर संयोग में शुरू हुआ और बना, लेकिन मेहनत बहुत की।
वैचारिक आग्रह में बंध नहीं सकता
दरअसल, मुझे कभी किसी विचारधारा से बंधना अच्छा नहीं लगा। मुझे किसी तरह की बंदिश कभी पसंद नहीं। स्कूल से लेकर कॉलेज व विश्वविद्यालय तक वाम व दक्षिणपंथी रुझान के लोग मिले, साहित्य दिया और जुड़ने का आग्रह किया। मैंने कहा, जो अच्छा लगता है वो करूंगा। गांधी के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। किसी तरह की धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय कट्टरता के साथ जा नहीं सकता। किसी वैचारिक आग्रह में बंध नहीं सकता। मनुष्यता का पक्षधर हूँ। जहां तक अखबार व किताब के संपादन में अंतर की बात है तो विजुअलाइजेशन दोनों में महत्वपूर्ण है। किताब में देखना होता कि इसकी सेल्फ लाइफ क्या है। अखबार में कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज न छूटे जो कल का इतिहास हो। अखबार पत्रिका का उद्देश्य लोगों को सचेत करना होता है। वहीं किताब में वर्ल्ड-व्यू के सर्किल को बड़ा करके देखना होता है। वैश्विक स्तर पर किस तरह का नयापन उभर रहा है, प्रॉडक्शन व डिजाइन के स्तर पर जागरूकता भी। पुस्तक जितना समकालीन परिवेश के प्रति सजग होगी,उतनी ही समर्थवान होगी। वहीं पुस्तक में रचनात्मक संभावना की पहचान जरूरी होती है।
इस प्रक्रिया में नए पाठक पैदा
वहीं जहां तक स्वांत: सुखाय के लिए लिखने व धनबल के प्रभाव की बात है तो यह समय की दस्तक है। सोशल मीडिया के आने से बहुत डेमोक्रेटिक हुई है दुनिया पढ़ने-लिखने में । हां, उच्छृंखलता भी आई। पहले भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट लेखक रहे हैं। फिर डाक्टर व इंजीनियर भी आए। ऐसा नहीं है कि अभी सेल्फ पब्लिशिंग शुरू हुई है। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अच्छे लोग भी आये। श्रीलाल शुक्ल भी ब्यूरोक्रेसी से आये। राग दरबारी जैसी रचना दी। वैसे इस प्रक्रिया में नए पाठक पैदा भी हुए। नई कॉर्पोरेट कल्चर में भी साहित्य की नई धारा का उदय हुआ। हिंदी पट्टी के युवाओं ने शेष भारत के युवाओं के साथ उनके साहित्य के नायकों को पढ़ा-सुना और फिर अपने साहित्य की ओर लौटे। उनमें लेखक बनने की भूख पैदा हुई। लेकिन अच्छे लेखन को प्रदूषित नहीं किया जा सकता। कालांतर पाठक में अच्छे साहित्य की भूख जगाती है।
किताब के चयन के आधार का सवाल
हल्के-फुल्के साहित्य ने भी पाठक जोड़े हैं। उससे प्रकाशन उद्योग को भी संबल मिला। हरिशंकर परसाई जी की बात याद आती है कि जब तक हिंदी के पाठक किताब नहीं खरीदेंगे, तब तक लेखक दरिद्र ही बना रहेगा। अब जहां तक किताब के चयन के आधार का सवाल है तो पुस्तक की विशिष्टता प्रथम होती है। यह कि पाठक क्यों पसंद करेगा। उसका समाज व विचार पर क्या प्रभाव होगा। ये किताब छापना क्यों जरूरी है। नहीं तो क्या मनोरंजन करने लायक है!
फिर लेखक में अपनी बात कहने की क्षमता है। कथ्य या क्राफ्ट कैसा है। दिल व दिमाग पर असर डालती है। वैसे प्रकाशन को लेकर ऐसे तो कोई प्रत्यक्ष व्यावसायिक दबाव नहीं होते पर बहुत से लोगों का जीवन इससे जुड़ा होता है। लेकिन उसकी सीमा रेखा तय करनी होती है। कभी भावनात्मक दबाव का पक्ष भी होता है। किसी संस्थान को चलाने की अपनी दुश्वारियां। लेकिन, ये सब चीजें बहुलांश से आंकी जानी चाहिए। वैसे तो शत-प्रतिशत सोना भी गहने बनाने में सहायक नहीं होता। सृजन यात्रा के कई सहयात्री होते हैं वो ऋषि-ऋण भी चुकाना होता है।