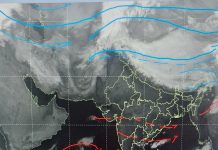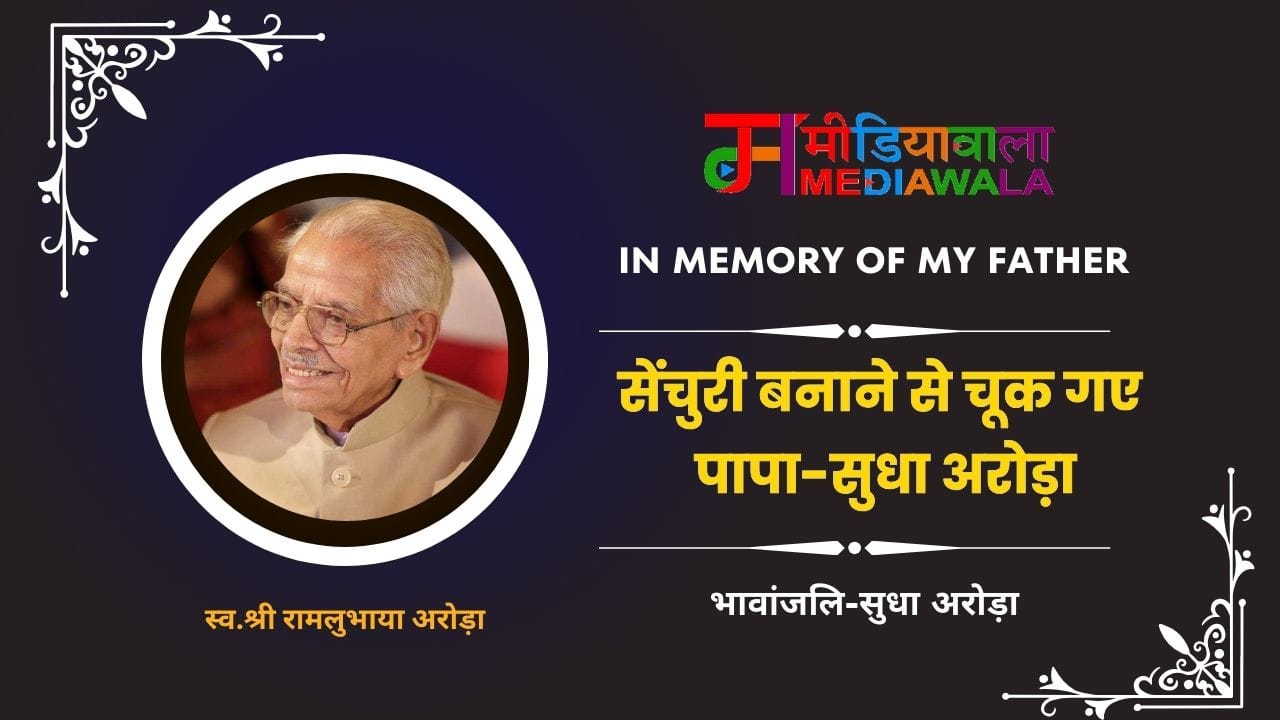
मेरे मन/मेरी स्मृतियों में मेरे पिता
पिता को लेकर mediawala.in में शुरू की हैं शृंखला-मेरे मन/मेरी स्मृतियों में मेरे पिता। इस श्रृंखला की 32 nd किस्त में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं देश की प्रख्यात साहित्यकार सुधा अरोड़ा जी को. सुधा जी वसुंधरा की संस्थापक निदेशक हैं, जो भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रचार के लिए समर्पित एक संगठन है। आपके पिताजी स्व. श्री रामलुभाया अरोड़ा जी कलकत्ता में अपना व्यवसाय करते थे. पश्चिमी पाकिस्तान के शहर लाहौर के मच्छीहट्टा बाज़ार के पुराने मोहल्ले ’’कूचा-काग़ज़ेयां‘‘ की एक संकरी गली मे जन्मे थे और वहां से विभाजन के चलते कलकत्ता आये थे. सुधाजी ने बहुत ही साहित्यिक शब्दावली में अपने पिता का स्मरण करते हुए लिखा है कि मैं हमेशा अपने भीतर अपने पिता को ज़िन्दा पाती हूं. घर में साहित्यकारों और कलाकारों (जिसमें राजेंद्र यादव, कृष्णाचार्य और कमलाकात द्विवेदी -जिन्हें हम बच्चे चाचाजी कहते थे-खास थे) का आना-जाना था। साहित्यिक रूचि उन्हें अपने पिता से ही मिली है .बहुत ही सुन्दर भावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अपने पिता को याद करते हुए अपनी भावांजलि दे रही हैं सुप्रसिद्ध कथाकार सुधा अरोड़ा…………..
जीवन में उतार-चढ़ाव आए हैं,
लेकिन आपकी ताकत और बुद्धि ने
हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है।
आपकी हंसी और खुशी ने
हमेशा मुझे एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद की।
आपकी कड़ी मेहनत और दयालुता ने
मुझे वह बनने के लिए प्रेरित किया जो मैं आज हूँ।-अज्ञात
32 .In Memory of My Father : सेंचुरी बनाने से चूक गए पापा-सुधा अरोड़ा

जब मैं छोटी थी, बड़े आश्चर्य की बात लगती थी मुझे कि एक मां अपने भीतर एक बच्चे को शक्ल, आकार देती है – अपने ही रक्त की आंच से उसे सींचती हुई, रूई के फाहे में लपेटी ’’हैण्डल विथ केयर‘‘ चीज़ की तरह – लगातार उसकी सुरक्षा करते हुए, लेकिन मां का सारा स्नेह और एहतियात सहेजे उसी के जिस्म का हिस्सा जब बाहर आता है तो कभी-कभी न सिर्फ़ सूरत-शक्ल में बल्कि स्वभाव, चाल-ढाल और आदतों में भी हूबहू अपने पिता की प्रतिलिपि होता है।
बीस साल पहले जब कोई मुझसे कहता कि तुम्हारी आदतें बिल्कुल अपने पापा पर हैं, मुझे बेहद खीझ होती थी क्योंकि मैं हमेशा अपनी मां की बेटी रही। मां – जिन्होंने एक औसत हिन्दुस्तानी औरत की तरह अपना घर बनाये और बचाये रखने में अपना अस्तित्व पूरी तरह होम कर दिया – सहज ही मेरे भीतर के ’’सॉफ्ट कॉर्नर’’ में दुबकी रहीं क्योंकि मुझमें वे अपने आप को पाती थीं। अपनी लिखी कविताएं तो उन्होंने संदूक में किताबों कापियों के बीच दबा कर रखीं और उन्हें बाहर की हवा नहीं लगने दी पर मेरी कलम के रचे शब्दों में अपना ही अक्स देखती रहीं।
अब मैं अपनी पचासवें वर्ष में कदम रखती अपनी बेटी को जब अपने पापा के नक्षे-क़दम पर चलता देखती हूं, तो अपने भीतर भी उतना ही अपने पिता को ज़िन्दा पाती हूं। मेरी शक्ल सूरत पर तो मेरी मां की छाप थीपर पिता के दाहिने गाल पर आंख के ठीक नीचे एक मस्सा था, जो हू-ब-हू उसी तरह मेरे बाएं गाल पर उतर आया। मां की शक्ल और मां को तहे दिल से अपने में समो लेने वाली मुझ पर, शायद यह उम्र और तजुर्बे का तकाज़ा है कि पापा की बहुत सी आदतों का, मुझमें ज्यों का त्यों उतर आना, अब मैं खुद महसूस कर सकती हूं । पापा की वे आदतें भी, जिन्हें मैंने कभी पसंद नहीं किया और जिन्हें अपने में लाने से मैं हमेशा बचती रही , अनचाहे-अनजाने किसी ढीठ की तरह मेरे भीतर अपनी जगह बनाती रहीं । उसमें से एक आदत यह भी कि हर ज़रूरी काम को आखि़री दिन तक टालते रहना लेकिन जब करने बैठे तो दिन-रात एक करके संतुष्टि के चरम (Perfection) तक पहुंचाकर ही दम लेना। पापा की तरह ही पर्फेक्शनिस्ट ! वह अधीरज, वह यातना और वह तृप्ति – कितनी कष्टकर होती थी उनके लिये। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मुझमें यह गुण उतरे। पर उतरा और पूरी शिद्दत के साथ। उसका एक प्रमाण यह संस्मरण – जो हमेशा की तरह इलेवेन्थ आवर में ही कागज पर उतर रहा है।

वह विभाजन पूर्व का लाहौर था। पश्चिमी पाकिस्तान के उस यादगार शहर लाहौर के मच्छीहट्टा बाज़ार के पुराने मोहल्ले ’’कूचा-काग़ज़ेयां‘‘ की एक संकरी गली मे 1 जून 1921 को पैदा हुए मेरे पापा अपने पांच भाइयों में से चौथे नम्बर पर थे, जिनके पैदा होने से पहले ही उनकी मां ने अपनी अगली संतान को अपने भाई, जो संतानहीन थे, को देने का वचन दे दिया था । इस तरह पैदा होने से पहले ही उनके मां-बाप बदल दिये गये थे। हमें तो यह किस्सा बहुत बड़े होने के बाद पता चला क्योंकि हमने उन्हें अपने मां-बाप के ’’अकेले और इकलौते बेटे’’ (लाड़ले और बिगड़ैल भी) के रूप में ही पाया । अकेली संतान – और वह भी बेटा – होने के जितने गुण-दोश हो सकते हैं, सब उनके साथ थे। अतिरिक्त संवेदनशील और उदार होने के साथ-साथ वे हद दर्जे के असहिष्णु और ज़िद्दी थे।

उस ज़माने में जब पापा के अपने चाचा – ताऊ बड़े-बड़े परिवारों के गर्वीले अभिभावक थे, पापा को अपना अकेला होना बहुत अखरता था। शायद यह” अकेले बेटे” के अकेलेपन का अहसास था कि पापा आधा दर्जन बच्चे चाहते थे। ईश्वर ने पांच के बाद जुड़वां बेटे देकर उन्हें एक बोनस दे दिया जिससे वे परम प्रसन्न थे . इतने बच्चों की ज़िम्मेदारी से अनजान पापा ने पांच बेटे और दो बेटियों का – जिसमें सबसे बड़ी बेटी मैं थी- रौनकी परिवार तो जुटा लिया पर इसका कितना बड़ा ख़ामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, यह शायद उन्होंने तब सोचा नहीं था। इस बड़े परिवार की इच्छा ने उनकी अपनी प्रतिभा, अपने शौक और अपने सपनों का गला घोंटकर रख दिया। अपने कॉलेज का सबसे ज़हीन छात्र घर गिरस्ती की चक्की में ऐसा पिसा कि अपनी सारी कलाकारी भूल गया।दसवीं पास करके पापा ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्टर और सिटी कॉलेज से बी. कॉम. किया और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में खूब ट्रॉफियां जीतीं। स्कॉटिश चर्च कॉलेज की फाइलन परीक्षा में पापा हिंदी में फर्स्ट आए। उसके बाद सिटी कॉलेज के कॉमर्स विभाग में पापा के हिन्दी शिक्षक प्रो. रामनारायण सिंह थे। हिन्दी में पापा क्लास में हमेशा पहले नंबर पर होते। बी. कॉम. करते हुए बंगाली रोमान्टिक भावुकता और कल्पनाशीलता उनपर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। देखने में लड़कियों सा नाजुक डील डौल, गोरा चिट्टा रंग और तीखे नैन नक्श – एकबार कॉलेज में क्लास में देर से पहुंचे तो शिक्षक ने दरवाजे पर पापा को देखकर कहा –“ द प्रिंसेज़ ऑफ द क्लास इज़ लेट टुडे । वहीं बैंकिग और करेंसी की कक्षाएं प्रो. आर.बी.बोस लेते थे और हर साल उनके विषय में प्रथम आने वाले छात्र को अपनी लिखी किताबें पुरस्कार में देते थे। पापा ने उस साल आर.बी.बोस पुरस्कार जीता।
अपनी पीढ़ी और अपने व्यवसायी तबके की पूरी बिरादरी में पापा पहले ग्रेजुएट थे, बी.कॉम. पास, वह भी अच्छे कॉलेज से डिस्टिंक्शन पाने वाले। पापा हर भाषा की वादविवाद प्रतियोगिता में जमकर हिस्सा लेते । बंगला, अंग्रेजी , उर्दू, हिन्दी सभी भाषाओं पर उनका एक सा अधिकार था । बंगला में उनका धाराप्रवाह भाषण सुनकर कोई कह नहीं सकता था कि वह गैर – बंगाली हैं । हिन्दी की सभी प्रमुख पत्रिकाएं हमारे घर आती थीं और पापा ने बरसों तक जिल्द मढ़े हुए विशाल भारत, विप्लव , हंस और चांद के अंक बरसों बरस सहेज कर रखे , जबतक महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की लायब्ररी के लिए कवि बोधिसत्व कोलकाता जाकर उनसे सारी किताबें और जिल्द बंधी अमूल्य पत्रिकाएं न ले गए।
दादा पापा के पीछे पड़े थे कि वे शादी कर लें। पापा की शर्त थी कि लड़की देखने में भी सुंदर हो और पढ़ी लिखी हो। पंजाबियों में सुंदर लड़कियों का मापदंड था बस गोरा चिट्टा रंग । सो ऐसी तो बहुतेरी थीं अपनी बिरादरी में, पर पढ़ी लिखी ? सो दादाजी गए लाहौर – अपने इकलौते बेटे के लिए लडकी पसंद करने। उन्होंने बुआ की सहपाठिनी एक ज़हीन लड़की वाहेगुरु कौर अरोड़ा को पसंद किया। लड़की पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, प्रभाकर पास कर साहित्य रत्न में एडमिशन ले चुकी थी। लड़की की भी यही जिद कि लड़का पढ़ा लिखा हो, दूकानदारी न करता हो, किसी अच्छी जगह नौकरी करता हो या टीचर हो। कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज का नाम सुनकर वे घबरा गईं कि लड़का कहीं अंग्रेजी दां न हो। उसे हिन्दी भाषा की जानकारी होनी चाहिये। प्रमाण के लिए पापा ने अपने होने वाले ससुर के नाम हिन्दी में पत्र लिखा। जब बेटी ने पत्र पढ़ा तो लजाकर अपने बाऊजी से कहा – इन्होंने तो मुझसे भी अच्छी हिन्दी लिखी है। सो दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्त मनवा ले गए । दादाजी के प्रस्ताव को नानाजी ने स्वीकार कर लिया और अपनी बिटिया के लिए हामी भर दी ।
उल्लास से लदे फंदे दादाजी लाहौर से जब कलकत्ता – चूहामल की बाड़ी – में लौटे तो बैंड बाजे के साथ । चूहामल की बाड़ी – एक चॉलनुमा मकान । बीच में खुला अहाता । वहां के सब रिहायशी अचंभे में कि यह बैंड बाजा क्यों बज रहा है। पता चला कि लाल सिंह जी अरोड़ा अपने इकलौते बेटे लुभाया का रिश्ता पक्का करके आए हैं। पापा जब अपनी लच्छेदार भाषा में बैंड बाजे वाले इस दृष्य का ब्यौरा देते, तो लगता था जैसे हम किसी कॉमेडी फिल्म का एक चुहल भरा दृष्य बड़े परदे पर देख रहे हैं। पापा बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। सभी अभिनेताओं दिलीप कुमार, मुकरी और देवानंद की खूब बढ़िया नकल उतारते।
सो पापा की मां-बाप द्वारा तय की गयी शादी (अरेन्जड मैरेज) भी कुछ-कुछ प्रेम-विवाह की तर्ज़ पर हुई। मां लाहौर में थीं और पापा कलकत्ता में। पापा शादी से पहले लाहौर गये तो अपनी होने वाली बीवी की एक झलक पाने के लिये घंटों थड़े (चबूतरे) पर बैठे रहते। मां की सहेलियां छेड़तीं – तेरा शौदाई मजनू थड़े पर बैठा है, ऐसे ही बैठा रहा तो दाढ़ी और बाल भी लंबे हो जाएंगे। फिर ऐसे बावरे से करना शादी!
कलकत्ता की हर पारिवारिक शादी में “ सेहरा” और “ सिखिया” (शिक्षा) मय सुर-ताल के पापा गाकर सुनाते । उर्दू की शायरी से लेकर के. एल. सहगल के गानों और रवीन्द्रनाथ टैगोर की रूमानी दुनिया में वह रहते थे । “ गीतांजलि “ का लयबद्ध अनुवाद उन्होंने शुरू किया था जो अद्भुत था । घर में साहित्यकारों और कलाकारों (जिसमें राजेंद्र यादव, कृष्णाचार्य और कमलाकात द्विवेदी – जिन्हें हम बच्चे चाचाजी कहते थे – खास थे) का आना-जाना था।

डॉ. प्रभुदयाल अग्निहोत्री जी – जो पापा के स्कूल के प्रिसिंपल थे और बाद में भोपाल वि.वि. के वाइस चांसलर बने – से पापा के पारिवारिक संबंध रहे । उनकी पत्नी शारदा को वे शारदा कह कर बुलाते क्योंकि वे पापा के लंगोटिया यार इटावा निवासी श्री श्रीराम द्विवेदी की छोटी बहन थीं ।
राजेंद्र यादव को जब पैर में गोली लगी तो श्रीराम द्विवेदी कमलाकांत द्विवेदी और पापा साथ ही थे । बताते हैं कि श्रीराम अपनी बन्दूक दिखा रहे थे कि अचानक गोली चल गई और साथ ही राजेंद्र यादव की चीख सुनाई दी – अरे मार डाला । सब घबरा गए । उन्हें टैक्सी में डालकर अस्पताल ले गए । वहां थोड़ी देर डॉक्टर का इंतजार करना पड़ा । जब डॉक्टर आया तो उसे बताया कि गलती से जांघ में गोली लग गई है । डॉक्टर ने पूछा – पर गोली लगी किसके पैर में है ? तब तक राजेंद्र जी का दर्द कम हो गया था और वे सामान्य दिखाई दे रहे थे। जब एक्सरे लिया गया तब तक टांग में लगी हुई गोली कूल्हे तक की यात्रा कर चुकी थी । ऑपरेशन करके गोली कूल्हे में से निकाली गई । एक पैर पहले से क्षतिग्रस्त था । दूसरे पैर में जांघ से लेकर पीठ तक दर्द होता था । उस पैर के भी जख्मी होने के बाद उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना नामुमकिन था सो एक ही रास्ता था कि उन्हें पापा अपनी साबुन फैक्टरी के कॉलेज स्ट्रीट स्थित ऑफिस में रख लें क्योंकि जहां राजेंद्र जी रहते थे, वह भी दूसरी मंजिल पर था और हम शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट के जिस रतन भवन में रहते थे, वह तीसरी मंजिल पर था और उसकी सीढ़ियां भी बहुत ऊंची थी ।
महीना भर राजेंद्र जी हमारी साबुन फैक्टरी के ऑफिस में साबुन की तीखी गंध के बीच रहे । पापा का कहना था कि बहुत जल्द उस गंध की आदत हो जाती है और बाद में वह गंध हवा का हिस्सा बन जाती है। दर्द, गंध, हर तरह की असुविधा में भी वह हंसी मज़ाक करते रहते थे और कभी उन्होंने फैक्टरी में रहने में होने वाली असुविधाओं की शिकायत नहीं की। राजेंद्र यादव की दर्द सहने की ताकत के कायल थे पापा और अक्सर उसका बयान करते । बीजी के हाथ का बना खाना ऑफिस में बाकायदा पहुंचाया जाता रहा जिसका जिक्र राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथात्मक किताब ‘मुड़ मुड़ के देखता हूं’ में किया है।

कई बार राजेंद्र यादव के साथ पापा रविवार को विक्टोरिया घूमने जाते । बताते हैं कि एक बार दोनों शायरी के मूड में थे । पापा ने ग़ालिब और मीर की कुछ शायरी सुनाई । राजेंद्र यादव ने भी कुछेक चुनिंदा शे’र सुनाए, पर जो एक शे’र पापा ने पहली बार राजेंद्र यादव के मुंह से सुना था, वह था –
खु़दी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले ,
खु़दा बंदे से खु़द पूछे – बता, तेरी रज़ा क्या है !!
पापा को यह लाइनें इतनी पसंद आईं कि उसे उन्होंने अपनी जिंदगी में उतार लिया और अपनी खुदी को बुलंद करने में जुट गए ।मां को हम बच्चे बीजी कहते थे – ठेठ लाहौरी थीं वे । लाहौरी होते हुए भी मां में बंगालीपन ज्यादा था और यह नफासत पापा की वजह से थी । बंगालियों के बीच पापा खालिस बंगाली लगते थे । “वेस्ट बेंगॉल स्मॉल स्केल सोप मेकर्स एसोसिएशन” के पंद्रह साल तक ज्वॉएंट सेक्रेटरी होने की वजह से पापा का बंगाली परिवारों में उठना बैठना ज्यादा था । टांघाइल और तांत की सूती और टसर सिल्क की कांथा की साड़ियां पहनी हुई हमारी मां यानी बीजी, नायलॉन और शेफॉन पहनने वाली पंजाबी औरतों के जमावड़े में, अपनी सुरूचिपूर्ण साड़ियों के कारण अलग से पहचानी जाती थीं । उनमें से कुछ साड़ियां आज भी सही सलामत हैं और मेरी बहुमूल्य थाती हैं।
वेस्ट बेंगॉल स्मॉल स्केल सोप मेकर्स एसोसिएशन में पापा का चुनाव डेव्हलपमेंट काउंसिल फॉर ऑएल्स, सोप्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्टीज में हुआ । लार्ज स्केल में टाटा और हिन्दुस्तान लीवर के दो सदस्य थे और स्मॉल स्केल में एक मद्रास से दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य और उत्तर भारत से पापा।
सन् 62 या 63 की बात है । एक बार मैं और मुझसे तीन साल छोटी बहन इन्दु आलमारी में कुछ खंगाल रहे थे कि हमें लाल कपड़े में बेहद एहतियात के साथ सहेजे हुए कुछ पुराने ख़त मिले । हमने उन्हें ऐसे चोरों की तरह खोला – जैसे कोई कारूं का खज़ाना हाथ लग गया हो, उसमें पापा और बीजी (मां को हम बीजी कहते थे ) के कुछ ख़त थे । शादी के बाद पहले बच्चे की (यानी मेरी ) डिलीवरी के लिये बीजी लाहौर गयी थीं – नाना-नानी के पास और पापा कलकत्ता में थे, उन्हीं दिनों ये ‘प्रेमपत्र’ लिखे गये थे। हमने बग़ैर उनकी इजाज़त के, घर के एक कोने में छुपकर, धड़कते दिल से कुछ ख़त पढ़े और उन्हें समेटकर वहीं रख दिया । उसके बाद जब भी पापा और बीजी नाइट शो में फिल्म देखने या किसी शादी – ब्याह में जाते, हम दोनों बहनें ख़त निकालकर पढ़ने लगते । ख़त क्या थे – बेहद रूमानी भाषा में शायरी या प्रेम – कवितायें थीं । उनकी भाषा इतनी बांधनेवाली थी कि हम बार-बार उन्हें पढ़ते । बीजी लाहौर की हिन्दी की प्रभाकर, साहित्यरत्न ( स्नातकोत्तर डिग्री ) थीं और पापा भी शेरो – शायरी में माहिर थे। हम दोनों बड़े खुश होते कि हमारे माता-पिता कितने “मेड फ़ॉर ईच अदर” हैं। अपने बीजी और पापा के उन प्रेमपत्रों की पोटली ने ही, हम दोनों बहनों में, हिन्दी भाषा और साहित्य के प्रति प्रेम तथा लेखन के प्रति रूझान के संस्कार डाले।
बीजी से शादी के बाद अपनी कलाकारनुमा सनक में पापा ने दादा के व्यवसाय के पचड़े में पड़ना मंजूर नहीं किया और उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में चालीस रुपये महीने की नौकरी कर ली। छह महीने के अंदर ही उनका ट्रांसफर न्यू मार्केट की शाखा में हो गया और तनखा पचहत्तर रुपए हो गई। नौकरी करते एक साल ही बीता कि उनके काम को देखते हुए उन्हें डबल इंक्रीमेंट मिला। पर नौकरी तो आखिर नौकरी है। दादा व्यवसायी व्यक्ति थे और चाहते थे कि उनका इकलौता होनहार बेटा व्यवसाय में उनका हाथ बंटाये । पापा की व्यवसाय में कोई रूचि नहीं थी । दादा और पापा में कलह-क्लेश शुरु हुए। पापा ने स्थितियों से समझौता किया और अपनी मनपंसद और सुविधाजनक नौकरी छोड़कर अपने आप को व्यवसाय में पूरी तरह झोंक दिया । आख़िर वही हुआ जिसका अंदेशा था – व्यवसायी माहौल में पापा का मन नहीं रमा । पापा अभी पूरी तरह व्यवसाय में पैर जमा भी नहीं पाये थे कि दादा ने हरिद्वार जाकर गेरुए वस्त्र धारण कर लिये ताकि बेटा पूरी तरह अपने व्यवसाय में ध्यान दे। दादा के संन्यास लेने पर घर में जैसे भूचाल आ गया। नतीजा यह हुआ कि पापा के कमज़ोर कंधों पर स्वाभाविक रूप से घर – परिवार के आर्थिक – सामाजिक उत्तरदायित्व का स्थानान्तरण हो गया। इस व्यवसाय ने पापा के कलाकार मन की आहुति ले ली। पत्नियों की रचनात्मकता का जैसे दक़ियानूसी पति क्षरण कर देते हैं, वैसे ही दादा ने घर गृहस्थी से संन्यास लेकर जबरन कलाकार बेटे की सारी रचनात्मकता को सोख लिया ।
दादा का अचानक गेरुए वस्त्र धारण कर हरिद्वार बस जाने का निर्णय ले लेना पूरे परिवार के लिये एक ज़बरदस्त झटका था – संभवतः परिवार के सबसे मजबूत स्तम्भ की मौत से भी बड़ा सदमा – लेकिन पापा ने इस मुश्किल दौर में पूरे घर को संभाला – दादी को, अपनी दोनों बहनो को और अपने सात बच्चों को भी । दादा, साल – दो साल में हरिद्वार से कलकत्ता हमारे पास मेहमानों की तरह आया करते और यह देखकर खुश होते कि शायरी और कविता, फिल्म और नाटक में लगे अपने “नालायक बेटे” को कोल्हू के बैल की तरह व्यवसाय के छकड़े में जोतने में वह कामयाब रहे हैं ।
लेकिन पापा व्यवसाय में कभी भी पूरी तरह रम नहीं पाए । अपना परिवार और बच्चे उन्हें बहुत प्रिय थे । वह एक पारिवारिक व्यक्ति थे । हफ्ते में छह दिन वह काम करते पर रविवार हम बच्चों के नाम होता । हर रविवार हम भाई – बहन कभी विक्टोरिया, कभी जेटी, कभी बोटैनिकल गार्डेन पिकनिक मनाने जाते । एकबार की घटना मुझे आज भी याद है । तब हम चार भाई – बहन ही थे । हर रविवार की तरह हम विक्टोरिया गये । शाम होते होते अचानक काले घने बादल घिर आए और अंधेरा छा गया । जब तक हम बाहर आते – धुआंधार तूफान के साथ गर्जन – तर्जन और कलकत्ता की बेमौसम बरसात शुरु हो गई । हम चारों बीजी से लिपटे एक पेड़ की छाया में खड़े हो गये और पापा बारिश में भीगते-भागते किसी प्रायवेट कार का बन्दोबस्त कर लाये और हम किसी तरह घर पहुंचे।
उस रात मुझे और मेरे भाई को बहुत तेज़ बुखार हो आया। बीजी के साथ-साथ पापा भी सारी रात जागते रहे। पापा का अपने सभी बच्चों के साथ अबाध-असीम प्यार था। कोई भी बच्चा बीमार होता, वह सारे ज़रूरी काम छोड़कर उसकी तीमारदारी में जुट जाते।
सात भाई – बहनों के उस विशाल परिवार में शायद ही कोई रात ऐसी होती होगी जब बीजी और पापा रातभर चैन की नींद सोते हों । बच्चों की उपेक्षा करना न उनके स्वभाव में था, न संस्कारों में । ऐसे कोई रईसजादे हम नहीं थे पर मुझे नहीं याद कि हमारी कोई भी मांग ऐसी रही हो जिसे तत्काल पूरा न किया गया हो। हम कुछ भी मांगते, वह चीज़ फ़ौरन हमें ला दी जाती। इस तरह के मध्यवर्गीय परिवारों में जितना प्यार किसी इकलौती सन्तान को मिलता होगा, हम सबको बराबर मिला। हम बच्चों को मां-बाप के प्यार की छत्रछाया और संभाल – सहेज ने इस कदर आच्छादित कर रखा था कि हम उस अतिरिक्त सुरक्षा के बंद माहौल में आज़ादी की खुली और ताज़ा हवा पाने के लिये सूराख ढूंढने लगे। नतीजा यह हुआ कि मुझ जैसी कुछ सन्तानें बग़ावत पर उतर आई और कुछ अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व बना पाने में असमर्थ अबतक उनपर ही निर्भर और आश्रित बनकर रह गयीं।
दादा, जब भी हरिद्वार से कलकत्ता आते, पापा और बीजी के सर पर सवार हो जाते कि सुधा के लिये इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उसकी शादी तय क्यों नहीं करते तुमलोग ? दादी भी अपने जीते-जी, अपनी बड़ी पोती की शादी तो देख लें । कलकत्ता के उस व्यवसायी, दकियानूस तबके के विशालकाय अरोड़ा परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी मैं । जैसें ही मैंने एम. ए. में दाख़िला लिया, घर में बवाल मच गया। दादा-दादी का कहना था कि सुधा ज्यादा पढ़ लिख गयी तो अपनी बिरादरी के व्यवसायी तबके में लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। “हमें लड़की से नौकरी तो करवानी नहीं है” यह उनका प्रिय वाक्य था पर पापा और बीजी शायद अपने अधूरे सपनों को मुझमें पूरा होता देखना चाहते थे । बीजी उन दिनों काफी बीमार रहती थीं, पर मुझे पढ़ते – लिखते देखतीं तो खुद ही चूल्हे चौके में बझी रहती, मुझे कभी रसोई के काम में मदद के लिये नहीं बुलातीं।
हमारी जान – पहचानवाले , नाते – रिश्तेदार सब बीजी को उलाहना देते – लड़की तुम्हारी कुछ जानती नहीं – न खाना बनाना, न सीना-पिरोना, उसे घरेलू काम भी सिखाओ। पर बीजी और पापा का एक ही कहना था – शादी के बाद तो घर-गृहस्थी संभालनी ही है, अभी जितना पढ़ना है, पढ़ ले । कोई ताज्जुब नहीं कि छब्बीस साल की उम्र में शादी होने के बाद भी मैं दालों को पीली, हरी और काली के नाम से जानती थी और दो लोगों का खाना बनाने में सारा दिन जुटी रहती थी।
हर वक्त पढ़ते रहने का जुनून और उधर दादा-दादी का शादी के लिये हर वक्त कोंचते रहना – मैं बीमार रहने लगी । कुछ अजीब सी बीमारी थी वह – बायें हाथ की कुहनी इतनी बुरी तरह सूज जाती थी कि हाथ हिलाना मुश्किल हो जाता था । मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है , जब मैंने 27 मई 1964 को – जिस दिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी । अपनी पहली रचना मैंने तभी लिखी थी । मैं बीमार थी और मुझे लग रहा था – आज मेरी ज़िन्दगी का आखिरी दिन है । तभी रेडियो पर नेहरु जी की मौत की ख़बर थी । देश का एक एक आदमी शोक में डूबा था । रेडियो पर “चाचा नेहरु अमर रहें” के आर्तनाद थे । रोती कलपती महिलायें और चीखते चिल्लाते नवयुवक और बच्चे । मुझे लगा, मैं कितनी अदना-सी चीज़ हूं – जिसके मरने पर पत्ता भी नहीं कांपेगा, मैं मर गई तो कुछेक दिन मेरे मां-बाप रो लेंगे, उसके अलावा कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस, यही सोच-सोचकर मैं रोती जा रही थी । सब समझ रहे थे – मैं अपने प्यारे प्रधानमंत्री की मौत पर रो रही हूं। मैंने अपनी पहली कविता भी मौत पर लिखी और पहली कहानी भी । बहुत संकोच के साथ मैंने वह कहानी पापा को पढ़ने को दी – कहानी क्या थी, अपनी लम्बी बीमारी से उपजे डिप्रेशन की एक निहायत बेवकूफ़ी भरी दास्तान थी । उस कहानी को पढ़कर लौटाते हुए बीजी रोने लग गयीं , उन्होंने मेरे हाथों को माथे से लगाया और पापा बेहद भावुक हो गये, लेकिन कहानी पर बहुत संतुलित और सही राय दी । बोले , “ अच्छा हुआ , एक बीमार लड़की की कहानी तुमने लिखी , अब इससे मुक्त होकर दूसरे विषय उठाओ और उनपर लिखो । “ और उन्होंने अपने साहित्यकार मित्र राजेन्द्र यादव की कुछ किताबें मुझे थमा दीं। साथ ही विशाल भारत के पुराने जिल्द बंधे कुछ अंक उन्होंने मुझे पढ़ने को दिये । उन दो – तीन सालों में मैंने ख़ूब पढ़ा और खूब लिखा और मेरी हर कहानी के पहले पाठक सन् 1971 तक (जबतक मेरी शादी नहीं हो गई) मेरे पापा, बीजी और बेहद ज़हीन भाई प्रमोद रहा।
हां, तो बात यह हो रही थी की पापा का मन व्यवसाय में कभी नहीं रमा। व्यवसाय का न उन्हें कोई अनुभव था, न रुचि । पर बड़े परिवार की ज़िम्मेदारी का तकाजा तो था ही। दादा के जाने के बाद अकेले पड़ गये पापा ने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप में जब भी कोई काम बेहद जोश के साथ शुरू किया, अपने सीधे स्वभाव के कारण उन्होंने व्यवसाय में धोखा ही खाया और हर पनपते व्यवसाय से अपने अनाड़ीपन में सबकुछ अपने पार्टनर के हाथ थमा पल्ला झाड़कर बाहर निकल आये । बीजी उन्हें हमेशा आगाह करती रहीं पर पापा को व्यवसाय में बीवी की बात सुनना अपनी हेठी लगता था।
कलकत्ता में चौरंगी स्थित नामी गिरामी विशालकाय रेस्तरां “कल्पतरु” खुद शुरु किया पर अपनी बहन की आर्थिक तंगी देखकर बहनोई को पार्टनर बना लिया और मां के बरजने के बावजूद अन्ततः फलते फूलते व्यवसाय को तिलांजलि देकर सबकुछ अपने बहनोई को दे डाला।इसके बाद पापा में कई बदलाव आये, जिसे हम दोनों बहनें बेहद अचम्भित – सी देखती रहीं ।

जो पापा दादी की ठाकुरों की मूर्ति पूजा का मज़ाक बना कर दादी को खिझाया करते थे, अप्रत्याशित रूप से पूजा-पाठ और आध्यात्म की ओर मुड़ गये । दादी के ठाकुरों की मूर्तियों, उनकी आरती, पूजा – अर्चना, भोग-प्रसाद की हमेशा खिल्ली उड़ाया करते थे, अचानक घोर धार्मिक हो उठे। उनके ज़रूरत से ज्यादा धार्मिक कर्मकांड ने हममें से कुछ बच्चों को प्रतिक्रिया स्वरूप, एक सिरे से घोर नास्तिक बना दिया।
दूसरा बदलाव उनमें यह आया कि वह पापा, जो बच्चों की उपस्थिति का ख़याल किये बिना, बीजी को हमेशा “न्हाने’ ‘विन्नी’ जैसे बड़े प्यार भरे सम्बोधन से बुलाया करते थे, अचानक उनके प्रति बड़े रूखे और साफ़ शब्दों में कहें तो ‘जालिम’ हो उठे। आर्थिक परेशानी और निराशा के उन दिनों में बीजी की कोई सलाह या हमदर्दी उनपर मरहम लगाने की जगह आग में घी का काम करती। यह शायद वह ज़माना था, जब अपनी पत्नी की सलाह मानना मध्यवर्गीय पुरुष को अपनी शान के खिलाफ़ लगता था। उठते –बैठते, हर जगह, हर किसी के सामने बीजी को अपना मुंह खोलते ही इस तरह के वाक्य सुनने पड़ते –
“ तुमसे चुप क्यों नहीं रहा जाता ?”
“ तुम बेवकूफ़ी की बातें मत करो । किसी बात की समझ न हो तो मत बोला करो । बिजनेस की बातों में टांग मत अड़ाया करो। “
“ तुम्हें तो अक्ल ही नहीं है। रसोई से बाहर की बातों में दखल मत दिया करो।
“अपनी अक्ल बस रसोई में ही चलाया करो !”
रोज दर रोज कम अक्ल और बेवकूफ़ होने के तमगे अपनी पोशाक पर टांकते हुए बीजी लगातार चुप होती चली गयीं । अब पापा के सामने वह सिर्फ़ एक श्रोता की भूमिका अदा करतीं। पापा अपने व्यवसाय की समस्याओं के बारे में बताते और वह बग़ैर अपनी राय दिये चुपचाप सुनतीं और वहां भी इस समझदारी के साथ कि तुम्हारे पापा के पास और कोई है भी तो नहीं जिससे वह अपने मन की बात कह सकें। सबसे बड़ी होने के नाते मां का यह दर्द सबसे ज्यादा मेरे हिस्से में आया। अपने पति और बच्चों द्वारा बेशक वह घर संभालने और खाना पकाने वाली एक नौकरानी की तरह ट्रीट की जातीं, पर बिना किसी गिले- शिकवे के हम सब को खुश रखना उनका एकमात्र सरोकार होता । पापा को खाना खिलाते वक्त वह इतनी सतर्क रहतीं कि खाना बिल्कुल वैसा बना हो जैसा पापा को पसंद है – भिंडी – न ज्यादा भुनी, न हरी, बैगन का भुरता ठीक बराबर के प्याज-टमाटर के अनुपात के साथ, दाल ऐसी जो उंगली पर चढ़े, घी बराबर उतना ही जितना दाल में होना चाहिये, और खाते वक्त एक फुलका ख़त्म हो, तभी दूसरा गरम फुल्का उनकी प्लेट में आये ।
उधर पापा का भी हाल यह कि बीजी सामने हों तो उन्हें ज़बान खोलने न देना या उनके हर छोटे-बड़े काम में नुक्स निकालना पर एक घंटे के लिये भी बीजी बाहर चली जायें तो उनके लिये सांस लेना दूभर हो जाता था । एकबार वे हम बच्चों को लेकर स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में बुआ के पास देहरादून चली गयीं तो हफ्ते भर बाद ही एक्सप्रेस टेलीग्राम देकर उन्हें वापस बुलाया गया । बीजी के बिना पापा की दुनिया का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता था ।
तब मैं समझ नहीं पाती थी कि बीजी और पापा का यह कैसा लव-हेट रिलेशनशिप है कि पापा , बीजी के बिना रह भी नहीं सकते और साथ रहने पर ऐसा सुलूक करते हैं जैसे उनके साथ कोई इन्सानी रिश्ता ही नहीं ।
उन दिनों अपने मां-बाप के बीच इस तरह के अजीब परेशान करने वाले सम्बन्धों ने शायद मेरे भीतर विद्रोह के बीज डाल दिये । अठारह-बीस साल की उम्र से पहले ही दस-बारह कहानियां लिख कर मिली प्रतिष्ठा ने मेरा दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा दिया था । अपने – आप को कलाकार समझने लगी मैं और कलाकार फितूरी-सनकी-खब्ती होते हैं, यह साबित करने के लिये एक इश्क भी कर डाला।
अगस्त, 1966 की वह रात मुझे आज भी साफ़-साफ़ याद है, जब मैंने कई दिनों की जद्दो जेहद के बाद ऐलान किया कि मै अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना चाहती हूं। मेरा बीसवां जन्मदिन अभी नहीं आया पर अठारह पूरे कर मैं बालिग तो हो ही चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि पापा जिस तरह बीजी पर गरजते-बरसते रहते हैं, यह सब सुनते ही आगबबूला हो जाएंगे और मुझे कमरे के पलंग पर धकेल कर लात-घूंसों से मेरी अच्छी खासी मरम्मत की जाएगी। हिन्दी फिल्मों की विद्रोहिणी नायिका की इमेज मेरे दिमाग में मय रंग-रेखाओं के स्थापित हो चुकी थी। खिड़की की सलाखों से रस्सी बांधकर नीचे कूदती जां-बाज़ प्रेमिका वाली स्थिति के लिये मैं पूरी तरह तैयार थी।…..
लेकिन मेरे दुस्साहसी ऐलान की बेहद अनपेक्षित प्रतिक्रिया हुई । पापा बड़ी संजीदगी से बोले , “ अब तुम बड़ी हो गई हो, अपना भला-बुरा खुद समझ सकती हो पर हम चाहेंगे कि तुम एक महीना उस आदमी से न मिलो और अपने आप को टटोलो कि क्या सारी ज़िन्दगी बिताने के लिये वह एक सही आदमी है। एक महीने बाद जो तुम्हारा निर्णय होगा, हमें मंजूर होगा। “ मेरे सारी विद्रोही मंसूबों पर उनकी इस संक्षिप्त प्रतिक्रिया ने घड़ों ठंडा पानी उंड़ेल दिया और मेरी बग़ावत के गुब्बारे की हवा निकाल दी।
उस शाम अगर वह मेरे साथ सख्ती से पेश आये होते तो निश्चित रूप से घर छोड़कर मैं अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की नासमझी कर बैठती। उनके इस प्यार और विश्वास से भरे शब्दों ने मेरी ज़िन्दगी में होनेवाली कितनी बड़ी ट्रेजेडी से मुझे तो बचा लिया, पर मेरे थोथे बगावती तेवर से जूझने में उनकी सारी ताकत चुक गई और वे मेरी छोटी बहन के लिए अतिरिक्त सतर्क हो गए जिसने उस ज़हीन और खूबसूरत लड़की का बहुत नुकसान किया।
लेकिन मेरे साथ जो बेहद सही वक्त पर सही राय देते हुए और सही कदम उठाते हुए पेश आये , वही पापा मुझसे छोटे भाई-बहनों के सन्दर्भ में कब-कैसे ग़लत हो गये, इस चक्रव्यूह को समझना मुझे अक्सर उदास कर जाता है, इसलिये इसमें उलझने से हमेशा बचती रहती हूं। यह उनके ज़रूरत से ज्यादा प्यार-दुलार-सुरक्षा का नतीजा रहा जिसने बैक-फ़ायर किया । बिजनेसमैन पिता होते हुए भी पैसे को लेकर हमेशा उनका पूरी तरह अव्यावहारिक और फक्कड़ दृष्टिकोण रहा। वह हमेशा अपने बनाये ‘यूटोपिया’ में रहते थे । सांसारिक व्यवहार कुशलता कूटनीति, छल-छद्म, बेईमानी – वे सारी चीजें, जो एक व्यवसायी आदमी को बेहतर भौतिक सुविधाएं या परिवार में एक “मालिक“ का रुतबा दिला सकती हैं, उनमें पूरी तरह अनुपस्थित थीं । बाप-बेटे या भाई-भाई के बीच भी रुपये-पैसे को धुरी मानकर चलती दुनिया में वह बड़ी उदारता से, अपने जीते-जी अपनी ज़िन्दगी भर की कमाई, जब-जिस बेटे ने जितना मांगा, उनके नाम करते चले गये। और एक दिन अपने ही गढ़े हुए साम्राज्य में अपने बेटों की ‘ज़रूरत’ या ‘ताकत’ बनने की संभावना से खुद हाथ धो बैठे ।
पंचानबे पार के बाद भी रोज़ नियमित योगाभ्यास और नियमित पूजा-पाठ के अनुशासन से बंधी दिनचर्या में उनकी ज़िन्दगी से लड़ने की ताकत हमेशा बरकरार रही। उन्हें देखकर यह अफ़सोस होना स्वाभाविक था कि जिन बच्चों पर बीजी – पापा ने जान छिड़की , जिन्हें कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने दिया, जिनकी हर मांग अपनी सामर्थ्य से आगे जाकर भी पूरा करने की कोशिश की – उन्हीं बच्चों से उपेक्षा, तिरस्कार और कड़वे बोल झेलते हुए वह एक ईश्वरीय-पारलौकिक विश्वास के भरोसे जीते रहे। अपनी बेलौस हंसी की तह में वह अपनी तकलीफ को बाहर झांकने नहीं देते क्योंकि उसके लिये भी खुद अपने को ही दोशी ठहराते रहे।
16 दिसंबर 1999 को बीजी नहीं रही । उनका मेरे पास मुंबई आकर उस तरह चले जाना एक रिसता हुआ जख्म है, उस पर फिर कभी। पर पापा की दिनचर्या देख कर हमेशा मन होता था, काश, इसका दसवां हिस्सा भी बीजी ने अपने जीते जी देखा होता तो कम से कम थोड़ा सा सुकून लेकर जातीं । बीजी की तबीयत कितनी भी खराब हो, रात भर के उनींदे के बाद उनसे सुबह उठा न जा रहा हो, पर पापा सोती हुई बीजी को बड़ी बेमुख्वती से हर दस मिनट बाद आवाज़ देकर उठा देते – चलो, चाय बनाओ । गिरते – पड़ते बीजी उठतीं और चाय बनातीं ।
जिन्होंने कभी अपने हाथ से पानी का गिलास उठाकर नहीं पीया , वह पापा 95 साल की उम्र तक सुबह उठकर , बड़े शांत भाव से न सिर्फ़ अपने लिये चाय बनाते, बल्कि कल्पना ( जो घर की अन्नपूर्णा है और पूरा घर संभालती है और अब हमारे घर का एक अनिवार्य हिस्सा हो गई है) के लिये भी चाय बनाकर रखते थे। बीजी के हमेशा के लिए चले जाने ने पापा को अपने पैरों पर खड़े होना सिखा दिया था । यह ‘आत्मनिर्भर’ रूप देखने के लिये मेरी मां तरसती रह गईं। तब पापा ने कभी उनको बस एक कप चाय बनाकर दी होती……. तो वे जिंदगी से इतनी असंतुष्ट न जातीं पापा का वजन कभी पैंतालिस किलो से ज्यादा नहीं रहा। अपनी सेहत का राज वह बताते थे कि एक दिन अपनी सोप फैक्टरी – जहां साबुन बनता था, कटता था, पैक होता था – में मशीनों को चलते और रुकते देख उन्हें यह ख्याल आया कि इन मशीनों को हर हफ्ते ग्रीज़ करना पड़ता है, इनमें तेल डालना पड़ता है। जिस मशीन को पांच-सात दिन न चलाओ, वह खड़ खड़ करने लगती है, चलते हुए अटकती है तो अपना शरीर भी तो एक मशीन ही है। तब से उन्होंने अपने योग व्यायाम खुद तय किए। कभी किसी योग शिक्षक को नहीं रखा। रोज शरीर के हर जोड़ को हिलातें और नियम से एक घंटा व्यायाम करते। 85 साल की उम्र तक रोज पांच किलोमीटर चलते । कभी सर्दी-खांसी, बुखार या पेट खराब हो भी जाए तो प्राकृतिक या होमियोपैथिक इलाज करते। अपने लिए कभी अस्पताल नहीं गए । एक बार अस्पताल गए तो होश आते ही इतना बवाल खड़ा कर दिया कि उन्हें घर लाना पड़ा । डॉक्टरों की ऑपरेशन की तैयारी धरी रह गई।
लौटने पर कहते हैं – उस दिन अगर ऑपरेशन टेबल पर मेरा राम नाम सत्त हो जाता तो डॉक्टरों ने तो कहना था कि एज फैक्टर है। मैं डॉक्टर के हाथों हलाल नहीं होना चाहता, मरना तो मुझे अपने घर में ही है।लेकिन अपने बनाये उस तिमंज़िले मकान में पापा ने मां के जाने के बाद खुद को जैसे कैद कर लिया । अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त होकर नयी-नयी जगहों में घूमना उनकी किस्मत में नहीं था। न वह मेरे पास मुंबई आए, न और कहीं गएं।
“ यह आप अपने आप को किस बात की सज़ा दे रहे हैं ? “ मैंने पापा से पूछा था ,” आप क्यों नहीं इस शहर से बाहर निकलते ?
“ मैंने जो ग़लतियां की हैं , उसकी सज़ा भी मुझे खुद ही भुगतनी है । ईश्वर की अदालत में मुझे कसूरवार ठहराया गया हैं । मैंने अपने कुछ बच्चों के साथ न्याय नहीं किया । वह आज की दुनिया के लिहाज़ से सरल और सीधे थे । पर मैं तो अनुभवी था, मैंने अपनी विचारशक्ति क्यों ताक पर रख दी । उनकी उपेक्षा करने की सज़ा यही है कि मैं मरते दम तक उन ग़लतियों का नतीजा शान्ति और संयम के साथ देखूं । अब उनसे भागने की कोशिश करना स्वार्थ या कायरता होगी ।“
सुना तो मैंने भी था कि आज के ज़माने में ईश्वर भी सीधे और ईमानदार इन्सानों के प्रति बेरहम होता है। पर यह ईश्वर पापा का ईश्वर नहीं है। बेहद बेहद विपरीत स्थितियों में भी उनसे ज़्यादा संतुष्ट प्राणी इस धरती पर मैंने नहीं देखा।
2021 में अपनी जन्म शती मनाने से डेढ़ साल पहले पापा एकाएक चले गए।
1 जनवरी 2019 को उनकी अंत्येष्टि हुई। सुबह उठे, चाय पी, खबरें सुनी, फिर फोन पर अपनी बहन से, अपनी बहू से यानी मेरी भाभी से बात की, फिर स्नान के लिए कल्पना – कोलकाता की हमारी अन्नपूर्णा – से कपड़े मांगे। कल्पना ने मना किया – पापाजी, ठंड बहुत है, आज नहाने मत जाइए । बोले- अरे, ठंड है तो क्या नहाना छोड़ दें? बाथरुम गए। जब आधे घंटे से ऊपर हो गया और वे बाहर नहीं निकले तो कल्पना ने बाथरुम के दरवाजे की कुंडी खड़काई – इतना देरी क्यों पापाजी ? कोई जवाब नहीं । उढ़का हुआ दरवाजा जरा सा खोलकर देखा तो पीढ़े पर बैठे हुए पापाजी का सिर एक ओर लुढ़का है और बाल्टी में खुले नल की टोटी से पानी गिर रहा है। उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया। वे जा चुके थे। ऐसे ही जाना चाहते थे वे। एक दिन के लिए भी बीमार पड़ना मंजूर नहीं था उन्हें। कभी अपनी सेवा के लिए कोई अटेंडेंट न रखा।
अपना सौवां जन्मदिन मनाना चाहते थे।हमेशा मेरे जाने पर बिगड़ते – सेंचुरी लगाउंगा, तब आना।
…… लेकिन उससे पहले ही चुपचाप निकल लेने की ठान ली थी उन्होंने।
हद दर्ज़े के ज़िद्दी तो वे जनम से थे।
जाते जाते भी अपनी ज़िद निभाई।

सुधा अरोड़ा
90824 55039