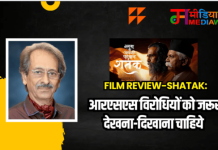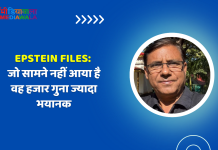उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजो ने इस सवाल को फिर रेखांकित किया है कि चुनाव जिताने वाले मुद्दे और अमूमन जनता के समझे जाने वाले मुद्दों में इतनी तफावत क्यों है? बुद्धिजीवी जिन्हें असल मुद्दे मानकर परसेप्शन का जो महल खड़ा करते हैं, आम आदमी उससे वैसा इत्तफाक क्यों नहीं रखता, जो नतीजों को भी उसीके मुताबिक उलट दें?
पिछले कुछ सालों में यह देखने में आ रहा है कि आम आदमी की जिंदगी से जुड़े मुद्दे तथा जद्दोजहद कुछ और है लेकिन उसका चुनावी जनादेश कुछ और होता है? इसी से यह सवाल भी नत्थी है कि वोटर आखिर बात से प्रभावित होकर अपना वोट देता है, अपना राजनीतिक मन बनाता है? इसको लेकर बौद्धिक जुगाली करने वाले ज्यादा समझदार हैं या फिर वोटर ज्यादा समझदार है? अथवा यह केवल समाज के एक वर्ग द्वारा ‘बिल्ली’ को ‘बाघ’ के रूप में देखने- दिखाने की कवायद है, जिससे आम वोटर ज्यादा इ्त्तफाक नहीं रखता?

ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पांच राज्यों में से यूपी में जिन मुद्दों को लेकर सत्ता परिवर्तन की हवा बनाई जा रही थी, वो जमीन पर नदारद दिखी। यहां हम राजनेताअों के बढ़चढ़ कर किए जाने वाले दावों और वादों की बात नहीं कर रहे हैं। पिछले डेढ़ साल से एक बड़ा मुद्दा यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में किसान आंदोलन का था। बेशक तीन विवादित कृषि कानूनो को लेकर भाजपा के प्रति किसानों में नाराजी थी। इसे लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर साल भर से ज्यादा समय तक आंदोलन चलाया गया।
माहौल यूं बनाया गया कि अगले चुनावों में यही एक निर्णायक मुद्दा साबित होने वाला है। इसका एक संदेश यह भी था इस देश का किसान इतना स्वार्थी है कि उसे अपनी उपज के बेहतर मूल्य पाने और अपने संघर्ष से ज्यादा किसी से मतलब नहीं है। यह सोच उसी तरह की है, जैसे कि मनुष्य के वजूद को केवल पेट में समेट देना या मनुष्यता को राष्ट्र की पहचान में विलीन कर देना। यह आसानी से भुला दिया गया कि किसान भी इस देश का जिम्मेदार वोटर है। उसकी दुनिया फसल की उपज से आगे भी है। वह भी दूसरे मुद्दों पर अपने ढंग से सोचता है। समग्रता में चीजों को आंकता है, तौलता है। वैसे भी जो दूसरे के लिए अन्न उपजाता हो, वो अपने स्वार्थ तक सीमित रह ही नहीं सकता।

बेशक किसान आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन था, लेकिन वही सब कुछ नहीं था। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव नतीजों ने साबित कर िदया। साल भर तक किसान आंदोलन संचालित करने वाले संयुक्त किसान मोर्चे के तहत आने वाले 25 किसान संगठनो ने नया ‘संयुक्त समाज मोर्चा’ बनाकर पंजाब में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। सीट जितना तो दूर, शायद उन सभी जमानत जब्त हो गई। यानी किसानों ने ही उन्हें वोट नहीं दिए। यानी किसान की नाराजी किसान मोर्चे के पक्ष में ही ट्रांसलेट नहीं हुई।
उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसानों की नाराजी को ‘भाजपा का काल’ बताया जा रहा था, वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला। नतीजो के बाद बड़बोले किसान नेता नरेश सिंह टिकैत कहीं नजर नहीं आए। कहा जा सकता है कि भाजपा के हिंदुत्व के आग्रह ने पश्चिमी यूपी में वैसा मुस्लिम-जाट समीकरण नहीं बनने दिया, जैसा कि बताया जा रहा था। भाजपा ने इस मुद्दे की गहराई को शायद पहले ही भांप लिया था। इसीलिए चुनाव के तीन माह पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीनो कृषि कानून वापस लेकर मुद्दे की सियासी हवा निकाल दी।
अगर पंजाब की बात करें तो जिन कृषि कानूनों के विरोध और बरसो राज्य में सत्ता में रहा अकाली दल एनडीए से अलग हुआ, उसे भी किसानों ने चुनाव में वोट नहीं िदए। उसके तो सभी सेनापति भी धराशायी हो गए। यही नहीं वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने किसान आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया था। लेकिन किसानों ने कांग्रेस की जगह उस आम आदमी पार्टी को बंपर समर्थन दिया, जो किसान आंदोलन का समर्थन तो कर रही थी, लेकिन खुलकर सामने भी नहीं आ रही थी।

पंजाब में आप और यूपी उत्तराखंड में किसानों द्वारा भाजपा को बड़े पैमाने पर वोट करने का अर्थ क्या समझा जाए? किसान नामसझ हैं या फिर जिस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभारा गया, उसमें वैसा चुनावी दम नहीं था, जैसा पेंट किया जा रहा था? इसका अर्थ यह कतई नहीं कि किसानों की समस्या को नजर अंदाज किया जाए या उसके प्रति असंवेदनशील हुआ जाए। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि खुद किसान और आम आदमी किन मुद्दों को लेकर ज्यादा संवेदनशील है, जो उसे सत्ता परिवर्तन के लिए विवश कर दे।
यहां प्रश्न यह भी है कि हमे मुद्दों को किस लैंस से देखना चाहिए? उसे कितना मैग्नीफाय करके समझना चाहिए? सवाल यह भी उठता है कि किसान आंदोलन या शाहीन बाग जैसे आंदोलन अपने आप में सचमुच उतनी गहराई और व्यग्रता लिए होते भी या नहीं या फिर वो केवल राजनीतिक प्रयोगशाला का एक और प्रयोग भर होते हैं। जिसमें आम आदमी इस्तेमाल हो जाता है।
यकीनन इस देश का वोटर उन कथित चिंतकों से ज्यादा समझदार और जमीन के करीब है। क्योंकि वो अपनी जायज समस्याअों के बरक्स उन कोणों से भी सोचता है, जो चुनाव नतीजों की दिशा तय करते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर राजनेता अभी भी चुनावी समीकरणों को अंकगणित का फार्मूला मानकर चलते हैं। यूपी और पंजाब के चुनाव ने उसे भी ध्वस्त किया है। परिणामों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे महाबड़बोले जातिवादी नेता परिदृश्य से गायब दिखे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के उस अमर डायलाॅग कि ‘ हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है’ की तर्ज पर ये दावा किया था कि वो जिस पार्टी में शामिल होता है, वही सत्ता सिंहासन पर सवार होती है।

यकीनन इस बार अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने जातियों का कागजी समीकरण अच्छा तैयार किया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। आम आदमी योगी राज और उनके पूर्ववर्तियों के राज की मन ही मन तुलना कर रहा था और तमाम खामियो के बाद भी उसे बेहतर पा रहा था। लिहाजा उसने योगी को एक मौका और दे दिया।
पंजाब में दलित वोटों का बड़ा हल्ला रहा। पार्टी की अंतर्कलह को खत्म करने कांग्रेस आलाकमान ने पानी की जगह पेट्रोल डाला। इस कागजी गणित कि पंजाब में 31 फीसदी दलित वोट निर्णायक है, बेचारे दलित चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई। लेकिन परिणामों ने साबित िकया कि चन्नी को दलितो ने भी वोट नहीं दिए। क्योंकि पंजाब में दलितो के बीच भी काफी अंत:विभाजन है।
यह भी विडंबना है कि जिन चंचल राजनीतिज्ञ और लाॅफ्टर शो के ठहाकेबाज जज नवजोतसिंह सिद्धू को राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी, उन्हीं सिद्धू को लाॅफ्टर शो के एक कंटेस्टेंट भगवंत मान ने चुनावी अखाड़े में जमीन सुंघा दी। यह बात अलग है कि उस जमाने में भगवंत मोना सिख हुआ करते थे। राजनीति में आने के बाद उन्होनें अपना हुलिया बदला और पूरे िसख हो गए।

सिद्धू का चुनाव में ‘आम आदमी पार्टी’ की एक गुमनाम प्रत्याशी से हार कर तीसरे नंबर पर रहना इस बात का प्रतीक है कि आप अब कांग्रेस की जमीन खाती जा रही है। अभी यह पंजाब में हुआ है, कल को दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। हालांकि आप अपनी बंपर जीत को आम आदमी के मुद्दों पर बात की जीत बता रही है, लेकिन हकीकत में वो कांग्रेस का विकल्प के रूप में उभरी है। लोग अब परिवारवादी पार्टियों से ऊबने लगे हैं, बादल परिवार का चुनाव में निपटना इसी का संकेत है।
इसमें संदेह नहीं कि आज लोगों की जिंदगी कष्टों से भरी है। बेरोजगारी है, महंगाई है, अच्छी शिक्षा का सुलभ न होना है, सस्ते और कारगर इलाज की कमी है, लेकिन ये सब रोजमर्रा के मुद्दे हैं। ये चुनावी जश्न की आरती नहीं बन पाते। ऐसा क्यों? इसका सही जवाब बहुत कठिन है। एक आम वोटर चुनाव में राजनीतिक दलो को शायद कई पैमानों पर तौलता है। जो व्यक्ति सापेक्ष भी हो सकते हैं और समाज सापेक्ष भी।

यह सच है कि पहले नरेन्द्र मोदी ने और अब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने महिला मतदाताअों के एक बड़े वर्ग को अपना मुरीद बना लिया है। इसमें सुरक्षा का आश्वस्ति भाव भी है और मर्दानगी का अंदाज भी। महिलाएं और खासकर हिंदू महिलाएं इन दोनो के पक्ष में चुनाव में खामोश दीवार बन कर खड़ी होती दिखती हैं। इसका अर्थ यह नहीं िक यूपी में या पूरे देश में सचमुच राम राज्य आ गया है लेकिन जो छवि महिलाअों के दिलों पर अंकित हो गई है या कर दी गई है, वो राखी के रक्षा सूत्र की तरह है।
पांच में से चार राज्यों में बीजेपी की सत्ता में वापसी को भाजपा विरोधी वोटों के विभाजन का नतीजा भी बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी विरोधी वोट एकजुट हो तो भगवा को मात दी जा सकती है। हमारे लोकतंत्र में जीत के लिए पचास फीसदी पाने की वोट की अनिवार्यता नहीं है। अगर सत्ता से हटाने का यही फार्मूला है तो पश्चिम बंगाल में ममता बैनर्जी तीसरी बार 48.02 प्रतिशत, अोडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी 44.71 प्रतिशत और केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार 45.43 फीसदी वोट लेकर सत्ता में लौटी है।
यानी बहुमत वहां भी बंटा हुआ था। वहां भी सत्तारूढ़ दलों को हटाने के लिए बाकी विरोधी वोट को एकजुट करने की जरूरत है। लेकिन यह सोच सही नहीं है। सोचा इस बात पर जाना चाहिए कि जनता उन मुद्दों को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं मानती, जिसे हम मुद्दे मानकर चलते हैं और उसी की बिना पर सारा गुणा भाग करते हैं। दोनो में इतना फर्क क्यों है? चश्मो की वजह से या फिर जनता को उसका व्यापक हित किसमें है, यह न समझा पाने की वजह से? बेशक इसमें प्रचार और छवि निर्माण भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसा ही होता तो संसाधनो में काफी पीछे रही आप दिल्ली और पंजाब में साधन सम्पन्न दलों को धूल नहीं चटा पाती। अगर इन सबके बाद भी कोई जनता को ही ‘मूर्ख’ बताने की हिमाकत करे तो मूर्ख की अलग से परिभाषा करने की जरूरत ही क्या है?