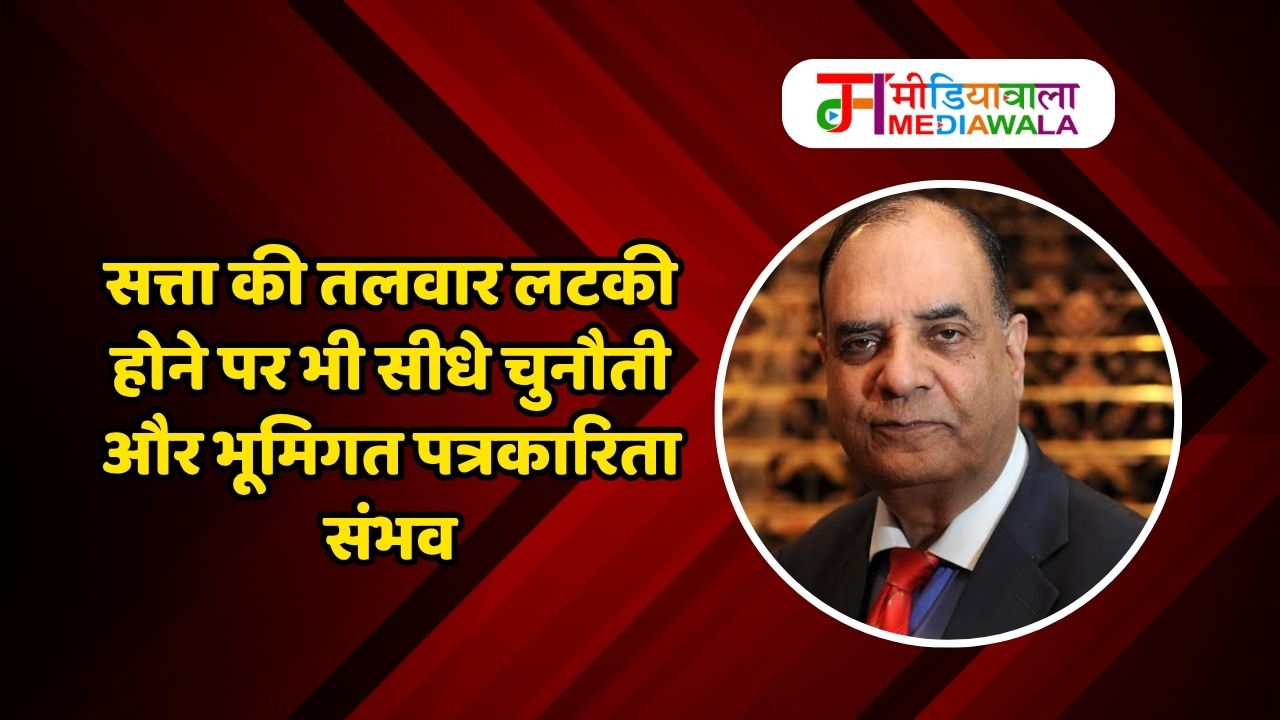
सत्ता की तलवार लटकी होने पर भी सीधे चुनौती और भूमिगत पत्रकारिता संभव
आलोक मेहता
आपात काल ( इमरजेंसी ) में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अत्याचार , गिरफ्तारियों , सेंसरशिप की चर्चा 50 वर्षों के बाद फिर गर्म हुई | लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सत्ता की तलवार लटकी होने के बावजूद भारत के कई सम्पादकों पत्रकारों ने विरोध के साथ सरकार को न केवल चुनौती दी , वरन भूमिगत गतिविधियों के लिए सूचनाएं पहुँचाने , लिखित या छपी सामग्री प्रकाशित कर देश भर में बंटवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | मैं 1971 से दिल्ली में न्यूज़ एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार में संवाददाता के रुप में कार्य कर रहा था | राजनीतिक और संसद की रिपोर्टिंग करता था | इसलिए गुजरात और बिहार के सरकार विरोधी आंदोलनों पर खबरों के साथ अख़बारों में लेख भी लिखता था | हिन्दुस्थान समाचार के प्रधान प्रबंध संपादक बालेश्वर अग्रवाल और ब्यूरो प्रमुख राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे थे , लेकिन भारतीय भाषाओँ की प्रमुख न्यूज़ एजेंसी होने से कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों नेताओं से अच्छे संपर्क सम्बन्ध थे और मेरे जैसे युवा पत्रकार को उन्होंने ही इन नेताओं से मिलाया था | केंद्र और राज्यों की सरकारें एजेंसी की ख़बरों के टेलीप्रिंटर अपने दफ्तरों में लगाने के लिए हर महीने जो पैसा देती थी , वह आमदनी का प्रमुख स्रोत होता था | इसलिए 1975 में इमरजेंसी लगने पर मेरे जैसे पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा झटका था | संयोग से संपादक के आदेश से कुछ महीने मुझे गुजरात में भी काम करना पड़ा और दिल्ली आना जाना चलता रहा | सरकार द्वारा फ़रवरी 1976 में देश की दो अंग्रेजी और दो हिंदी की न्यूज़ एजेंसियों के विलय से पहले मुझे हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में संवाददाता की नौकरी मिल गई | इसलिए मुझे सत्ता तथा विरोध की गतिविधियों की जानकारियां भी मिलती रही |
26 जून, 1975 को राष्ट्रपति ने एक आदेश के जरिए आपातकाल की घोषणा के साथ कहा गया था कि देश में गंभीर संकट पैदा हो गया है। आंतरिक उपद्रवों के चलते देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। इमरजेंसी लगाने के साथ ही प्रेस पर भी हमला बोल दिया। इमरजेंसी की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन प्रेस सेंसरशिप का खाका तैयार नहीं था। सरकार की नजर में अखबारों को छपने से रोकना जरूरी था। अखबारों की बिजली 26 जून से लेकर 29 जून तक गुल रही। बाद में सरकार ने सेंसरशिप की रूपरेखा तैयार की और प्रमुख सूचना अधिकारी डाॅ. बाजी को चीफ सेंसर नियुक्त कर दिया। वह तब तक चीफ सेंसर का काम देखते रहे जब तक कि इस पद पर एच.जे.डी. पेन्हा की स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं हुई। प्रधान मंत्य्री श्रीमती गांधी प्रेस से बहुत खफा थीं। 22 जुलाई, 1975 को उन्होंने राज्यसभा में दिए भाषण में कहा कि ‘‘पहले जब अखबार नहीं थे तो आंदोलन भी नहीं थे। दरअसल, आंदोलन अखबार के पन्नों पर ही है। अगर आप जानना चाहते हैं, कि अखबारों पर सेंसर क्यों लगाया गया है तो उसका जवाब यही है। मुझे इस बात में थोड़ा भी संदेह नही है कि अखबार लोगों को भड़काते हैं , वे सांप्रदायिक उन्माद भी फैलाते रहे हैं।’’ श्रीमती गांधी मानती थीं कि प्रेस उनकी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने प्रेस पर झूठा, मनगढ़ंत बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और देश की गरिमा गिराने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि अधिकारों पर जोर देने और जिम्मेदारियों को भूल जाने से भयावह स्थिति पैदा हो जाती है और कुछ अखबार यही कर रहे हैं। वे कहती थीं कि सकारात्मक खबरों के लिए अखबारों में जगह नहीं है, जबकि गपशप, झूठ और देश की गरिमा गिरानेवाली खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। इससे देश कमजोर होता है और लोगो का मनोबल गिरता है। उन्होंने प्रेस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा गिराने और विपक्ष को दिशा-निर्देश देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहकर इमरजेंसी को जायज ठहराने की कोशिश की कि इमरजेंसी जिम्मेदारियों और अधिकारों में संतुलन कायम करने के लिए लगाई गई है।
इन्हीं विचारों के अनुसार 27 जून, 1975 को प्रेस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसमें अखबरों से कहा गया कि वे ऐसी खबरों को छापने से बचें, जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय की गरिमा गिरती हो। 5 अगस्त, 1975 को एक और दिशा-निर्देश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि ऐसी खबरों प्रकाशित की जाएं, जिससे कानून व्यवस्था को कोई खतरा न हो। देश के आर्थिक विकास से संबंधित खबरें ही प्रकाशित की जएं। सेंसर ऑफिस की ओर से एक और दिशा-निर्देश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार विरोधी किसी भी खबर या आंदोलन के प्रकार्शन को इजाजत नही दी जाएगी। संपादकीय जगहो को खाली छोड़ने या कोटेशन लिखने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, चीफ सेंसर ने राज्यों के सेंसर प्रमुखों को टेलेक्स संदेश भेजा-‘चूंकि सेंसरशिप के सारे निर्देश गोपनीय है और इनका मतलब सिर्फ पालन होने से है, इसलिए इ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सम्पादकों को इस बारे में मौखिक तौर पर बताएं। ‘
इस तरह सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसके खिलाफ कुछ भी न छपा सके। जो छपेगा, सबकुछ उसके समर्थक में छपेगा। सेंसर के आदेशों का नतीजा यह निकला कि सार्वजनिक क्षे़त्र उद्यमों की कार्यप्रणाली की आलोचना करनेवाला एमआरटीपी आयोग के चेयरमैन का बयान भी नहीं छपा। सेंसर ने अदालतों के आदेश छापने पर तो पांबदी लगा ही दी थी, जजों के तबादले की खबरें भी नहीं छप पा रही थीं। कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें थीं। उन्होंने कुछ संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे खबरें भी छपने से रोक दी गई।
मुझे याद है सबसे पहले मदरलैंड अख़बार के संपादक के आर मलकानी की गिरफ्तारी हुई | यह अखबार संघ के प्रकाशन संस्थान का था | दुर्भाग्य की बात थी कि कुछ सम्पादक इमरजेंसी लगाने के लिए इन्दिरा गांधी को ‘बधाई’ देने तक पहुंचे थे । दूसरी तरफ कभी लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गाँधी के साथ काम कर चुके कुलदीप नैय्यर जैसे प्रतिष्ठित संपादक कुलदीप नय्यर ने कुछ अखबारों और न्यूज एजेंसियों का चक्कर लगाकर पत्रकारों को अगले दिन (28 जून, 1975) सुबह 10 बजे प्रेस क्लब में जमा होने के लिए कहा। अगली सुबह मैं वहां 103 पत्रकारों का जमघट देखकर हैरान रह गया, जिनमें कुछ सम्पादक भी शामिल थे। कुलदीपजी ने ही एक प्रस्ताव तैयार कर लिया था जिसे उन सबने पास कर दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया था-‘यहां एकत्रित हुए हम पत्रकार सेंसरशिप लागू किए जाने की भर्त्सना करते हैं और सरकार से इसे फौरन हटाने का आग्रह करते हैं। हम पहले से ही हिरासत में लिए जा चुके पत्रकारों की रिहाई की भी मांग करते हैं।’ यह प्रस्ताव सबके हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री को भेज दिया गया ।
उन्ही दिनों ‘इंडियन एक्सप्रेस में उनका साप्ताहिक कालम छपा था। इसका शीर्षक था-‘नाॅट इनफ मिस्टर भुट्टो।’ यह जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान के बारे में था, जिसमें उनके और फील्ड मार्शल अयूब खान के कार्यकाल की तुलना की थी। उन्होंने लिखा था, ‘सबसे बुरा कदम उन्होंने लोगों का मुंह बन्द करके उठाया है। प्रेस के मुंह पर ताला लगा है और विपक्ष के बयानों को सामने नहीं आने दिया जा रहा है। मामूली-सी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है।’ कोई भी समझ सकता था कि यह इन्दिरा गांधी और इमरजेंसी की तरफ इशारा था । यह सच भी था। सेंसर को चकमा देने का यह भी रास्ता था। इस तरह के दो और लेख उन्होंने लिखे | इसके बाद सेंसर अधिकारियों ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ को निर्देश दिया कि ‘श्री कुलदीप नैयर द्वारा उनके अपने नाम से या किसी छद्म नाम से लिखा गया कोई भी लेख सेंसर को दिखाए बिना आपके अखबार में नहीं छपना चाहिए।’ बाद में कुलदीप नैय्यर जैसे प्रतिष्ठित संपादक और देश के अन्य भागों में कई पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई | कुलदीपजी और कुछ नामी संपादक जेल से जल्दी छूट गए , लेकिन वे फिर भूमिगत पत्र प्रकाशनों में ही लिखते और चर्चाएं करते रहे |
अंग्रेजी मासिक पत्रिक ‘फ्रीडम फर्स्ट ‘ के संपादक और जाने-माने नेता मीनू मसानी ने प्रकाशनी पर बंदिश लगाने के सेंसर के रवैये को कोर्ट में चुर्नाती दी। मीनू मसानी ने सेसर की काररवाई को चुनौती देते हुए 17 जुलाई, 1975 को मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इनके 11 लेखों को सेंसर ने छापने से रोक दिया था। मीनू मसानी की याचिका पर जस्टिस आर.पी. भट्ट ने सुनवाई की। जस्टिस भट्ट ने 26 नवंबर, 1975 को दिए फैसले में कहा कि इन 11 लेखो में ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिसे छपने से रोका जाए। उन्होंने ऐसे लेखों और सरकार की सकारात्मक आलोचनाओं को भी छापने के आदेश दिए। सेंसर ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। लेकिन उसे वहां भी मुहंकी खानी पड़ी। अदालत ने इस मामले में 10 फरवरी, 1976 को फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि व्यक्ति को आपातकाल में भी नाराजगी जताने का अधिकार है। इस आधार पर लेख का प्रकाशन नहीं रोका जा सकता।
‘इडियन एक्सप्रेस’ और ‘स्टेट्समैन’ ने सेंसर के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। स्टेट्समैन के प्रमुख निदेशक सी.आर. ईरानी और एक्सप्रेस के चेयरमैन रामनाथ गोयनका तथा उनके संपादकों ने बड़ी हिम्मत दिखाई। इसका नतीजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। इन्हें मिलनेवाले सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए। इनके साथ ही कुछ और संपादकों ने भी सेंसर के सामने झुकने से मना कर दिया। ए.डी गोरवाला ने भी सेंसर के सामने झुकने से मना कर दिया। ये ‘ ओपिनियन’ नाम से साप्ताहिक निकालते थे। पत्रिका ने एन.ए. पालखीवाला का एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख को आपत्तिजनक माना गया। कहा गया कि इस लेख से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा पर आचं आती है। इस लेख में पालखीवाला ने सुप्रीम कोट्र्र की कार्यवाहियों को रखा था। पत्रिका के संपादक से लेख में उद्धृत कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतियां पेश करने को कहा गया। मुंबई के चीफ सेंसर ने निर्देश जारी किया कि ऐसा न करने पर प्रेस जब्त किया जा सकता है, लेकिन संपादक गोरेवाला ने सेंसर की चेतावनी की परवाह किए बिना 17 फरवरी, 1976 को पत्रिका का एक अंक निकाला, जिसमें प्रेस की सेंसरशिप को लेकर बंबई हाईकोर्ट का एक फैसला छापा गया था। इस पर चीफ सेंसर ने ‘ओपिनियन’ का प्रेस जब्त कर लेने का 3 मई, 1976 को आदेश जारी किया। आखिर में 2 जुलाई, 1976 को ‘ओपिनियन’ के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन गोरेवाला फिर भी नहीं माने। वे साइक्लोस्टाइल कराकर डाक से पत्रिका भेजने लगे। तब चीफ सेंसर ने डाक विभाग के पोस्ट मास्टर जनरल से अपील करके उसका भी प्रसार रुकवा दिया। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ‘हिम्मत’ निकालते थे। उन्होंने भी सेंसर की परवाह नही की और काफी हिम्मत दिखाई। अक्तूबर 1975 में ‘हिम्मत’ को प्री-सेंसरशिप के लिए कहां गया। यह आदेश इस पत्रिका में छपे एक लेख के आधार पर दिया गया। लेख को आपत्तिजनक माना गया था। इसके बावजजूद ‘हिम्मत’ ने झुकना स्वीकार नही किया। वह चीजें छापता रहा, जो उसे सही लगती थीं। अगस्त 1976 में इस पत्रिका ने छापा कि श्रीमती गांधी ने कोलंबों में सेंसरशिप से संबंधित गलतबयानी की है। श्रीमती गांधी ने कहा था कि प्रेस को सेंसरशिप में छूट दे दी गई है। पत्रिका ने यह भी बताया कि किस तरह से प्रेस पर अभी भी शिकंजा कसा हुआ है। ‘हिम्मत’ जैसी ही हिम्मत ‘सेमिनार’ ने भी दिखाई। ‘सेमिनार’ की बहुत प्रतिष्ठा थी। उस दौरान ‘सेमिनार’ के जितने भी अंक निकले, सब में आपातकाल के औचित्य पर सवाल उठाया गया। दिसंबर 75 के अंक में इस पत्रिका ने पत्रकार कुलदीप नैयर के मामले को छापा। इस मामले में पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई मशहूर वकील पालखीवाला की दलील भी छापी।
गुजरात की पत्रिका ‘साधना’ और ‘जनता’ ने भी सेंसर का मुंहतोड़ जवाब दिया। ‘साधना’ मराठी और गुजराती में निकलती थी, जबकि ‘जनता’ अंग्रेजी में। पत्रिका का रुख सरकार विरोधी था। वे अपने हर अंक में सरकार विरोधी लेख प्रकाशित कर रही थी। जून 1975 से अक्तूबर 1975 के बीच पत्रिका के 11 अंक जब्त किए गए। प्रकाशक से एक हजार रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई और उसे भी जब्त कर लिया गया। आखिर में महाराष्ट्र सरकार ने पत्रिका को बंद करने के आदेश दे दिए। साधना के सम्पादक विष्णु पंड्या से मुझे कई बार मिलने के अवसर मिले थे | वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उन दिनों भूमिगत रहकर सरकार विरोधी लोगों की सूचनाएं , कुछ अखबार पत्रिकाएं जेलों तक पहुँचाने का काम कर रहे थे |गुजरात में ‘भूमिपुत्र’ नाम की पत्रिका निकलती थी। पत्रिका ने सरकारी सेंसर को मानने से इनकार कर दिया। 17 जुलाई, 1975 को सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने इस पत्रिका के आपत्तिजनक अंकों को जब्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही प्रेस और सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली गई। पत्रिका ने गुजरात हाईकोर्ट में सेंसर के खिलाफ अपील की। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला हाईकोर्ट पत्रिका के पक्ष में गया। लेकिन उस अदालती फैसले को भी नहीं छापने दिया गया |







