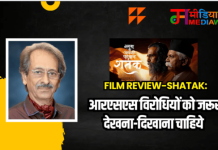हिंदी दिवस के मौके पर यदि सीध-सीधे कहें तो ऐसा लगता है कि भारत में 2050 के आसपास हिन्दी जानने-समझने-पढऩेे वाले नगण्य हो जाएंगे, इसका अंदेशा होने लगा है।इसलिए नहीं कि भारतवासियों का हिंदी से लगाव कम हो जाने की वजह से ऐसा होगा, बल्कि इसलिए कि आज का अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी की बजाय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में दाखिला करवा रहा है। जब वह हिंदी पढ़ेगा ही नहीं या ऐच्छिक भाषा के तौर पर पढ़ेगा तो हिंदी को कैसा और कितना जानेगा ? हद तो यह है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित माताएं तो बच्चों को डांट और प्यार भी अंग्रेजी में करने लगीं हैं। छी,छी , शु,शु बोलना उसे अशिष्टता लगता है और अंग्रेजी में पोट्टी,टॉयलेट बोलती है तो सोच लीजिये कि हम आखिर कहाँ जा रहे हैं ?
जिस तेजी के साथ हिंदी में अंग्रेजी की घुसपैठ हुई है, वह सीधे-सीधे भाषाई हमला ही है। विसंगति यह है कि ऐसा अंग्रेजी भाषियों ने नहीं किया, बल्कि जो हिंदी की खा रहे हैं, उन्होंने ही यह गुनाह किया है। इसमें साहित्य वाले तो फिर भी भाषा का मान बनाए हुए हैं, लेकिन हिंदी जानने-बोलने वालों के साथ हिंदी अखबार वालों ने कूड़ा ही कर दिया। उस पर तुर्रा यह कि ऐसा करना समय की मांग है। जबकि मुझे यह कहने में कतई मर्यादा आड़े नहीं आ रही कि बाजार में बिकने के लिए ही बैठने वाला भौंडा श्रृंगार कर और उत्तेजक भाव-भंगिमाओं से ग्राहक को लुभा रहा है, बनिस्बत रूप सौंदर्य का जलवा बिखेरने के। मॉरिशस में आयोजित ग्यारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन में 18 से 20 अगस्त 2018 तक दुनिया भर के हिंदी धुरंधरों का एकत्रीकरण हुआ , जिसमें इस नाचीज को भी भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल में शरीक किया गया था। वहां हिंदी में अंग्रेजी को बेवजह घुसाकर हिंदी को बदसूरत करने के लिए बाध्य करने वालों को बेनकाब करने पर बात नहीं हो पाई । अलबत्ता हिंदी को देश,दुनिया में प्रतिष्ठित करने पर ज़रूर गंभीर चिंतन हुआ ।यूँ इस वर्ष संभवत आयोजन की बारी थी , किन्तु कोरोना ने गड़बड़ कर दी।तीन,चार वर्ष के अंतराल में होने वाले इस आयोजन को वार्षिक किये जाने पर विचार होना चाहिए। अब भी समय है , जब हिंदी के माथे से बिंदी पोछने वाले हाथों को पकडक़र परे धकेलना होगा।
दुनिया में जो बदलाव हुआ ,उसकी अपेक्षा तो कतई न थी, फिर भी वह हुआ और निरंतर जारी है । कोई माई का लाल इसे रोक नहीं सकता । भाषा जैसे मौलिक विषय पर नि:संदेह यह सब नहीं होना चाहिए । जीवन के हर क्षेत्र में मिलावट और छेडख़ानी फिर भी धक सकती है,लेकिन भाषा और संस्कृति में इसकी दखलंदाजी समूचा तंत्र,तमाम सरोकार ही नष्ट-भ्रष्ट कर देगा । बीते कुछ वर्षों में भाषा को लेकर सर्वाधिक छेडख़ानी हिंदी में हुई और मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं कि इसकी शुरुआत तमाम हिंदी अखबारों और कुकुर मुत्तों की तरह गांव,खेड़ों तक में उग आये अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों ने की ।निस्संदेह उसे बढ़ावा दिया हमारी अपनी उस पीढ़ी ने जो अपने नौनिहालों को इसलिए अंग्रेजी पढ़ाने के पीछे बौरा गए, जो उन्हें किसी भी कीमत पर अच्छी नौकरी या विदेश में बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने की चाहत रखने लगे। इधर कुछ अलग करने की भेड़ चाल में हिंदी अखबारों ने एक सर्वथा नई भाषा विकसित की, जिसे नाम दिया-हिंग्लिश याने न हिंदी न इंग्लिश ।
ऐसे मिश्रण को हम खिचड़ी कहते हैं । यूं देखा जाए तो इसका संबंध देश में बढ़ती अंग्रेजी के चलन से है,लेकिन सीधे -सीधे उसे गलत ठहराने से हमारे अपने लोग बरी नहीं हो जाते । अंग्रेजी का बढ़ता प्रयोग, इसके अंतरराष्ट्रीय भाषा हो जाने,कॅरियर में इसके सहायक होने और समाज में इसके रूतबे के कारण हिंदी पत्र-पत्रिका संस्थानों ने इसके व्यावसायिक लाभ के मद्देनजर हिंदी को खिचड़ी बनने पर विवश किया । गलाकाट प्रतिस्पर्धा के बीच अपने को अलग और बेहतर करने के चक्कर में वे यह तक भूल गए कि वे जो करने जा रहे हैं,उस पर लगाम कसना उनके बस मेेंं नही रह पाएगा । दरअसल जबसे हिंदी पत्रकारिता में रोजाना कुछ अतिरिक्त पृष्ठ देने की शुरूआत हुई तभी से इस तरह की भाषा का बीजरोपण भी हुआ । तय यह किया गया कि युवा और विशिष्ट तबके के लिए कुछ अलग सामग्री दी जाए लेकिन इसमें विचारोत्तेजक,जानकारी वर्धक और उपयोगी लेखन की बजाए खिचड़ी भाषा को तवज्जो दी गई ,जिसने समूचे भाषा तंत्र को तहस-नहस कर डाला । इसकी एक बानगी एक अखबार की खबर का देखिए-
प्रदेश में प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल कोर्सेस के हजारों कॉलेज हैं जिनमें लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं । जॉब्स के मामले में कुछ हजार स्टूडेंट्स सफल हो पाते हैं । एक जैसे कोर्सेस में अधिक स्टूडेंट होने से मुसीबत नहीं आती । टेक्सटाइल और केमिकल्स ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भरपूर जॉब्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स कम हैं । प्रदेश में मात्र एक ही कॉलेज होने से यह आफत आई हैं । डिमांड देखते हुए एसजीएसआईटीएस जैसे बड़े गवर्नमेंट इंजीनियर कॉलेज ब्रांच शुरू करना चाहते हैं लेकिन बजट उनके आड़े आ जाता है ।
आप गौर करें कि छह वाक्यों के इस पैरेग्राफ में ठूंस-ठूसकर अंग्रेजी के शब्द भरे गए हैं । अब इसमें लॉर्ड मैकाले और महारानी विक्टोरिया की आत्मा हंसे या रोये ये वे खुद भी तय नहीं कर पा रहे होंगे । क्या आपको ऐसा लगता है कि उपर्युक्त पैरेग्राफ को आसान और सर्वग्राह्य हिंदी में नहीं लिखा जा सकता था ? क्या कोई पत्र-पत्रिका मालिक या संपादक यह बताना चाहेगा कि ऐसे कितने पाठकों ने उनके दरवाजे पर धरना देकर यह आग्रह किया कि वे हिंग्लिश में प्रकाशन करें ? यह ठीक उसी तरह है कि फिल्मों में हिंसा,मादकता और नग्नता के प्रर्दशन पर निर्माता-निर्देशक यह कहते पाए जाते हैं कि यह तो जनता की मांग है ।
इसी हिंग्लिश को आगे बढ़ाया मोबाइल के एसएमएस और इंटरनेट ने,लेकिन वह काफी बाद में आया । इसमें भी हिंदी के अखबारों ने उस समय तो हद ही कर दी जब उन्होंने युवा और हाई सोसायटी के अखबार के नाम पर परिशिष्ट में कुछ पेज अंग्रेजी के भी डालना शुरू कर दिया । याने जो लोग हिंदी न पढऩा चाहें वे बाकी पन्नों को कूड़ेदान में फेंक दें । दुनिया में शायद ही ऐसा कोई अन्य भाषा का प्रकाशन हो कि वह अंग्रेजी ,मलयायम,बंगला,मराठी,तमिल के बीच में हिंदी या अंग्रेजी का प्रकाशन करे । तब हिंदी वालों को ही ऐसी क्या पड़ी है कि अपनी मातृभाषा की बैंड बजा रहे हैं ?
यह सब एक घृणित प्रतिस्पर्धा का हिस्सा मात्र है । जबसे अखबारों में गुणवत्ता की बजाए पैकेजिंग,प्रजेंटेशन (ऐसा खुद अखबार वाले बोलते हैं)का दौर शुरू हुआ,तभी से इस खिचड़ी भाषा की शुरूआत भी हुई । अखबारों में भर्ती की एक अनिवार्य शर्त अब उसका भाषा का जानकार होना नहीं बल्कि अंग्रेजीदा होना हो गया । न कोई अखबारी पृष्ठभूमि, न लेखन से कोई वास्ता,न सामाजिक सरोकारों से लेना-देना ,न दीन-दुनिया की कोई जानकारी । सिर्फ और सिर्फ एक ही योग्यता कि बंदे को अंग्रेजी आती है क्या ? फर्राटे से बोल सकता है,टीप-टॉप रहता है ,फ्रेश ग्रेजुएट है-बस चयन हो गया । एक वक्त था जब अखबारों में भर्ती की एक प्रक्रिया होती थी । पहले लिखित परीक्षा होती,फिर साक्षात्कार । इसमें प्रतिस्पर्धी के धुर्रे बिखेर दिए जाते । चयन के बाद कहीं छह माह तो कहीं एक वर्ष का प्रशिक्षण होता । तब कहीं जाकर हाथ दिखाने का मौका मिलता ।
ऐसा भी कुछ नहीं है कि तमाम पत्रकार या हिंदी लेखक इसी प्रक्रिया से गुजरकर निखरे । उन्होंने अपने सामर्थ्य और समझ की बदौलत गहन परिश्रम के जरिए वह मुकाम हासिल किया जिसके वे हकदार थे । हां इतना तय है कि वे जन्मजात पत्रकार साबित हुए ।हिंदी मान बढ़ाने वाले पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी , माखनलाल चतुर्वेदी ,राजेंद्र माथुर,प्रभाष जोशी,राहुल बारपुते, वेदप्रताप वैदिक ,सुरेंद्र प्रताप सिंह ,उदयन शर्मा ,धर्मवीर भारती,कन्हैयालाल नंदन,रघुवीर सहाय,प्रभाकर माचवे ,श्रीनरेश मेहता,विद्यानिवास मिश्रा,गणेश मंत्री,राहुल देव, विश्वनाथ सचदेवा ,मनमोहन सरल ,चंदूलाल चंद्राकर,रतनलाल जोशी,राधेश्याम शर्मा, मृणाल पांडे, आलोक मेहता ,आलोक तोमर, राजकिशोर,हरिवंश , ओम थानवी, महावीर अधिकारी,कमल दीक्षित ,देवप्रिय अवस्थी , जवाहरलाल राठौर,दाऊलाल साखी,एन.के.सिंह,राजकुमार केसवानी,मदनमोहन जोशी, मायाराम सुरजन, माणिकचंद वाजपेयी,कृष्णकुमार अष्ठाना प्रमुख रहे । अस्सी,नब्बे के दशक से लेकर तो इक्कीसवीं सदी की शुरुआत की बात करें तो देश में हिंदी पत्रकारिता में रवींद्र शुक्ला,शाहिद मिर्ज़ा, राजेश बादल,पंकज शर्मा,शिव अनुराग पटैरया ,अवधेश व्यास,प्रकाश हिंदुस्तानी,प्रकाश दुबे ,यशवंत व्यास ,स्वामी त्रिवेदी, प्रभु जोशी ,निर्मला भुराड़िया,जयदीप कर्णिक,विकास मिश्रा, विजय मनोहर तिवारी आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा।
इन तमाम महारथियों ने खासकर हिंदी पत्रकारिता का मान बढ़ाया । अब मौजूदा हालातों में यह कहना तो पूरी तरह ठीक नहीं कि जन्मजात पत्रकार नहीं आ रहे,लेकिन इतना सुनिश्चित है कि अब अखबारी संस्थानों को इसमेें खास दिलचस्पी नहीं कि गुणवत्तापूर्ण, खोजपूर्ण पत्रकारिता करने वाले उनके यहां हों । वे चाहते हैं चटर-पटर अंग्रेजी बोलनेे वाले,कंप्यूटर जानने वाले,पेज बनाना जानने वाले,सुंदर ले आउट देने वाले।
बिगड़ तो काफी कुछ चुका है,फिर भी सुधार की गुंजाइश अभी बची है । हिंदी हमारी मातृभाषा है और सबसे ज्यादा छेड़छाड़ इसी के साथ हुई है । मां का यह अपमान कब तक ? व्यावसायिक हितों के आगे मूल भाव को खत्म कर देना इतना महंगा पड़ेगा कि एक समय के बाद इसकी कीमत चुका पाने लायक भी हम नहीं रह जाएंगे ।