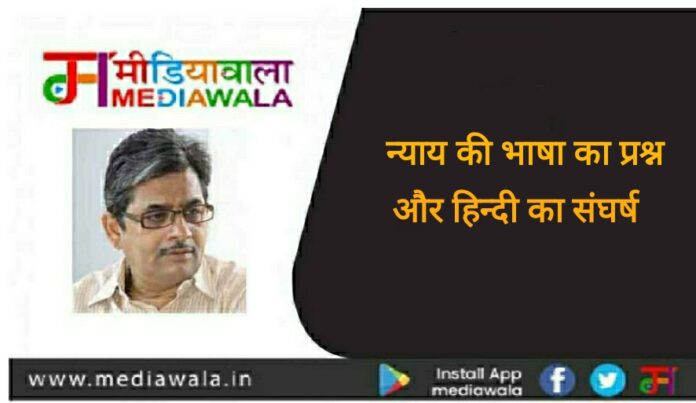
भला ये क्यों राय देंगे कि हिन्दी और देशी भाषाओं को न्याय की भाषा बनाई जाए।
सरकार के नीति निर्देशक प्रारूप यही अँग्रेजीदा लाटसाहब लोग बनाते हैंं तो ये अपनी ही पीढी के पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। सो यह मानकर चलिए कि ये सरकारोँ में आने जाने वाले लोग बातें तो हिन्दी की बहुत करेंगे, कसमें खाएंगे और संकल्प भी लेंगे पर हिन्दी की बरकत के लिए करेंगे कुछ भी नहीं।
हिन्दी को हिन्दी के मूर्धन्य भी नहीं पालपोस रहे हैं। उनकी रचनाओं, कृतियों को पढता कौन है..जो पीएचडी कर रहे होते हैं वे, या वे जिन्होंने समालोचकों का हुक्का भरा व उसके प्रतिद्वंदी को गरियाया वो, फिर कमराबंद संगोष्ठियों में अपनी अपनी सुनाने की प्रत्याशा में बैठे साहित्य के कुछ लोभार्थी और लाभार्थी। य
दि ये माने कि हिन्दी इनके माथे बची है या आगे बढ़ रही है तो मुगालते में हैं। हिन्दी में कोई बेहतरीन बिक्री वाली पुस्तक क्यों नहीं निकलती…? मैंने ही कमलेश्वर की..कितने पाकिस्तान ..के बाद कोई पुस्तक नहीं खरीदी। प्रेमचंद, निराला, दिनकर और इनके समकलीन ही पुस्तक की दूकानों में अभी भी चल खप रहे हैं।
दरअसल जो लोकरूचि का लेखक है उसे ये महंत और उनके पंडे साहित्यकार मानते ही नहीं। बाहर गाँडफादर, और लोलिता जैसे उपन्यासों को साहित्यिक कृति का दर्जा है। यहां ऐसी कृतियों को लुगदी साहित्य करार कर पल भर में खारिज कर दिया जाता है।
हिन्दी के कृतिकार अपने ख़ोल में घुसे हैं । यही इनकी दुनिया है। हिन्दी को बाजार पालपोस रहा है। यह उत्पादक और उपभोक्ता की भाषा है। बाजार के आकार के साथ साथ हिन्दी का भी आकार बढ़ रहा है। फिल्में हिन्दी को सात समंदर पार ले जा रही हैं। जिस काम की अपेक्षा साहित्यकारों से है वह काम अपढ फिल्मकार कर रहे हैं।
हिन्दी की गति उसकी नियति से तय हो रही है। जैसे फैले फैलने दीजिए। अपन तो यही मानते हैं कि जैसे घूरे के दिन भी कभी न कभी फिरते हैं, वैसे ही हिन्दी के भी फिरेंगे।







